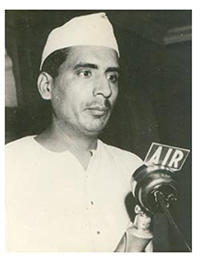 लिखते-लिखते लो उन्यासी वर्ष बीत चले। ऐसे बीते कि पता ही नहीं चला। अचरज होता है कि इतने दिन जिये तो कैसे! अपनी तरफ से तो कोई कसर छोड़ी नहीं। पिछले पचास वर्षों में मनों तंबाकू और टनों चाय के रूप में निकोटिन चूस लिया होगा, पी लिया होगा। आज भी उठते ही राम का नाम लेने से पहले चाय का नाम लेता हूं। फिर तंबाकू का पान जम जाता है, तब राम-कृष्ण का ध्यान आता है। कविता और पत्रकारिता तथा अल्हड़पन के साथ-साथ काम करने के दबाव ने मेरे जीवन को अनियमित बना दिया। बड़े गर्व के साथ कहता हूं कि भाइयो, मैं अनियमितताओं को बरतने के मामले में अत्यंत नियमित रहा हूं। शायद ही उन्यासी वर्ष का कोई ऐसा आदमी मिले जो दिन में कम से कम बीस प्याले चाय और तंबाकू के पच्चीस पान पी जाता हो, चबा जाता हो। जो ग्यारह बजे नाश्ता करता हो। तीन बजे से पहले लंच न लेता हो और रात का भोजन, मतलब कि डिनर ग्यारह बजे से पहले न करता हो। बुढ़ापे में जब मृत्यु का डर अधिक सताने लगता है और जीवन तथा जगत् के प्रति मोह दिन-पर-दिन बढ़ता जाता है, तब ऐसे आचरण करने वाले व्यक्ति को आप क्या कहेंगे ? इस पर तुर्रा यह कि मैं सोलह घंटे हिन्दी के लिए काम करता हूं और अब राजधानी में हिन्दी का विश्वमंदिर बनवाने में जुटा हूं। मूर्ख कहीं का मैं ! ऐसे कर्त्ता-धर्त्ता न जाने कितने हुए हैं, कितने हैं और न जाने कितने आगे होंगे ? लेकिन वाह रे मेरे दंभ ! जो अपनी अक्षमताओं को भी गुण-गौरव प्रदान करने में बाज नहीं आता। लेकिन इतनी बात सच है कि जब वैद्यों ने बताया कि मुझमें तपेदिक के आसार बढ़ रहे हैं, तब मैं हंसा और हंसते-हंसते बिना किसी उपचार के तपेदिक को भगा दिया। जब आंखें जवाब देने लगीं, तब सोचा-व्यास, अब देखने को क्या बचा है ? देश-विदेश, नदी-सरोवर, वन-पहाड़, पुरातत्त्व के पवित्र स्थान, तीर्थस्थल, देश का कोई बड़ा नगर या कस्बा रह गया क्या देखने से ? अपने देखे, पराये देखे। सुंदर देखे, सुंदरियां देखीं। सिंह देखे, गीदड़ देखे। विषधर नाग देखे, बलखाती नागिनें देखीं। बहुतों को मित्र बनाकर देख लिया और शत्रु बनाकर भी। शिष्य बनाकर देख लिया और शिष्या बनाकर भी। परंतु जब देखा-
लिखते-लिखते लो उन्यासी वर्ष बीत चले। ऐसे बीते कि पता ही नहीं चला। अचरज होता है कि इतने दिन जिये तो कैसे! अपनी तरफ से तो कोई कसर छोड़ी नहीं। पिछले पचास वर्षों में मनों तंबाकू और टनों चाय के रूप में निकोटिन चूस लिया होगा, पी लिया होगा। आज भी उठते ही राम का नाम लेने से पहले चाय का नाम लेता हूं। फिर तंबाकू का पान जम जाता है, तब राम-कृष्ण का ध्यान आता है। कविता और पत्रकारिता तथा अल्हड़पन के साथ-साथ काम करने के दबाव ने मेरे जीवन को अनियमित बना दिया। बड़े गर्व के साथ कहता हूं कि भाइयो, मैं अनियमितताओं को बरतने के मामले में अत्यंत नियमित रहा हूं। शायद ही उन्यासी वर्ष का कोई ऐसा आदमी मिले जो दिन में कम से कम बीस प्याले चाय और तंबाकू के पच्चीस पान पी जाता हो, चबा जाता हो। जो ग्यारह बजे नाश्ता करता हो। तीन बजे से पहले लंच न लेता हो और रात का भोजन, मतलब कि डिनर ग्यारह बजे से पहले न करता हो। बुढ़ापे में जब मृत्यु का डर अधिक सताने लगता है और जीवन तथा जगत् के प्रति मोह दिन-पर-दिन बढ़ता जाता है, तब ऐसे आचरण करने वाले व्यक्ति को आप क्या कहेंगे ? इस पर तुर्रा यह कि मैं सोलह घंटे हिन्दी के लिए काम करता हूं और अब राजधानी में हिन्दी का विश्वमंदिर बनवाने में जुटा हूं। मूर्ख कहीं का मैं ! ऐसे कर्त्ता-धर्त्ता न जाने कितने हुए हैं, कितने हैं और न जाने कितने आगे होंगे ? लेकिन वाह रे मेरे दंभ ! जो अपनी अक्षमताओं को भी गुण-गौरव प्रदान करने में बाज नहीं आता। लेकिन इतनी बात सच है कि जब वैद्यों ने बताया कि मुझमें तपेदिक के आसार बढ़ रहे हैं, तब मैं हंसा और हंसते-हंसते बिना किसी उपचार के तपेदिक को भगा दिया। जब आंखें जवाब देने लगीं, तब सोचा-व्यास, अब देखने को क्या बचा है ? देश-विदेश, नदी-सरोवर, वन-पहाड़, पुरातत्त्व के पवित्र स्थान, तीर्थस्थल, देश का कोई बड़ा नगर या कस्बा रह गया क्या देखने से ? अपने देखे, पराये देखे। सुंदर देखे, सुंदरियां देखीं। सिंह देखे, गीदड़ देखे। विषधर नाग देखे, बलखाती नागिनें देखीं। बहुतों को मित्र बनाकर देख लिया और शत्रु बनाकर भी। शिष्य बनाकर देख लिया और शिष्या बनाकर भी। परंतु जब देखा-
“चेले हुए रफूचक्कर,
चेलीं गईं पराये घर,
साथी गए किनारा कर,
जय बम बोले शिवशंकर !”
 अब जितना दीखे वह ठीक और न दीखे वह भी ठीक। कान जितना सुनें, ठीक और न सुनें तो भी ठीक। मधुमेह जब तक जिलाए तब तक ठीक, ले जाए तो राम-नाम सत्य है। न लगकर दवा की, न मन से दुआ मांगी। ऐसों की दुआ कबूल होती भी कहां है ?
अब जितना दीखे वह ठीक और न दीखे वह भी ठीक। कान जितना सुनें, ठीक और न सुनें तो भी ठीक। मधुमेह जब तक जिलाए तब तक ठीक, ले जाए तो राम-नाम सत्य है। न लगकर दवा की, न मन से दुआ मांगी। ऐसों की दुआ कबूल होती भी कहां है ?
जो हो रहा है, होने दो। जो चल रहा है, चलने दो। जो जला है, वह बुझेगा ही। जो खिला है, वह मुरझाएगा ही। आग बुझ जाती है। पानी सूख जाता है। हवा रुक जाती है। सूरज, चांद और सितारे उदय होते हैं और अस्त हो जाते हैं। तब इस नश्वर काया की क्या बात ? धरती पर जो आया है, वह जाएगा ही, तो चिंता क्यों ?
परंतु भाई, इस नश्वर देह के जाने पर तुम शोक न करना। अनमोल आंसुओं को न बहाना। मेरी ये पक्तियां याद रखना-
“खुशियों को खरीदा है हमने,
सेहत को सदा नीलाम किया,
लमहा वह याद नहीं आता,
जिस वक्त कि हो आराम किया।
रोगों को सहेजा है हमने,
भोगों को नहीं परहेजा है,
गम बांटे नहीं, खुशियां बोईं,
मुस्कान को सब तक भेजा है।”
 तो शिव के निकल जाने पर शव को देखकर रोना क्या ? खुशियां मनाना कि यह रोगग्रस्त जर्जर देह से व्यास नामक जीवधारी का पिंड छूटा। चलो अच्छा हुआ।
तो शिव के निकल जाने पर शव को देखकर रोना क्या ? खुशियां मनाना कि यह रोगग्रस्त जर्जर देह से व्यास नामक जीवधारी का पिंड छूटा। चलो अच्छा हुआ।
मैं ज्ञानी तो नहीं, पर इतना अवश्य जान गया हूं कि यह जो देह मेरी समझी जाती है, वह मेरी नहीं है। मैं देह नहीं हूं। ”ईश्वर-अंश जीवन अविनाशी” हूं। हिन्दू हूं न। शास्त्रों की वह बात संस्कारों में बैठी हुई है कि जीव तो कर्मों के बंधन में जकड़ा हुआ है। कर्मों का नाश जप-तप और साधनों से नहीं होता। वह तो श्रद्धा, भक्ति और अच्युत भगवान के अनुग्रह से संभव है। ज्ञान की बड़ी महिमा है। भगवान कहते हैं कि मुझे ज्ञानी प्रिय हैं।
लेकिन उनका यह भी कथन है कि ”हम भक्तन के भक्त हमारे”। महात्मा कवि सूरदास के मन में भी यह द्वंद्व था। लेकिन उन्होंने समाधान पा लिया और गाया-
“इक माया, इक ब्रह्म्र कहावत,
‘सूरदास’ झगरौ।
अबकी बेर मोहि पार उतारौ,
नहिं प्रन जात टरौ॥”
 ज्ञान और भक्ति के संबंध में एक बड़ा रोचक प्रसंग है। एक साधक मोक्ष-मार्ग को जानने के लिए व्याकुल था। उसके गांव में एक साधु आए। उसने रास्ता पूछा। साधु ने बताया कि ‘सोऽहम्-सोऽहम्’ का जाप करो। कुछ दिन बाद दूसरे साधु आए। उन्होंने कहा-‘सोऽहम्’ नहीं, ‘दासोऽहम्’ जपा करो। पहले वाले साधु फिर से घूमते-घामते आगए। देखा कि चेला तो ‘दासोऽहम्-दासोऽहम्’ जप रहा है। तो उन्होंने समझाया कि ‘दासोऽहम्’ नहीं, ‘सदासोऽहम्’ जपा करो। इसके उत्तर में अंत में भक्तिवादी कह गए-नहीं बच्चा, ‘सदासोऽहम्’ क्या ? ‘दासदासोऽहम’ जपो। कहने का तात्पर्य यह कि ज्ञान-मार्ग हो या भक्ति-मार्ग, जब तक प्रभु का अनुग्रह प्राप्त नहीं होता, जब तक ”पुनरपि जननं, पुनरपि मरणं, पुनरपि जननी जठरे शयनम्।”
ज्ञान और भक्ति के संबंध में एक बड़ा रोचक प्रसंग है। एक साधक मोक्ष-मार्ग को जानने के लिए व्याकुल था। उसके गांव में एक साधु आए। उसने रास्ता पूछा। साधु ने बताया कि ‘सोऽहम्-सोऽहम्’ का जाप करो। कुछ दिन बाद दूसरे साधु आए। उन्होंने कहा-‘सोऽहम्’ नहीं, ‘दासोऽहम्’ जपा करो। पहले वाले साधु फिर से घूमते-घामते आगए। देखा कि चेला तो ‘दासोऽहम्-दासोऽहम्’ जप रहा है। तो उन्होंने समझाया कि ‘दासोऽहम्’ नहीं, ‘सदासोऽहम्’ जपा करो। इसके उत्तर में अंत में भक्तिवादी कह गए-नहीं बच्चा, ‘सदासोऽहम्’ क्या ? ‘दासदासोऽहम’ जपो। कहने का तात्पर्य यह कि ज्ञान-मार्ग हो या भक्ति-मार्ग, जब तक प्रभु का अनुग्रह प्राप्त नहीं होता, जब तक ”पुनरपि जननं, पुनरपि मरणं, पुनरपि जननी जठरे शयनम्।”
ईश्वर क्या है ? बड़ा झमेला है। कोई कहता है कि वह क्षीरसागर में है। कोई कहता है कि वह सातवें आसमान पर है। कोई कहता है कि वह साकेत में है। कोई कहता है कि वह गोलोक में है। कोई कहता है – ”मुझको कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में।” महर्षि अंगिरा कहते हैं कि ईश्वर तुम्हारे बाईं तरफ है, दाहिनी ओर है, पीठ पीछे है और देखो, वह सामने भी है। बहुत सारी लोकोक्तियां हैं जो कहती है- ”मोमें, तोमें, खड्ग-खंभ में व्याप रह्यौ जगदीश।” संत कहते हैं-”पुष्प मध्य ज्यों वास बसत है, मुकुर मध्य ज्यों छांहीं।” ऐसे ही ईश्वर सर्वत्र व्याप्त है। कोई सूंघे तो सही। कोई झांके तो सही। कोई कहता है कि इस जग-जंजाल से बचने के बाद ही ईश्वर को पाया जा सकता है।
 तो कोई कहता है ”जगत साक्ष्यरूपं नमामः”। कोई कहता है कि हृदयरूपी गुहा में स्थित आत्मा के परमात्मा से मिलन में माया ही सबसे बड़ी बाधा है। यह माया ही मन को चलाती है। मन ही इंद्रियों को आदेश देता है। इंद्रियां ही कर्म करती हैं। इन्हीं कर्मों का फल भोगने के लिए जीव विवश है- ” माया महाठगनि हम जानी।” लेकिन कुछ ज्ञानियों का कहना है कि माया ही ब्रह्म की आदिशक्ति है। उसी के द्वारा जगदीश्वर निखिल ब्रह्मांड की उत्पति करते हैं, परिचालन करते हैं और फिर अपनी माया को समेटकर अपने में लीन कर लेते हैं। माया शक्ति है, अनुरक्ति है, भक्ति है, कला और संस्कृति है। वह उमा है, रमा है और शारदा है। है न यह झमेले की बात ?
संत कहते हैं कि ईश्वर को तर्क से नहीं पाया जा सकता। तर्क विवेक नहीं है। लेकिन दुनिया में करोड़ों लोग हैं, उनमें असंख्य चिंतक भी हैं जो मानते हैं कि ईश्वर नाम की कोई वस्तु है ही नहीं। जो कुछ है, वह प्रकृति है।
तो कोई कहता है ”जगत साक्ष्यरूपं नमामः”। कोई कहता है कि हृदयरूपी गुहा में स्थित आत्मा के परमात्मा से मिलन में माया ही सबसे बड़ी बाधा है। यह माया ही मन को चलाती है। मन ही इंद्रियों को आदेश देता है। इंद्रियां ही कर्म करती हैं। इन्हीं कर्मों का फल भोगने के लिए जीव विवश है- ” माया महाठगनि हम जानी।” लेकिन कुछ ज्ञानियों का कहना है कि माया ही ब्रह्म की आदिशक्ति है। उसी के द्वारा जगदीश्वर निखिल ब्रह्मांड की उत्पति करते हैं, परिचालन करते हैं और फिर अपनी माया को समेटकर अपने में लीन कर लेते हैं। माया शक्ति है, अनुरक्ति है, भक्ति है, कला और संस्कृति है। वह उमा है, रमा है और शारदा है। है न यह झमेले की बात ?
संत कहते हैं कि ईश्वर को तर्क से नहीं पाया जा सकता। तर्क विवेक नहीं है। लेकिन दुनिया में करोड़ों लोग हैं, उनमें असंख्य चिंतक भी हैं जो मानते हैं कि ईश्वर नाम की कोई वस्तु है ही नहीं। जो कुछ है, वह प्रकृति है।
 जो भी जड़-चेतन इस जगत में है, वह प्रकृति के नियमों से बंधा हुआ है। उन नियमों और उनके कारणों को जानकर ही हम व्यक्ति, समाज, राष्ट्र और जगत का कल्याण कर सकते हैं। सबसे अद्यतन वैज्ञानिक खोज है कि हो न हो, कहीं कोई ज्योति-पुंज अवश्य है। प्रकाश का अक्षय केन्द्र है। उससे ही सृष्टि की उत्पत्ति, विकास और विनाश होता रहता है। उसी से ग्रह या लोक बनते-बिगड़ते हैं, उल्काएं टूटती हैं, सूर्य प्रकाशित होते हैं और ठंडे पड़ते हैं, ग्रह-नक्षत्र घूमते हैं, उसी एक धुरी पर। अब बताइए, किसकी बात पर विश्वास करें और कैसे उस ईश्वर को प्राप्त करें ? आदमी ने जबसे होश संभाला है, तभी से वह अदृश्य के प्रति जिज्ञासु रहा है। उसने सूर्य को नमस्कार किया। चंद्रमा के दिव्य प्रकाश को नमन किया। वरुण को, पवन को, धरित्री को, अग्नि को पहले ईश्वर माना, बाद में देवता कह दिया। फिर ब्रह्म्र माना और ”अथातो ब्रह्म्र जिज्ञासा” शुरू हो गई।
जो भी जड़-चेतन इस जगत में है, वह प्रकृति के नियमों से बंधा हुआ है। उन नियमों और उनके कारणों को जानकर ही हम व्यक्ति, समाज, राष्ट्र और जगत का कल्याण कर सकते हैं। सबसे अद्यतन वैज्ञानिक खोज है कि हो न हो, कहीं कोई ज्योति-पुंज अवश्य है। प्रकाश का अक्षय केन्द्र है। उससे ही सृष्टि की उत्पत्ति, विकास और विनाश होता रहता है। उसी से ग्रह या लोक बनते-बिगड़ते हैं, उल्काएं टूटती हैं, सूर्य प्रकाशित होते हैं और ठंडे पड़ते हैं, ग्रह-नक्षत्र घूमते हैं, उसी एक धुरी पर। अब बताइए, किसकी बात पर विश्वास करें और कैसे उस ईश्वर को प्राप्त करें ? आदमी ने जबसे होश संभाला है, तभी से वह अदृश्य के प्रति जिज्ञासु रहा है। उसने सूर्य को नमस्कार किया। चंद्रमा के दिव्य प्रकाश को नमन किया। वरुण को, पवन को, धरित्री को, अग्नि को पहले ईश्वर माना, बाद में देवता कह दिया। फिर ब्रह्म्र माना और ”अथातो ब्रह्म्र जिज्ञासा” शुरू हो गई।
मनु के पुत्र की ईश्वरीय रहस्य को भेदने, उसे खोजने और जानने की लगन जारी रही। समुद्र की उत्ताल तरंगों के ऊपर जब उसने नाचती हुई मछली को देखा तो कहा-यही ईश्वर है।
जब उसने हिरण्यकश्यप जैसे शक्तिशाली और प्रतापी राजा को एक सिंह जैसे नर द्वारा अपने नखों से विदीर्ण करते देखा, तब बोला- अब समझ में आया, यही ईश्वर है। जब कुठारधारी एक पराक्रमी ब्राह्मण ने इक्कीस बार इस धरती के योद्धाओं (क्षत्रियों) को अकेले पराजित कर दिया, तब उसने शक्ति-पुंज महाबली परशुराम को ही परमेश्वर मान लिया। लेकिन जब परशुराम के तेज को दाशरथी राम ने आत्मसात कर लिया और दण्डकारण्य में अकेले दस हजार आतंकवादियों को धराशायी कर डाला तथा उसके बाद विश्वविजयी, महापराक्रमी लंकाधिपति रावण को परिजन-पुरजन समेत नष्टकर सीता को छुड़ा लिया तो कौशल्या नंदन राम घट-घटवासी होगए। ”उठते राम, बैठते राम, सोते राम, जब बोलो तब रामहि राम, खाली जिह्वा कोने काम।” राम जनजीवन में रम गए। लोगों ने कहा-अरे, यह तो राजा हैं। पर तुलसीदास ने उत्तर दिया-
“जो जगदीश तो अति भलो, जो महीप तौ भाग।
तुलसी चाहत दुहूं विधि, राम-चरण अनुराग।”
“स्तोत्रों में स्तुति की गई-
राम रामेति रामेति रमे राम मनोरमे,
समस्रनाम तततुल्यं राम नाम वरानने।”
लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम बारह कलाओं से युक्त रहे। लोकमानस ने श्रीकृष्ण में सोलह कलाओं के दर्शन किए और घोषणा होगई-”कृष्णस्तु भगवान् स्वयं” और कृष्ण ही क्यों, उनका गुणगान करते-करते ”व्यासस्तु भगवान् स्वयं” बन गए। व्यास लेखक और संपादक थे तो क्या मैं उस पंरपरा में नहीं हूं। बुद्ध और महावीर को तो भगवान् कहा ही गया है। लोकमान्य तिलक भी भगवान् कहकर सम्मानित किए गए। बचपन में हम गाया करते थे-”अवतार महात्मा गांधी है, इस गवरमेंट के मारन को।” कहने का तात्पर्य यह है कि जिसमें भी मनुष्य को सत्य, शिव और सुंदर के दर्शन हुए, जो भी शक्तिसंपन्न और तेजोमय लगा, वही भगवान् का अवतार मान लिया गया। अवतार क्या, स्वयं भगवान् मान लिया गया। स्वयं श्रीकृष्ण भगवान् कह ही गए हैं-
“यद् यद् विभूतिमन्सत्वं श्रीमर्द्जितमेव वा।
तत् तदेवावगच्छं त्वं मम तेजोंऽश सम्भवम्।”
अंत में, जहां तक समझा वह यह कि न मैं लोक को जान पाया, न परलोक को। आत्म-तत्व की खोज में लगा हूं, परंतु उसने भी अभी तक परमात्मा तक पहुंचाने में कोई सहायता नहीं की। तो फिर जो होना है, हो। जो नहीं होना है, न हो। सार यही है – ”कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन।”
कर्म किए जाओ। भाव यह रखो कि ”यथा नियुक्तोऽस्मि तथा करोमि।” जब कर्म करने का अधिकार हमें मिला है तो क्यों न करें ? जब फल-प्राप्ति पर हमारा वश नहीं है तो उसे लेकर परेशान क्यों हों ? और कर्म ? पाप-पुण्य ? महर्षि व्यास के ये वचन-”परोपकारः पुण्याय, पापाय परपीड़नम्।” भला सोचो, भला कहो, भला करो। कोई ऐसा काम न करो जिससे दूसरों को कष्ट पहुंचे।
परंतु महाभारत में ही कहा है-
“जानामि धर्मं न च मे प्रवृत्ति
जानामि अधर्मं न च मे निवृत्ति।
केनापि देवेन हृदि स्थितेन
यथा नियुक्तोऽस्मि तथा करोमि।”
”मैं धर्म को जानता हूं, परंतु उसमें मेरी प्रवृत्ति नहीं हो पाती। अधर्म और अकर्म को भी जानता हूं, परंतु उनसे निवृत्ति नहीं हो पाती।” मित्रो, यही हाल मेरा भी है-
“जनम पाय कछु भलौ न कीनौ,
याते अधिक डरौं।
अब मैं कौन उपाय करौं ?”
जिज्ञासाओं का अंत नहीं। पर समाधान का कोई ठिकाना नहीं। इतना अवश्य पता है कि ईश्वर है और अवश्य है। साकार है और निराकार भी है। उसे ग्रहण भी किया जा सकता है-श्रद्धा, भक्ति और प्रेम के द्वारा। उसे समझा भी जा सकता है-सत्-चित और आनंद के रूप में।
उसमें से मैंने आनंद को पकड़ लिया है-वही मेरे व्यक्तित्व और कृतित्व का केन्द्र है। इसे समझकर जितना कर सकता हूं, किया है और जिया है।
हां, तो मैं कह रहा था कि उन्यासी वर्ष का होगया। जीवन की अंतिम बेला निकट आ रही है-”सब ठाठ पड़ा रह जाएगा, जब लाद चलेगा बंजारा।” यह पुत्र-कलत्र, यह संपत्ति और संतति सब यहीं रह जाएंगे। लोग कहते हैं कि साहित्य बचेगा। यह भ्रम है। कालिदास और सूरदास से पहले न जाने कितने कवि हुए हैं, उनका पता नहीं चलता। मेरे देखते-देखते सैकड़ों बहुप्रचारित और बहुप्रसारित साहित्यिक व्यक्तित्व ऐसे लुप्त हुए कि आज उनका कोई नाम भी नहीं जानता। सूर, तुलसी, मीरा और कबीर आज हैं, कल उनकी प्रासंगिकता रहेगी, यह कौन कह सकता है ? वेदों की रचना जिन ऋषियों ने की, उनके नाम किसी को पता हैं ? सारे पुराण, महाभारत, श्रीमद् भागवत गीता, यहां तक कि वेद भी,उनके रचयिताओं का पता न लगने पर, व्यास के साथ जुड़ गए।
अब व्यास को भी उन सबका कर्त्ता नहीं माना जा रहा है। नैमिषारण्य के अठ्ठासी हजार शौनकादिक ऋषि कौन थे, इसका किसी को क्या पता ? तब मैं और मेरा साहित्य क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा ! लोग कहते हैं कि मैंने हिन्दी व्यंग्य-विनोद में नई ज़मीन तोड़ी है। यह भुलाए नहीं भूलेगी। इस खुशफहमी के लिए मैं क्या कहूं ? लोग यह भी कहते हैं कि मेरी बनाई और चलाई हुई संस्थाओं से मेरा नाम चलेगा। परंतु मैंने बड़ी से बड़ी संस्थाओं को अपने सामने ध्वस्त होते देख लिया है। आगे आने वाले लोगों ने उन संस्थाओं के प्रवर्तकों और परिचालकों के नाम मिटा दिए। कुछ लोगों का कहना है कि मेरी ब्रज और ब्रजभाषा, दिल्ली, हिन्दी और हिन्दी भवन के निर्माण की सेवाओं को लोग नहीं भूलेंगे। किंतु मैं ऐसे भ्रम नहीं पालता। मैं वर्तमान में जिया हूं। जो करने योग्य मेरे वश के काम मेरे सामने आए हैं, उन्हें हंसते-खेलते किया है। अपने समय में यदि मैं कर्तव्य का पालन कर सका तो मेरे लिए यही बहुत है। भविष्य की चिंता न तब थी और न अब है।
हां, तो मैं कह रहा था कि मेरे न रहने पर शोक न करना। मैंने हंसी-खुशी से अपना जीवन गुज़ारा है। तुम भी हंसी-खुशी से मेरी देह को ठिकाने लगा देना। शोक सभाएं मत करना। हो सके तो हास्य-रस के कवि-सम्मेलन कराना। हिन्दी को आगे बढ़ाने की बात निश्चित करना। भाषा के रूप में नहीं, भारतवाणी के रूप में। भारतीय संस्कृति के रूप में। भारत की अमर आत्मा के रूप में। अगर मेरे परवर्ती लोग मानें तो मैं यह कहना चाहता हूं कि- मेरी इस देह को किसी जंगल में फेंक देना, जिससे जीव-जंतु इस मृत शरीर को खाकर कुछ क्षणों के लिए तो आनंद प्राप्त कर सकें-”माटी खाय जिनावरा, महा-महोच्छव होय।” अथवा, जल-जीवों के निमित्त इसे किसी नदी में प्रवाहित कर देना। परंतु लोक-लाज और परंपराओं के कारण यदि ऐसा संभव न हो, तो इसे साधारण ढंग से वेद-मंत्रों के साथ अग्नि को समर्पित कर देना। मेरी कर्मकांड मे रुचि नहीं है, न पिंडदान में, न शय्यादान में, न मृतकभोज में। शव से दूषित घर को, शरीर को, वस्त्रों को स्वच्छ करना और देह की नश्वरता का स्मरण करते हूए षट्कर्म करना, प्यारे भाई ! ओम शांति !
(‘कहो व्यास, कैसी कटी ?’, सन् 1994)