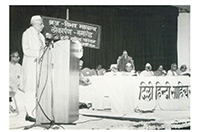 जि मन करै है कै जा अग्रलेख कूं अपनी मिठबोलनी, रसघोलनी ब्रजभाषा में ही च्यौं न लिखैं ? परंतु नहीं, भारत के राष्ट्रीय जागरण और हिन्दी के अरुणोदय की बेला में ही हमारे अग्रचेता पूर्वजों ने यह अलिखित समझौता और दृढ़ संकल्प कर लिया था कि भाई, तुम लिखो गद्य और हमसे बन पड़ेगा तो रचते रहेंगे पद्य। संवर्धन रहा आज से हिन्दी के लिए और संरक्षण रहा ब्रजभाषा के लिए। संप्रेषण हिन्दी का और सर्वेक्षण ब्रजभाषा का। इस तरह प्रयाग पहुंचते-पहुंचते ही ब्रज की कलित कालिंदी राष्ट्रभाषा की पावन गंगा में स्वेच्छा से समाहित हो चुकी थी। पूर्वजों के ऐसे ऐतिहासिक समझौते और शुद्ध संकल्प को हम तोड़ेंगे नहीं। माना कि ब्रज हमारे रोम-रोम में बसा है, चित्त पर चढ़ा है और उसके साहित्य की सुधराई तथा ब्रज की लुनाई हम पर ऐसी छाई है कि ‘मन ह्वै जात कालिंदी के तीर।’ जैसे-जैसे हम ब्रज-रस में पैठते हैं, उसकी चंद्र सरोवर में अवगाहन करते हैं, गोवर्धन गिरिराज महाराज की परिक्रमा देते हैं, ब्रज-साहित्य का अवलोकन करते हैं, उसके स्वर्णिम अतीत में झांकते हैं तो मन वृंदावन हो जाता है। xमथुरा मनोहर लगने लगती है। गोकुल, नंदगांव, बरसाना, परम रासस्थली अर्थात वृंदावन का परमानंद और महारास हमारी मनोभूमि पर अवतरित हो जाता है। बांसुरिया बज उठती है। मोर नाचने लगते हैं। कोकिल कूकने लगती है। यमुना लहर-लहर हो जाती है। धौरी-धूमर और काजर गायें कहीं हूकती और कहीं हूलती दिखाई देती हैं, तो कहीं बछिया-बच्चे उछल-कूद मचाते मिलते हैं। तरु, लता, गुल्म, कुंज और कुटीर, सर-सरोवर, मंदिर-मठ, टीले, स्तूप, हरीभरी छोटी-छोटी पहाड़ियां, कोरे और भोरे ग्वाल तथा गौरी और चिरकिशोरी गोपियां एवं उनके सर्वस्व युगल प्रिया-प्रियतम राधाकृष्ण हमारे मन के हिंडोले पर ऐसे झूलने लगते हैं कि जैसे महाकवि देव कह रहे हों-‘झूलत है हियरा हरि कौ, हिय मांहि तिहारे हरा के हिंडोरे।’
ब्रज ससीम नहीं, असीम है।
जि मन करै है कै जा अग्रलेख कूं अपनी मिठबोलनी, रसघोलनी ब्रजभाषा में ही च्यौं न लिखैं ? परंतु नहीं, भारत के राष्ट्रीय जागरण और हिन्दी के अरुणोदय की बेला में ही हमारे अग्रचेता पूर्वजों ने यह अलिखित समझौता और दृढ़ संकल्प कर लिया था कि भाई, तुम लिखो गद्य और हमसे बन पड़ेगा तो रचते रहेंगे पद्य। संवर्धन रहा आज से हिन्दी के लिए और संरक्षण रहा ब्रजभाषा के लिए। संप्रेषण हिन्दी का और सर्वेक्षण ब्रजभाषा का। इस तरह प्रयाग पहुंचते-पहुंचते ही ब्रज की कलित कालिंदी राष्ट्रभाषा की पावन गंगा में स्वेच्छा से समाहित हो चुकी थी। पूर्वजों के ऐसे ऐतिहासिक समझौते और शुद्ध संकल्प को हम तोड़ेंगे नहीं। माना कि ब्रज हमारे रोम-रोम में बसा है, चित्त पर चढ़ा है और उसके साहित्य की सुधराई तथा ब्रज की लुनाई हम पर ऐसी छाई है कि ‘मन ह्वै जात कालिंदी के तीर।’ जैसे-जैसे हम ब्रज-रस में पैठते हैं, उसकी चंद्र सरोवर में अवगाहन करते हैं, गोवर्धन गिरिराज महाराज की परिक्रमा देते हैं, ब्रज-साहित्य का अवलोकन करते हैं, उसके स्वर्णिम अतीत में झांकते हैं तो मन वृंदावन हो जाता है। xमथुरा मनोहर लगने लगती है। गोकुल, नंदगांव, बरसाना, परम रासस्थली अर्थात वृंदावन का परमानंद और महारास हमारी मनोभूमि पर अवतरित हो जाता है। बांसुरिया बज उठती है। मोर नाचने लगते हैं। कोकिल कूकने लगती है। यमुना लहर-लहर हो जाती है। धौरी-धूमर और काजर गायें कहीं हूकती और कहीं हूलती दिखाई देती हैं, तो कहीं बछिया-बच्चे उछल-कूद मचाते मिलते हैं। तरु, लता, गुल्म, कुंज और कुटीर, सर-सरोवर, मंदिर-मठ, टीले, स्तूप, हरीभरी छोटी-छोटी पहाड़ियां, कोरे और भोरे ग्वाल तथा गौरी और चिरकिशोरी गोपियां एवं उनके सर्वस्व युगल प्रिया-प्रियतम राधाकृष्ण हमारे मन के हिंडोले पर ऐसे झूलने लगते हैं कि जैसे महाकवि देव कह रहे हों-‘झूलत है हियरा हरि कौ, हिय मांहि तिहारे हरा के हिंडोरे।’
ब्रज ससीम नहीं, असीम है।
लोग ब्रज को सीमाओं में बांधते हैं। कोई कहते हैं कि गोकुल ही ब्रज है।
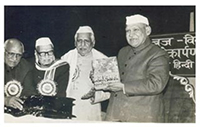 कोई कहते हैं नहीं, वृंदावन ही ब्रज है। कोई गिरि गोवर्धन की तलहटी में बसे हुए गांवों को, यानी जहां-जहां से गोवर्द्धन दिखाई देता है, ब्रज बताते हैं। कोई कहते हैं, ब्रज, चौरासी कोस में फैला हुआ है-“ब्रज चौरासी कोस में चार गाम निज धाम। वृंदावन अरु मधुपुरी, बरसानौ नंदनाम।” कुछ का मानना है कि ब्रज मथुरा जनपद तक ही सीमित नहीं है। ब्रजभाषा जहां-जहां बोली जाती है, ब्रज की व्यापकता की परिधि वहीं-वहीं तक जानिए। अर्थात अलीगढ़, आगरा, एटा, इटावा, मैनपुरी आदि और इधर धौलपुर, ग्वालियर, बुंदेलखंड, झांसी तक। उधर फिर डीग, भरतपुर, बयाना, करौली, अलवर आदि जिलों में भी तो ब्रजभाषा और ब्रज-भावना की लटक पूरी तरह विद्यमान है। कुछ इस वृहत्तर ब्रज से भी संतुष्ट नहीं है। वे कहते हैं कि कृष्ण की रसमयी लीलाभूमि ही नहीं, जहां-जहां से श्रीकृष्ण का रथ गुजरा है, जहां वह बसे हैं और जहां-जहां तक उनकी गीता का संदेश गया है, वह सब ब्रज ही है। अर्थात ब्रज ससीम नहीं, असीम है। वह नयन-पथगामी भी है और पलक-कपाट लगाने के बाद भावुकों के भावना-जगत में भी अखंड रूप से विद्यमान है।
कोई कहते हैं नहीं, वृंदावन ही ब्रज है। कोई गिरि गोवर्धन की तलहटी में बसे हुए गांवों को, यानी जहां-जहां से गोवर्द्धन दिखाई देता है, ब्रज बताते हैं। कोई कहते हैं, ब्रज, चौरासी कोस में फैला हुआ है-“ब्रज चौरासी कोस में चार गाम निज धाम। वृंदावन अरु मधुपुरी, बरसानौ नंदनाम।” कुछ का मानना है कि ब्रज मथुरा जनपद तक ही सीमित नहीं है। ब्रजभाषा जहां-जहां बोली जाती है, ब्रज की व्यापकता की परिधि वहीं-वहीं तक जानिए। अर्थात अलीगढ़, आगरा, एटा, इटावा, मैनपुरी आदि और इधर धौलपुर, ग्वालियर, बुंदेलखंड, झांसी तक। उधर फिर डीग, भरतपुर, बयाना, करौली, अलवर आदि जिलों में भी तो ब्रजभाषा और ब्रज-भावना की लटक पूरी तरह विद्यमान है। कुछ इस वृहत्तर ब्रज से भी संतुष्ट नहीं है। वे कहते हैं कि कृष्ण की रसमयी लीलाभूमि ही नहीं, जहां-जहां से श्रीकृष्ण का रथ गुजरा है, जहां वह बसे हैं और जहां-जहां तक उनकी गीता का संदेश गया है, वह सब ब्रज ही है। अर्थात ब्रज ससीम नहीं, असीम है। वह नयन-पथगामी भी है और पलक-कपाट लगाने के बाद भावुकों के भावना-जगत में भी अखंड रूप से विद्यमान है।
भारत में ब्रजभाषा कहां नहीं रची गई ? कहां बोली और समझी नहीं गई ? भारत के किस क्षेत्र ने अपने को ब्रजमय अनुभव नहीं किया ? कहां से आध्यात्मिक आचार्यों ने यह स्वीकार नहीं किया कि ब्रज के अवतारी महापुरुष ही कृष्णस्तु भगवान स्वयं ? इस मान्यता पर आगे बढ़ें तो एशिया में महाभारत की कथाओं के रूप में और शेष विश्व में हरे राम, हरे कृष्ण आंदोलन के रूप में ब्रज दुनिया के किस छोर में व्याप्त नहीं है ? इस व्यापकता का रहस्य क्या है ? इस पर विचार करें।
भारत मां का हृदय
भौगोलिक दृष्टि से देखें तो ब्रज भारत का हृदयस्थल है। ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो भारत की दो-दो राजधानियों दिल्ली और आगरा के बीच में अवस्थित मुख्य ब्रज भारत की कर्मस्थली, योगस्थली, भक्तिस्थली, साधनास्थली ही नहीं, रंगस्थली और शक्तिस्थली भी रहा है। ज्ञात इतिहास में जितने व्यापक आयामों से भांति-भांति के द्वंद्व, युद्ध, जय-पराजय, उत्थान-पतन और विनाश एवं निर्माण के जितने विविध आयामों से यह ब्रज गुजरा है
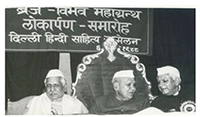 तथा बिगड़-बिगड़कर बना है और आज की अभावग्रस्त परिस्थितियों में भी अपने अस्तित्व को बनाए रखकर सिर ऊंचा करके खड़ा हुआ है, उसे कौन भूल सकता है ? उसे कैसे भुलाया जा सकता है ? ब्रज भारत की महत्ता का, राष्ट्र की सांस्कृतिक एकता का, साहित्य का, कला का और अध्यात्म का प्रतीक है। भारत माता का हृदय है न। इसके स्पंदनों से ही संपूर्ण राष्ट्र में शुद्ध रक्त का, अजस्र ऊर्जा का और दिव्यता का अखंड रस प्रवाहित हुआ है। पूछो दक्षिण के आचार्यों से। महाराष्ट्र के संतों से। गुजरात के आवाल-वृद्ध नर-नारियों से। गिरिधर गोपाल के रंग में रंगी मीरा के प्रदेश राजस्थान से। गुरुओं के प्रदेश पंजाब से। वैष्णो देवी की भूमि जम्मू-कश्मीर से। ‘भज गोविंदम् ! भज गोविंदम् !!’ के गायक आदि शंकराचार्य के प्रदेश केरल से। राधाकुंड और गोवर्धन में अपनी इहलीला समाप्त करने वाले उड़ीसावासियों से। ब्रजबुलि में रचना करने वाले पूर्वांचल प्रदेशों से। ब्रज का ग्वालबाल बनने की कामना करने वाले विश्ववंद्य कवींद्र रवींद्र से। महाकवि सुब्रह्मण्यम भारती से। महारास को अपना महाप्राण अनुभव करने वाले मणिपुर के लोगों से। और किससे नहीं ? सभी यह कहते सुने जाएंगे -‘मोहि ब्रज बिसरत नाहिं।’
तथा बिगड़-बिगड़कर बना है और आज की अभावग्रस्त परिस्थितियों में भी अपने अस्तित्व को बनाए रखकर सिर ऊंचा करके खड़ा हुआ है, उसे कौन भूल सकता है ? उसे कैसे भुलाया जा सकता है ? ब्रज भारत की महत्ता का, राष्ट्र की सांस्कृतिक एकता का, साहित्य का, कला का और अध्यात्म का प्रतीक है। भारत माता का हृदय है न। इसके स्पंदनों से ही संपूर्ण राष्ट्र में शुद्ध रक्त का, अजस्र ऊर्जा का और दिव्यता का अखंड रस प्रवाहित हुआ है। पूछो दक्षिण के आचार्यों से। महाराष्ट्र के संतों से। गुजरात के आवाल-वृद्ध नर-नारियों से। गिरिधर गोपाल के रंग में रंगी मीरा के प्रदेश राजस्थान से। गुरुओं के प्रदेश पंजाब से। वैष्णो देवी की भूमि जम्मू-कश्मीर से। ‘भज गोविंदम् ! भज गोविंदम् !!’ के गायक आदि शंकराचार्य के प्रदेश केरल से। राधाकुंड और गोवर्धन में अपनी इहलीला समाप्त करने वाले उड़ीसावासियों से। ब्रजबुलि में रचना करने वाले पूर्वांचल प्रदेशों से। ब्रज का ग्वालबाल बनने की कामना करने वाले विश्ववंद्य कवींद्र रवींद्र से। महाकवि सुब्रह्मण्यम भारती से। महारास को अपना महाप्राण अनुभव करने वाले मणिपुर के लोगों से। और किससे नहीं ? सभी यह कहते सुने जाएंगे -‘मोहि ब्रज बिसरत नाहिं।’
जब से हड़प्पा और मोहनजोदड़ो तथा सिंधुघाटी की सभ्यता की खोज का सिलसिला प्रारंभ हुआ है, तब से पुरातत्ववेत्ताओं का ध्यान ब्रज के भग्नावशेषों, चैत्यों, स्तूपों, टीलों, प्राप्त मूर्तियों पर गया है। फलस्वरूप उत्खनन पर उत्खनन की श्रृंखलाओं से प्राप्त प्रागैतिहासिक सामग्रियां यह सिद्ध करती जाती हैं कि भारत की केंद्रीय संस्कृति और इतिहास के जितने अनूठे रत्न ब्रज-वसुंधरा में छिपे हैं, उतने भारत में कदाचित कहीं नहीं। पूछो ह्वेनसांग से। जानो फाह्यान से। मुगलकाल में बादशाहों द्वारा लिखी या लिखवाई गई तवारीखों से। जानो ग्राउस क्या कहता है। ग्रियर्सन क्या कह गए हैं ? और कुछ नहीं तो प्राचीन ब्रज-वैभव के दर्शन के लिए एक बार मथुरा के पुरातात्विक संग्रहालय में मत्था अवश्य टेक लीजिए। ब्रज की कला और संस्कृति की उपलब्धियों की एक छोटी-सी मनोहर झांकी से ही आपका मन गौरवान्वित और तृप्त हो जाएगा। यह तो प्रथम चरण है, शुभारंभ है। उत्खनन, अन्वेषण और अनुशीलन होता रहे तो ब्रज की सांस्कृतिक धरोहर के ऐसे चार संग्रहालय और स्थापित किए जा सकते हैं, जो निश्चय ही कालांतर में यह सिद्ध करने में समर्थ होंगे कि भारतीय सभ्यता, संस्कृति, इतिहास और कलाओं का केंद्र पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण से अधिक वास्तविक रूप में ब्रजभूमि में ही अवस्थित था और है।
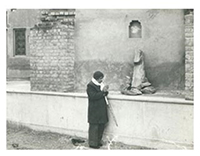 वैदिक अवधारणा के अनुसार ब्रज गोलोक रहा है। यहां के लंबे-लंबे सींगोंवाली पुष्ट गायों, गोचर-भूमि और मनोरम प्राकृतिक छटा को देखने के लिए देवता भी तरसते थे। वैष्णवों के मतानुसार भी ब्रज भूतल पर गोलोकधाम है। मथुरा बैकुण्ठपुरी है। गोपियां वेदों की ऋचाएं हैं। ग्वालबाल वैकुंठनाथ के पार्षदों के रूप में यहां अवतरित हुए थे। राजनीतिक दृष्टि से देखें तो पश्चिम की ओर से आने वाले आक्रांताओं ने जब तक दिल्ली और आगरा अर्थात ब्रज क्षेत्र पर फतहयाबी हासिल नहीं कर ली, तब तक वे जहांपनाह, शहंशाह और अकबर नहीं बन पाए। डच, पुर्तगाली और फ्रांसीसी छोटे-छोटे क्षेत्रों पर कब्जा करके बैठ गए और ब्रज की ओर नहीं बढ़े तो उन्हें महत्व नहीं मिला। अंग्रेज भी जब तक कलकत्ता को राजधानी बनाए रहे, भारत के शासक नहीं हो सके। ब्रज को कब्जाकर ही जब उन्होंने दिल्ली-तख्त को कायम किया, तभी उन्हें भारतेंदु का आशीर्वाद प्राप्त हुआ- ‘पूरी अमी की कटोरिया सी चिरजीवी रहौ विक्टोरिया रानी।’ तभी रवींद्रनाथ ठाकुर ने ब्रिटिश सम्राट की स्तुति में वह गीत गाया जो आज भारत का राष्ट्रगान बना हुआ है-‘जन-गण-मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता।’
वैदिक अवधारणा के अनुसार ब्रज गोलोक रहा है। यहां के लंबे-लंबे सींगोंवाली पुष्ट गायों, गोचर-भूमि और मनोरम प्राकृतिक छटा को देखने के लिए देवता भी तरसते थे। वैष्णवों के मतानुसार भी ब्रज भूतल पर गोलोकधाम है। मथुरा बैकुण्ठपुरी है। गोपियां वेदों की ऋचाएं हैं। ग्वालबाल वैकुंठनाथ के पार्षदों के रूप में यहां अवतरित हुए थे। राजनीतिक दृष्टि से देखें तो पश्चिम की ओर से आने वाले आक्रांताओं ने जब तक दिल्ली और आगरा अर्थात ब्रज क्षेत्र पर फतहयाबी हासिल नहीं कर ली, तब तक वे जहांपनाह, शहंशाह और अकबर नहीं बन पाए। डच, पुर्तगाली और फ्रांसीसी छोटे-छोटे क्षेत्रों पर कब्जा करके बैठ गए और ब्रज की ओर नहीं बढ़े तो उन्हें महत्व नहीं मिला। अंग्रेज भी जब तक कलकत्ता को राजधानी बनाए रहे, भारत के शासक नहीं हो सके। ब्रज को कब्जाकर ही जब उन्होंने दिल्ली-तख्त को कायम किया, तभी उन्हें भारतेंदु का आशीर्वाद प्राप्त हुआ- ‘पूरी अमी की कटोरिया सी चिरजीवी रहौ विक्टोरिया रानी।’ तभी रवींद्रनाथ ठाकुर ने ब्रिटिश सम्राट की स्तुति में वह गीत गाया जो आज भारत का राष्ट्रगान बना हुआ है-‘जन-गण-मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता।’
ब्रज एक भावलोक
 क्यों भारत का जन-गण-मन ब्रज वसुंधरा की ओर आकृष्ट हुआ ? क्यों शताब्दियों तक ब्रजभाषा भारत की साहित्यिक भाषा रही ? क्यों उसके दोहे, सवैये, कवित्त और छंद भारतीयों के कंठहार बन बैठे ? क्यों भारतीय संगीत ने अद्यतन अपनी गायकी के लिए ब्रजभाषा को वरण कर रखा है ? क्यों भारत के लाखों-लाखों लोग प्रतिवर्ष ब्रज की ओर अनंत कष्ट और असुविधाएं झेलकर भी दौड़ते हैं ? क्यों प्रदूषण से युक्त यमुना और कुंड-सरोवरों में आचमन और स्नान करके अपने को धन्य मानते हैं ? ब्रज-रज जहां अब कहने को ही बची है, क्यों उसमें लेट-लेटकर गिरिराज गोवर्धन की सात कोस की दंडौती परिक्रमा करते हैं ? क्यों गर्मियों में छोटे से नाले की तरह बहने वाली यमुना के संबंध में कहते हैं-‘तेरौ दरस मोहे भावै श्रीयमुने’ ? क्यों लिखा वल्लभाचार्य ने ‘यमुनाष्टक’-‘नमामि यमुनामहम् सकल सिद्धि हेतुम् मुदा’ ? क्यों एक छोटी-सी पहाड़ी को लोग गिरिराज महाराज कहते हैं ? क्यों ‘बोलंत हेला, बचनंत गारी’ के लिए प्रसिद्ध ब्रजवासियों को कहा गया-‘ब्रज के परम सनेही लोग’? धर्म की दुकानों पर लुटते-पिटते और आज के यथार्थ से सुपरिचित व्यक्तियों की भी यही आकांक्षा है-“एहो विधिना तोपै अंचरा पसारकर मांगत हौं, जनम-जनम दीजो मोहि याही ब्रज बसिबौ।” क्यों रसखान नंद की गायें बनाना चाहते हैं ? क्यों पंछी बनकर ब्रज के वृक्षों पर बसेरा करने की कामना करते हैं ? यदि पत्थर भी बनना पड़े तो उनकी प्रार्थना है कि गिरि गोवर्धन की शिला उन्हें ही बनाया जाए ? क्या ये मात्र पद्य या गीत हैं ? केवल कविता कहेंगे इन्हें ? नहीं, यह ब्रज का भावलोक है। इसका भूगोल, इतिहास, राजनीति और भौतिकता से कोई संबंध नहीं, रसिकों और भक्तों के हृदय में ब्रज आनंदधाम के रूप में अवस्थित है। इस आनंदधाम में ही उनके सच्चिदानंद आनंदकंद श्री कृष्णचंद्र अहर्निश निवास करते हैं। अनहद नाद की तरह उनकी मनोहर मुरलिया मन-प्राण में गूंजा करती है। नयनों में उन्हीं की छवि छाई रहती है। गाते हैं-‘बसो मेरे नैनन में नंदलाल।’ या ‘मेरे तो गिरिधर गुपाल, दूसरो न कोई।’ सूरदास इसी अद्वैत भाव को आंतरिक आस्था से अभिव्यक्त करते हुए इस तरह कहते हैं -“उधो, मन न भए दस-बीस। एक हुतौ सो गयौ स्याम संग, को आराधै ईस ?” वैष्णव आचार्य लिख गए हैं-‘कृष्णएव गतिर्मम’ और वल्लभाचार्य गीता के अंतिम श्लोक ”यत्र योगेश्वरः पार्थो धनुर्धराः। तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम।” के आधार पर अपने अनुयायियों को मंत्र देते हैं -‘श्री कृष्ण शरणम् मम।’ इस तरह ब्रज की गीता ही श्री कृष्ण के उपदेश के रूप में सर्वमान्य सर्वधर्म-ग्रंथ बन गई है।
क्यों भारत का जन-गण-मन ब्रज वसुंधरा की ओर आकृष्ट हुआ ? क्यों शताब्दियों तक ब्रजभाषा भारत की साहित्यिक भाषा रही ? क्यों उसके दोहे, सवैये, कवित्त और छंद भारतीयों के कंठहार बन बैठे ? क्यों भारतीय संगीत ने अद्यतन अपनी गायकी के लिए ब्रजभाषा को वरण कर रखा है ? क्यों भारत के लाखों-लाखों लोग प्रतिवर्ष ब्रज की ओर अनंत कष्ट और असुविधाएं झेलकर भी दौड़ते हैं ? क्यों प्रदूषण से युक्त यमुना और कुंड-सरोवरों में आचमन और स्नान करके अपने को धन्य मानते हैं ? ब्रज-रज जहां अब कहने को ही बची है, क्यों उसमें लेट-लेटकर गिरिराज गोवर्धन की सात कोस की दंडौती परिक्रमा करते हैं ? क्यों गर्मियों में छोटे से नाले की तरह बहने वाली यमुना के संबंध में कहते हैं-‘तेरौ दरस मोहे भावै श्रीयमुने’ ? क्यों लिखा वल्लभाचार्य ने ‘यमुनाष्टक’-‘नमामि यमुनामहम् सकल सिद्धि हेतुम् मुदा’ ? क्यों एक छोटी-सी पहाड़ी को लोग गिरिराज महाराज कहते हैं ? क्यों ‘बोलंत हेला, बचनंत गारी’ के लिए प्रसिद्ध ब्रजवासियों को कहा गया-‘ब्रज के परम सनेही लोग’? धर्म की दुकानों पर लुटते-पिटते और आज के यथार्थ से सुपरिचित व्यक्तियों की भी यही आकांक्षा है-“एहो विधिना तोपै अंचरा पसारकर मांगत हौं, जनम-जनम दीजो मोहि याही ब्रज बसिबौ।” क्यों रसखान नंद की गायें बनाना चाहते हैं ? क्यों पंछी बनकर ब्रज के वृक्षों पर बसेरा करने की कामना करते हैं ? यदि पत्थर भी बनना पड़े तो उनकी प्रार्थना है कि गिरि गोवर्धन की शिला उन्हें ही बनाया जाए ? क्या ये मात्र पद्य या गीत हैं ? केवल कविता कहेंगे इन्हें ? नहीं, यह ब्रज का भावलोक है। इसका भूगोल, इतिहास, राजनीति और भौतिकता से कोई संबंध नहीं, रसिकों और भक्तों के हृदय में ब्रज आनंदधाम के रूप में अवस्थित है। इस आनंदधाम में ही उनके सच्चिदानंद आनंदकंद श्री कृष्णचंद्र अहर्निश निवास करते हैं। अनहद नाद की तरह उनकी मनोहर मुरलिया मन-प्राण में गूंजा करती है। नयनों में उन्हीं की छवि छाई रहती है। गाते हैं-‘बसो मेरे नैनन में नंदलाल।’ या ‘मेरे तो गिरिधर गुपाल, दूसरो न कोई।’ सूरदास इसी अद्वैत भाव को आंतरिक आस्था से अभिव्यक्त करते हुए इस तरह कहते हैं -“उधो, मन न भए दस-बीस। एक हुतौ सो गयौ स्याम संग, को आराधै ईस ?” वैष्णव आचार्य लिख गए हैं-‘कृष्णएव गतिर्मम’ और वल्लभाचार्य गीता के अंतिम श्लोक ”यत्र योगेश्वरः पार्थो धनुर्धराः। तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम।” के आधार पर अपने अनुयायियों को मंत्र देते हैं -‘श्री कृष्ण शरणम् मम।’ इस तरह ब्रज की गीता ही श्री कृष्ण के उपदेश के रूप में सर्वमान्य सर्वधर्म-ग्रंथ बन गई है।
ब्रज को जानना है, तो श्रीकृष्ण को जानना ही पड़ेगा। गोपालक के रूप में सही। कृषि के उन्नायक के रूप में सही। ब्रज के लोकनायक के रूप में सही। ललित लीलाधर के रूप में सही। आतताइयों के संहारक के रूप में ही सही। राष्ट्र को समृद्धि के शिखर तक पहुंचाने वाले द्वारावती के संस्थापक के रूप में ही सही। साम्राज्यवाद के विरुद्ध लोकतंत्र और समाजवाद की प्रतिष्ठा करने वाले महापुरुष के रूप में ही सही। परम आसक्ति और चरम निरासक्ति को अपने दोनों हाथों में धारण करने वाले नर-नारायण के रूप में ही सही। महापुरुष और महानेता ही सही। भगवान ही सही। श्रीकृष्ण के बिना ब्रज के मानस में प्रविष्ट होने की कोई अन्य राह ही नहीं है। जिज्ञासुओं को, चाहे वे नास्तिक हों या आस्तिक, ब्रज-तत्व को जानने के लिए श्रीकृष्ण की शरण में जाना ही होगा।
ब्रज का संदेश
क्या है श्री कृष्ण के रूप में ब्रज का संदेश ? कर्म के प्रति आसक्त होते हुए भी निरासिक्त का शाश्वत भाव। रूप, माधुर्य, स्नेह और संयोग में से गुजरते हुए चिरविरह की लालसा। यह विरह ही योग है। यह विरह ही भक्ति है। यह विरह ही जीवन-दर्शन है। यही साहित्य का शाश्वत सत्य है। यही ब्रजवल्लभियों और उनकी स्वामिनी राधारानी का सच्चा स्वरूप है। यही भुक्ति के साथ-साथ मुक्ति का मार्ग भी है।
आज के संदर्भ में यदि इस संदेश को और अधिक नामांकित करना चाहें तो है-‘चरैवेति चरैवेति’। चलते चलो, बढ़ते चलो ! क्योंकि यही जीवन की गति है, प्रगति है। बिना थके चलो। आनंद के साथ बढ़ो। परम आनंद की ओर बढ़ो। श्रीकृष्ण का जीवन-वृत्त यही तो कहता है-जन्म लेते ही मथुरा के कारागार से चल पड़े। बाल्यावस्था से निकलते ही वृंदावन की ओर चल पड़े। तरुणाई आते ही मथुरा की ओर गमन किया। मथुरा में नहीं रुके, चल पड़े द्वारावती की ओर। वहां का वैभव भी उन्हें नहीं बांध सका। वह चलते रहे हस्तिनापुर की ओर, इंद्रप्रस्थ की ओर। जहां-जहां व्यथा-पीड़ित पांडवों को जाना पड़ा, उनकी ओर। धर्मराज के अनुज महाबाहु अर्जुन की सहायता के लिए देश-देशांतरों की ओर। यानी महाभारत की ओर। फिर अपने रथ पर बिठाकर अर्जुन को ले चले कौरव-पांडवों की सेना के मध्य की ओर। अपने सखा और भक्त अर्जुन को ले चले विरक्ति से हटाकर योग की ओर। अकर्मण्यता के बोध को नष्ट करके कर्मयोग की ओर। कर्म को ले चले संघर्ष की ओर। यहीं नहीं रुके, ईश्वर की विराट विभुता का दर्शन कराकर ले चले अर्जुन को अपनी, यानी अनंत सत्ता की ओर। पांडवों को चक्रवर्ती राज देकर भी वह उनके पास नहीं रुके। लौट चले द्वारिका की ओर। धन, वैभव, सुरा और सुंदरियों के जाल में फंसे अहंकारी यादवों को अंत में ले चले विनाश-सागर की ओर-चलो आपस में ही लड़ मरो। भौतिक संपत्ति अंत में विनाश का कारण होती है-चलते-चलते कह गए श्रीकृष्ण। ऐसा अदभुत व्यक्तित्व, ऐसा संपूर्ण कलाओं से युक्त, लोकरंजक, लोकरक्षक और सच्चिदानंद संदोह ब्रज के अतिरिक्त किसी और ने अवतरित किया है ? यही ब्रज का महत्व है। यही ब्रज का संदेश है। शेष ब्रज-महिमा तो इस ग्रंथ के पृष्ठ-पृष्ठ पर स्वर्णाक्षरों की तरह अंकित है। कहने को बहुत है। क्या-क्या कहें ? यहां तो केवल इतना ही कहते हैं-‘कहां लौं कहिए ब्रज की बात।’
(संपादित ग्रंथ- ‘ब्रजव विभव’ से, सन् 1987 )