 कहते सुनेंगे, मेरी कहानी ? इतनी फुरसत है आपको ? लोग आम खाते हैं, पेड़ नहीं गिनते। अखबार पढ़ते हैं, लेकिन पत्र-पत्रिकाओं के लिए कितने लोग मर-खपकर नींव की ईंट बन गए हैं, इसे नहीं जानते। जानना कोई जरूरी भी नहीं। ताजमहल सुंदर है। कुतुबमीनार बहुत ऊंची है। चित्तौड़गढ़ का किला बड़ा विशाल है। ब्रह्मपुत्र नदी बड़ी लंबी है। प्रयाग में किले के नीचे यमुना बहुत गहरी है। इतना जान लेना ही क्या कोई कम है। दुनिया में एक-से-एक बड़े शिल्पी, चित्रकार, कवि, कलाकार और महापुरुष होगए हैं। कौन इन्हें खोजे और कौन इनके करतबों पर जाए ? आज के आदमी को अपनी राम कहानी से ही फुरसत कहां है ? फिर मेरी कर्म-कहानी ! न मैं कोई बड़ा कवि, न उल्लेखनीय लेखक और न ही ऐसा पत्रकार कि जिसकी कलम ने कोई धुआंधार करिश्मा ही करके दिखा दिया हो, फिर ऐसी क्या मुसीबत आ पड़ी है कि मेरी कहानी आप सुनें-ही-सुनें ?
कहते सुनेंगे, मेरी कहानी ? इतनी फुरसत है आपको ? लोग आम खाते हैं, पेड़ नहीं गिनते। अखबार पढ़ते हैं, लेकिन पत्र-पत्रिकाओं के लिए कितने लोग मर-खपकर नींव की ईंट बन गए हैं, इसे नहीं जानते। जानना कोई जरूरी भी नहीं। ताजमहल सुंदर है। कुतुबमीनार बहुत ऊंची है। चित्तौड़गढ़ का किला बड़ा विशाल है। ब्रह्मपुत्र नदी बड़ी लंबी है। प्रयाग में किले के नीचे यमुना बहुत गहरी है। इतना जान लेना ही क्या कोई कम है। दुनिया में एक-से-एक बड़े शिल्पी, चित्रकार, कवि, कलाकार और महापुरुष होगए हैं। कौन इन्हें खोजे और कौन इनके करतबों पर जाए ? आज के आदमी को अपनी राम कहानी से ही फुरसत कहां है ? फिर मेरी कर्म-कहानी ! न मैं कोई बड़ा कवि, न उल्लेखनीय लेखक और न ही ऐसा पत्रकार कि जिसकी कलम ने कोई धुआंधार करिश्मा ही करके दिखा दिया हो, फिर ऐसी क्या मुसीबत आ पड़ी है कि मेरी कहानी आप सुनें-ही-सुनें ?
फिर भी सुन ही लीजिए। आखिर विविध भारती के गानों के बीच आप अवांछित विज्ञापन सुनते ही हैं। जनसभाओं में मनपसंद वक्ता से पहले, समय काटने वाले नेताओं, उपनेताओं और भीड़ को बहलाने वाले जोकरों की तकरीर सुनने और देखने की भी तकलीफ़ आप गवारा कर ही लेते हैं। दावतों में मिष्ठान्न से पहले भांति-भांति के खट्टे-चरपरे और पेट-भराऊ पदार्थों से काम निकालते ही हैं। राम-राज्य की लालसा में स्वराज्य से पूर्व तथा स्वराज्य के बाद सब कुछ झेलते-सहते ही आए हैं, तो एक मुसीबत यह भी सही।
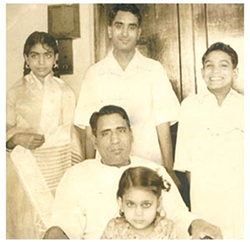 मेरी कहानी में शैतानों का जिक्र आएगा। लेकिन ये शैतान की आंत नहीं है। यह एक छोटे-से आदमी की छोटी-सी कहानी है। ऐसे आदमी की कहानी, जिसने पढ़ाई की कोई डिग्री प्राप्त नहीं की। जो किसी बड़े बाप का बेटा, या किसी बड़े या मंझोले नेता की पत्नी का सगा या मुंहबोला भाई भी नहीं। जिसका संबंध राजनीति के इस या उस दल के साथ भी नहीं जुड़ा। या जो स्वराज्य से पहले या उसके बाद किसी आंदोलन में जेल जाने का सर्टिफिकेट भी प्राप्त नहीं कर सका। हमारे देश में बिना जेल गए कोई बड़ा आदमी बना है ? बिना पद से हटे या हटाए कोई चर्चित हुआ है ? पत्रकार तो हमारे देश में बस वही उल्लेखनीय होता है, जिसे या तो सरकार अपना ले, या उसे किसी महाशक्ति का प्रत्यक्ष या परोक्ष समर्थन प्राप्त हो। वह प्रायः नामधारी प्रधान संपादक होता है या राजनीतिक दलों और विदेशी एजेंटों का चहेता। उसी की आज़ादी पर अखबार की आज़ादी निर्भर है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का आंदोलन भी सिर्फ इसी वर्ग के लिए है। अगर मैं वह होगया होता, तो मेरी कहानी भी कहने और सुनने योग्य बन जाती।
मेरी कहानी में शैतानों का जिक्र आएगा। लेकिन ये शैतान की आंत नहीं है। यह एक छोटे-से आदमी की छोटी-सी कहानी है। ऐसे आदमी की कहानी, जिसने पढ़ाई की कोई डिग्री प्राप्त नहीं की। जो किसी बड़े बाप का बेटा, या किसी बड़े या मंझोले नेता की पत्नी का सगा या मुंहबोला भाई भी नहीं। जिसका संबंध राजनीति के इस या उस दल के साथ भी नहीं जुड़ा। या जो स्वराज्य से पहले या उसके बाद किसी आंदोलन में जेल जाने का सर्टिफिकेट भी प्राप्त नहीं कर सका। हमारे देश में बिना जेल गए कोई बड़ा आदमी बना है ? बिना पद से हटे या हटाए कोई चर्चित हुआ है ? पत्रकार तो हमारे देश में बस वही उल्लेखनीय होता है, जिसे या तो सरकार अपना ले, या उसे किसी महाशक्ति का प्रत्यक्ष या परोक्ष समर्थन प्राप्त हो। वह प्रायः नामधारी प्रधान संपादक होता है या राजनीतिक दलों और विदेशी एजेंटों का चहेता। उसी की आज़ादी पर अखबार की आज़ादी निर्भर है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का आंदोलन भी सिर्फ इसी वर्ग के लिए है। अगर मैं वह होगया होता, तो मेरी कहानी भी कहने और सुनने योग्य बन जाती।
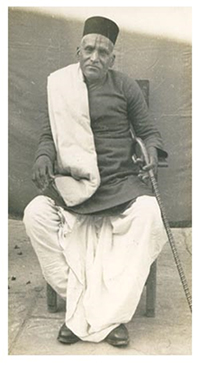 मैं आपको अच्छी तरह जानता हूं कि आप ऐसे रोग के रोगी हैं, जो अपना ध्यान एक जगह केंद्रित नहीं कर सकते। दैनिक पत्रों, साप्ताहिकों और मासिकों में आपकी रुचि सिर्फ इतनी ही रह गई है कि चलते-फिरते उनके शीर्षक देख लिए, कला के नाम पर कोई नंगी-अधनंगी तस्वीर मिली तो उसे घूर लिया, कहीं कोई निंदा-रस प्राप्त हुआ तो उसकी चुस्की ले ली और जुट गए बैल की तरह जीवन के कोल्हू में। मरीज़ अच्छा हो या न हो, मरे या तड़फड़ाता रहे, मेरे हाथ कलम का इंजेक्शन लग गया है, मैं उसे आपको ठोकूंगा ही। क्योंकि मैं यह भी जान गया हूं कि आपकी सहनशक्ति बड़ी अदभुत है। कितनी महामारियां इस देश में आईं, आप बच ही गए। हर साल सूखा, बाढ़, लू और शीतलहर आती है और चली जाती है, फिर भी आप जिंदा हैं। अन्याय, जुल्म और सितम तो आप हजारों वर्षों से सहते रहे हैं। आपने अंग्रेज भी सहे और अंग्रेजी भी सह रहे हैं। आपको पराधीनता का भी अहसास है और आज की स्वतंत्रता का भी, आपात्काल में भी आप शांत रहे और मंहगाई, मुद्रास्फीति तथा लूटमार और बलात्कार भी आपको क्लांत नहीं कर सके हैं। आपकी स्थितप्रज्ञता को नमस्कार करते हुए मैं अपनी कलम उठा रहा हूं।
कहीं आप दोष निकालने लगें, इसलिए पहले स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि पढ़ाई के नाम पर मुझे मिडिल का भी सर्टिफिकेट प्राप्त नहीं। न मैंने पूरी तरह गांधी को पढ़ा है और न मार्क्स को। पूंजी एकत्र करने की तमन्ना आपकी तरह मेरे मन में भी अवश्य रही है, लेकिन न मेरे पास साहित्य की पूंजी है और न पूंजीवाद का तत्वज्ञान ही है। पंडितजी के घर में पैदा हुआ हूं, पर संस्कृत का पंडित नहीं। मुस्लिम जनसंपर्क साधा है, लेकिन उर्दू अदब में मेरी पैठ नहीं। बाबू श्यामसुंदर दास, बी.ए., बाबू गुलाबराय, एम. ए. और अंग्रेजी पढ़ाते-पढ़ाते हिन्दी के डॉक्टर बने नगेन्द्र के साथ मेरी अच्छी-खासी बनी है। पत्रकारिता के पच्चीसों प्रकाश स्तंभों जैसे नेशनल हेरल्ड के चेलापति राव, मालिक संपादक या हिंदुस्तान टाइम्स के दुर्गादास, इंडियन एक्सप्रेस के मुलगांवकर, टाइम्स ऑफ इंडिया के श्यामलाल एवं कार्टूनिस्ट शंकर, अहमद, संतानम कृपानिधि, कल्हण और श्यामाचरण काला आदि से मेरी भेंट कामचलाऊ रही है। मेरे अंग्रेजी अज्ञान को दूर करने के लिए संपादक शिरोमणि पं. बनारसीदास चतुर्वेदी ने एक नुस्खा तज़वीज़ किया था कि मैं किसी एंग्लो-इंडियन लड़की से दोस्ती कर लूं, तो मेरी अंग्रेजी फर्राटेदार बन जाएगी, लेकिन इसका भी डौल नहीं बैठा।
मैं आपको अच्छी तरह जानता हूं कि आप ऐसे रोग के रोगी हैं, जो अपना ध्यान एक जगह केंद्रित नहीं कर सकते। दैनिक पत्रों, साप्ताहिकों और मासिकों में आपकी रुचि सिर्फ इतनी ही रह गई है कि चलते-फिरते उनके शीर्षक देख लिए, कला के नाम पर कोई नंगी-अधनंगी तस्वीर मिली तो उसे घूर लिया, कहीं कोई निंदा-रस प्राप्त हुआ तो उसकी चुस्की ले ली और जुट गए बैल की तरह जीवन के कोल्हू में। मरीज़ अच्छा हो या न हो, मरे या तड़फड़ाता रहे, मेरे हाथ कलम का इंजेक्शन लग गया है, मैं उसे आपको ठोकूंगा ही। क्योंकि मैं यह भी जान गया हूं कि आपकी सहनशक्ति बड़ी अदभुत है। कितनी महामारियां इस देश में आईं, आप बच ही गए। हर साल सूखा, बाढ़, लू और शीतलहर आती है और चली जाती है, फिर भी आप जिंदा हैं। अन्याय, जुल्म और सितम तो आप हजारों वर्षों से सहते रहे हैं। आपने अंग्रेज भी सहे और अंग्रेजी भी सह रहे हैं। आपको पराधीनता का भी अहसास है और आज की स्वतंत्रता का भी, आपात्काल में भी आप शांत रहे और मंहगाई, मुद्रास्फीति तथा लूटमार और बलात्कार भी आपको क्लांत नहीं कर सके हैं। आपकी स्थितप्रज्ञता को नमस्कार करते हुए मैं अपनी कलम उठा रहा हूं।
कहीं आप दोष निकालने लगें, इसलिए पहले स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि पढ़ाई के नाम पर मुझे मिडिल का भी सर्टिफिकेट प्राप्त नहीं। न मैंने पूरी तरह गांधी को पढ़ा है और न मार्क्स को। पूंजी एकत्र करने की तमन्ना आपकी तरह मेरे मन में भी अवश्य रही है, लेकिन न मेरे पास साहित्य की पूंजी है और न पूंजीवाद का तत्वज्ञान ही है। पंडितजी के घर में पैदा हुआ हूं, पर संस्कृत का पंडित नहीं। मुस्लिम जनसंपर्क साधा है, लेकिन उर्दू अदब में मेरी पैठ नहीं। बाबू श्यामसुंदर दास, बी.ए., बाबू गुलाबराय, एम. ए. और अंग्रेजी पढ़ाते-पढ़ाते हिन्दी के डॉक्टर बने नगेन्द्र के साथ मेरी अच्छी-खासी बनी है। पत्रकारिता के पच्चीसों प्रकाश स्तंभों जैसे नेशनल हेरल्ड के चेलापति राव, मालिक संपादक या हिंदुस्तान टाइम्स के दुर्गादास, इंडियन एक्सप्रेस के मुलगांवकर, टाइम्स ऑफ इंडिया के श्यामलाल एवं कार्टूनिस्ट शंकर, अहमद, संतानम कृपानिधि, कल्हण और श्यामाचरण काला आदि से मेरी भेंट कामचलाऊ रही है। मेरे अंग्रेजी अज्ञान को दूर करने के लिए संपादक शिरोमणि पं. बनारसीदास चतुर्वेदी ने एक नुस्खा तज़वीज़ किया था कि मैं किसी एंग्लो-इंडियन लड़की से दोस्ती कर लूं, तो मेरी अंग्रेजी फर्राटेदार बन जाएगी, लेकिन इसका भी डौल नहीं बैठा।
 मैं क्या हूं, इसे आप पहले अच्छी तरह जान लें। साहित्यकार मुझे पत्रकार समझते हैं और वे पत्रकारिता को साहित्य नहीं मानते। पत्रकार मुझे साहित्यकार मानते हैं। उनका मत है कि साहित्यिक भाषा, कला-कल्पना की उड़ान और ख्याली दुनिया का आदमी, पत्रकारिता के लिए ‘मिसफिट’ है। इतना ही नहीं, कांग्रेसी मुझे भूतपूर्व जनसंघी समझते हैं। जनसंघियों का कहना है कि हम धोखा नहीं खा सकते, यह ऊपर से नीचे तक कांग्रेसी है। समाजवादी कहते हैं कि मैं ‘टंडनाइट’ हूं और ‘टंडनाइट’ कहते हैं कि भाषा के मसले पर यह ‘लोहियावादी’ है। साम्यवादी समझते हैं कि मैं पूंजीपतियों का एजेंट हूं और पूंजीपतियों ने यह खबर खोज निकाली है कि मैं मुंशी प्रेमचंद के ज़माने से ही प्रगतिशील लेखक संघ से कभी सीधा और कभी तिरछा संबद्ध रहा हूं। आज के लेखक मुझे पुराणपंथी या रीतिकालीन कहते हैं और पुराने लेखक यह मानते हैं कि मैं सींग कटाकर नये बछड़ों में शामिल होने का प्रयत्न करता रहा हूं। बात यहीं तक होती तो गनीमत थी। ब्रजवासी कहते हैं कि मैं ब्रज का हूं। राजस्थानी मानते हैं कि गौड़ ब्राह्मण और व्यास तो राजस्थान से गए हैं। आगरा, इटावा, इलाहाबाद और बनारस जहां-जहां मैं थोड़े-बहुत दिन रहा हूं, वे मुझे दिल्लीवासी मानने के लिए तैयार ही नहीं। दिल्ली के दिलवाले लोग तो अब मुझे दिल्लीवाला ही कहने लगे हैं। यानि एड़ी से लेकर चोटी तक मैं विवादग्रस्त आदमी हूं। यदि विवादग्रस्तता अपने-आप में कोई गुण है, यदि नहीं है तो वह मान ली जानी चाहिए, तो निस्संदेह मैं गुणी आदमी हूं। क्योंकि यदि मैं गुणी नहीं होता तो अपने लेखन और करतबों से लाखों-लाख नर-नारियों को कैसे मूर्ख बना सकता था ? कोई-न-कोई करामात मुझमें है अवश्य। इसी करामात को एक कथा के रूप में प्रस्तुत करने जा रहा हूं।
मैं क्या हूं, इसे आप पहले अच्छी तरह जान लें। साहित्यकार मुझे पत्रकार समझते हैं और वे पत्रकारिता को साहित्य नहीं मानते। पत्रकार मुझे साहित्यकार मानते हैं। उनका मत है कि साहित्यिक भाषा, कला-कल्पना की उड़ान और ख्याली दुनिया का आदमी, पत्रकारिता के लिए ‘मिसफिट’ है। इतना ही नहीं, कांग्रेसी मुझे भूतपूर्व जनसंघी समझते हैं। जनसंघियों का कहना है कि हम धोखा नहीं खा सकते, यह ऊपर से नीचे तक कांग्रेसी है। समाजवादी कहते हैं कि मैं ‘टंडनाइट’ हूं और ‘टंडनाइट’ कहते हैं कि भाषा के मसले पर यह ‘लोहियावादी’ है। साम्यवादी समझते हैं कि मैं पूंजीपतियों का एजेंट हूं और पूंजीपतियों ने यह खबर खोज निकाली है कि मैं मुंशी प्रेमचंद के ज़माने से ही प्रगतिशील लेखक संघ से कभी सीधा और कभी तिरछा संबद्ध रहा हूं। आज के लेखक मुझे पुराणपंथी या रीतिकालीन कहते हैं और पुराने लेखक यह मानते हैं कि मैं सींग कटाकर नये बछड़ों में शामिल होने का प्रयत्न करता रहा हूं। बात यहीं तक होती तो गनीमत थी। ब्रजवासी कहते हैं कि मैं ब्रज का हूं। राजस्थानी मानते हैं कि गौड़ ब्राह्मण और व्यास तो राजस्थान से गए हैं। आगरा, इटावा, इलाहाबाद और बनारस जहां-जहां मैं थोड़े-बहुत दिन रहा हूं, वे मुझे दिल्लीवासी मानने के लिए तैयार ही नहीं। दिल्ली के दिलवाले लोग तो अब मुझे दिल्लीवाला ही कहने लगे हैं। यानि एड़ी से लेकर चोटी तक मैं विवादग्रस्त आदमी हूं। यदि विवादग्रस्तता अपने-आप में कोई गुण है, यदि नहीं है तो वह मान ली जानी चाहिए, तो निस्संदेह मैं गुणी आदमी हूं। क्योंकि यदि मैं गुणी नहीं होता तो अपने लेखन और करतबों से लाखों-लाख नर-नारियों को कैसे मूर्ख बना सकता था ? कोई-न-कोई करामात मुझमें है अवश्य। इसी करामात को एक कथा के रूप में प्रस्तुत करने जा रहा हूं।
लेकिन ठहरिए, एक बात और सुन लीजिए। पिताजी मुझे संस्कृत का पंडित और मर्यादी वैष्णव बनाना चाहते थे।
नहीं बना। ब्रज के महान संगीतज्ञ ग्वारिया बाबा मुझे संगीत, नृत्य और नाटक में पारंगत देखना चाहते थे। उनकी साध पूरी नहीं हुई। भारत प्रसिद्ध चंद्रसेन उर्फ ‘भौंरा’ पहलवान ने मुझे अपना उत्तराधिकारी बनाने की ठानी थी, पर किसी से कुश्ती न हारने वाले मुझसे हार गए। भारत प्रसिद्ध शतरंज मार्तण्ड कृष्णकवि ने मुझे बड़ी चालें सिखाईं, वे भी मात खा गए। चक्रधारी नागा बाबा हरिदास मुझे तलवार, बनैटी, धनुर्विद्या और लाठी भांजने में अपने अखाड़े का खलीफा बनाने चले थे। बेचारे खुद अखाड़ा छोड़ गए। बाबू गुलाबराय, डॉ0 सत्येन्द्र, प्रकाशचंद्र गुप्ता, नंददुलारे वाजपेयी और शांतिप्रिय द्विवेदी सोचते थे कि यह व्यक्ति हिन्दी-समीक्षा-साहित्य में कुछ करके दिखाएगा, उनकी आशाओं पर भी तुषारापात हो गया। डॉ0 वासुदेवशरण अग्रवाल, सेठ कन्हैयालाल पोद्दार और ‘रसालजी’ सोचते थे कि मैं ब्रजभाषा और ब्रज साहित्य के लिए निश्चय ही कुछ कर पाऊंगा, वह भी संभव नहीं हुआ। बन गया मैं लुढ़कते-लुढ़कते, उठते-गिरते, घिस-पिटकर मन से कवि, ललक से लेखक और कर्म से पत्रकार।
कभी सोचा भी नहीं था कि मैं अपनी आपबीती लिखूंगा। वह तो भाई धर्मवीर भारती ने शुरू करा दी- 7 जून, 1981 से मेरे सात लेख लगातार ‘धर्मयुग’ में छापे। उनके बाद श्री गणेश मंत्री आए तो उन्होंने भी ‘धर्मयुग’ के लिए पांच लेख मांग लिए। इन्हें देखकर कुछ अन्य पत्र-पत्रिकाओं ने भी मुझसे संस्मरण चाहे। इस तरह पूरे बारह वर्षों में एक-एक करके, समय निकाल-निकालकर मैंने इस आपबीती को ‘कहो व्यास, कैसी कटी ?’ के रूप में पूरा किया है। क्योंकि ये निबंध अलग-अलग लिखे गए है, इसलिए घटनाओं और व्यक्तियों की चर्चा और पुनरावृत्ति आपको देखने को मिलेगी। जब इसे पुस्तकाकार करने का विचार मन में आया तब तक स्मृति तो जाग्रत थी, लेकिन सन्-संवत् और व्यक्तियों के नाम कभी-कभी तो बहुत सोचने पर भी याद नहीं आए। यह बात आपको खटक सकती है। एक बात और-यह पुस्तक बोलकर लिखवाई गई है। इसलिए बोलचाल की भाषा का मज़ा इसमें है। जब जो शब्द मन में आया वही लिखवाया। वह चाहे ब्रज का हो, हिन्दी का हो, उर्दू का हो या अंग्रेजी का । वैसे भी मैं यह मानता हूं कि हिन्दी भाषा को बहुभाषाओं में प्रचलित शब्दों से संपन्न होना ज़रूरी है। एक बात और बता दूं कि इन बारह वर्षों में मेरे बोले को लिखनेवाले बार-बार बदले हैं। मेरे लिखियाजनों की श्रेणी में कुमारी भी रही हैं और श्रीमती भी। कुछ ने कहने पर लिखा है और कुछ ने कर्तव्य मानकर रस लेकर लिखा है। महत्त्व व्यास का ही नहीं, सरस्वती और गणेश का भी है। मेरा एक स्वभाव यह भी है कि मेरा लिखिया प्रबुद्ध और आत्मीय होना चाहिए। यह प्रबुद्धता और आत्मीयता मुझे इस पुस्तक को अंतिम रूप देने वाले श्री देवराजेन्द्र से मिली है। गलतियां आप उनके खाते में डालिए और गुन-औगुन मेरे मत्थे मढ़िए। बहुत होगया, अब पुस्तक पढ़िए !
(‘कहो व्यास, कैसी कटी ?’, सन् 1994)