गोपालप्रसाद व्यास से साक्षात्कार
( श्री अशोक चक्रधर )
ब्रज के प्यारे, दिल्ली के दुलारे : व्यासजी हमारे
प्रश्न : व्यासजी, ‘कहो व्यास कैसी कटी’ के माध्यम से आपने हमको अपनी व्यथा तो दे दी, अब व्यथा की कथा में यह बताइए कि मैंने उसमें पढ़ा था कि बीस साल की उम्र तक आपने बनियान नहीं पहनी। इसके दो कारण हो सकते हैं, या तो आप ब्रज-संस्कृति में पले थे, वहां कोई बनियान पहनता ही नहीं था या कोई अभाव था, विपन्नता थी या क्या था ?
 उत्तर : अभाव नहीं था। नंगे पैर चलना और कम से कम कपड़े पहनना ब्रज की परंपरा रही है। मैंने बनियान क्या, कोई भी अधोवस्त्र जो बच्चे इस उम्र में पहना करते हैं, मैंने नहीं पहने, क्योंकि ब्रज की संस्कृति और ब्रज मेरे रोम-रोम में बसा हुआ है। ब्रज की मस्ती, ब्रज की लीला, ब्रज की ज़िदादिली, ब्रज का विनोद ही मेरे साहित्य की, व्यक्तित्व और कृतित्व की जान है।
उत्तर : अभाव नहीं था। नंगे पैर चलना और कम से कम कपड़े पहनना ब्रज की परंपरा रही है। मैंने बनियान क्या, कोई भी अधोवस्त्र जो बच्चे इस उम्र में पहना करते हैं, मैंने नहीं पहने, क्योंकि ब्रज की संस्कृति और ब्रज मेरे रोम-रोम में बसा हुआ है। ब्रज की मस्ती, ब्रज की लीला, ब्रज की ज़िदादिली, ब्रज का विनोद ही मेरे साहित्य की, व्यक्तित्व और कृतित्व की जान है।
प्रश्न : इसमें कोई संदेह नहीं। बालकृष्ण का रूप जब हम देखते हैं कि करधनी बंधी हुई है, बनियान-कच्छे वह भी कहां पहनते थे। जैसे बालकृष्ण की छवि संस्कृति की ओर ले जाती है, जहां हम करधनी बांधते हैं, काला डोरा पहनते हैं या दिठौना लगाती है मां। तो कुछ जो अंग पर होता था वह क्या होता था- डोरा, दिठौना या करधनी ?
 उत्तर : इस संदर्भ में तुलसीदासजी का एक पद्यांश देने लायक है कि “ठुमक चलत रामचन्द्र बाजत पैंजनिया, किलक किलक उठत धाय, गिरत भूमि लटपटाय………” तो ऐसा ही बस मेरे साथ हुआ है कि मेरी मां मुझको पैंजनिया पहनाकर नचाते-नचाते दादी के पास भेजती थी और दादी कहती थी कि अब तू बिना सहारे के नाचता-नाचता अपनी मां के पास जा, तो गिरता-पड़ता मां की गोद में जाकर छिप जाता था। ये तो ब्रज की संस्कृति है, कोई अभाव नहीं है।
उत्तर : इस संदर्भ में तुलसीदासजी का एक पद्यांश देने लायक है कि “ठुमक चलत रामचन्द्र बाजत पैंजनिया, किलक किलक उठत धाय, गिरत भूमि लटपटाय………” तो ऐसा ही बस मेरे साथ हुआ है कि मेरी मां मुझको पैंजनिया पहनाकर नचाते-नचाते दादी के पास भेजती थी और दादी कहती थी कि अब तू बिना सहारे के नाचता-नाचता अपनी मां के पास जा, तो गिरता-पड़ता मां की गोद में जाकर छिप जाता था। ये तो ब्रज की संस्कृति है, कोई अभाव नहीं है।
प्रश्न : मां के बारे में आपकी स्मृतियां कैसी हैं ? मां के पास जब आप “बाजत पैंजनिया ठुमक चलत रामचंद्र” के अंदाज़ में जाते थे और मां की गोदी में छिप जाते थे तो मां का वत्सल भाव निश्चित रूप से पाते थे। मां के किन गुणों को आप आज भी याद करते हैं ?
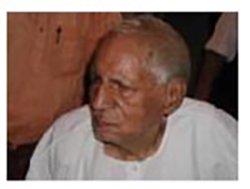 उत्तर : आपको इसकी भूमिका जाननी चाहिए कि मेरी मां जिसे मैं जीजी कहता था, सम्पन्न मायके वाली जैसी थीं, वहां पनिहारा भी था, चक्की पर आटा पिसता था और घर में नौकर-चाकर भी थे। लेकिन हमारे गांव में न चक्की थी और कुंआ तीन मील दूर पड़ता था, तो मेरी जीजी को पीसना भी पड़ता था, पानी भी भरना पड़ता था। तब उसे अपने मायके की सुध आती थी और वह कहती भी थी हमारे मायके में तो ऐसा है, यहां ऐसा नहीं है। तो मेरी दादी ने कहा कि जा अपने मायके में ही रह। देखते हैं मायके वाले तुझे कितने दिन रखते हैं। तो मुझको तो दादी ने छीन लिया और मां मेरी मायके चली गई। लेकिन मां ब्रज की परिक्रमा के बहाने गांव में आती थी और अपनी पुरानी सहेलियों से कहती थी कि मेरे गोपाल को कैसे भी मुझे दिखा दो। तब वह मुझे गोद में उठाकर खिड़की से दिखा देती थीं और मां विह्वल होकर मुझे देखती और लौटकर चली जाती थी।
उत्तर : आपको इसकी भूमिका जाननी चाहिए कि मेरी मां जिसे मैं जीजी कहता था, सम्पन्न मायके वाली जैसी थीं, वहां पनिहारा भी था, चक्की पर आटा पिसता था और घर में नौकर-चाकर भी थे। लेकिन हमारे गांव में न चक्की थी और कुंआ तीन मील दूर पड़ता था, तो मेरी जीजी को पीसना भी पड़ता था, पानी भी भरना पड़ता था। तब उसे अपने मायके की सुध आती थी और वह कहती भी थी हमारे मायके में तो ऐसा है, यहां ऐसा नहीं है। तो मेरी दादी ने कहा कि जा अपने मायके में ही रह। देखते हैं मायके वाले तुझे कितने दिन रखते हैं। तो मुझको तो दादी ने छीन लिया और मां मेरी मायके चली गई। लेकिन मां ब्रज की परिक्रमा के बहाने गांव में आती थी और अपनी पुरानी सहेलियों से कहती थी कि मेरे गोपाल को कैसे भी मुझे दिखा दो। तब वह मुझे गोद में उठाकर खिड़की से दिखा देती थीं और मां विह्वल होकर मुझे देखती और लौटकर चली जाती थी।
प्रश्न :यह दृश्य बड़ा मार्मिक है, व्यासजी ! इसको तो सुनकर भी सिहरन हो रही है कि मां अपने बालक से मिलने के लिए कैसे-कैसे भटकती हुई आती थी। मुझे लगता है, यही पीड़ा आपके लेखन में झलकती है। जब आप पत्नीवाद, सालीवाद अपनी कविता में लाते हैं और महिलाओं को प्रवंचनाओं से भरा हुआ पाते हैं। क्या ऐसा है ?
उत्तर : एक बार की बात बताता हूं, संवत् 1981 में बड़ी जबरदस्त बाढ़ आई और एक लोकगीत प्रचलित हुआ था- “संवत् इक्यासी की साल, हाल कुछ कहा न जाता है, डूब गए सारे सात बाजार, छत्ता और नया बाजार देख दिल धड़का खाता है।” तो वह बाढ़ का पानी विश्राम घाट पर हमारा जो राधा दामोदर का मंदिर है, यद्यपि वह ऊंचाई पर है, लेकिन उसमें भी भर गया और तहख़ाने में भी पानी घुस गया। कीचड़ ही कीचड़ होगई। दीवारें फट गईं। पिताजी बाहर थे। चाचाजी ने चिट्ठी लिखी नानाजी को कि गोपाल की मां को भेज दो। नानाजी इक्के में मां को बिठाकर चल दिए। वहां भी बरसात का मौसम था। एक शालिग्राम का तालाब था जिसका पानी सड़क पर भी आगया था। घोड़ा इक्के सहित उस तालाब में घुस गया और मां लहंगा पहने हुए थी। लेकिन तैरना जानती थी, उसने नानाजी को धक्का देकर नीचे उतार दिया। वह तो बच गए, परंतु मां इक्के के साथ ही डूबती हुई चली गई। तत्काल नाना दौड़ पड़े। नानाजी, जो राजा भरतपुर के बड़े प्रिय पात्र थे, उन्होंने कहा राजा तेरी दुहाई है, मेरी बेटी डूब गई है, बचाओ उसको। राजा ने हाथी भेजा तो हाथी पर बैठकर मां लौटकर आगई। लौटकर आई तो मुझे छाती से लगा लिया। हाय ! आज मैं मर गई होती तो मेरे गोपाल का क्या होता ?
प्रश्न : अभी आप बता रहे थे कि विश्राम घाट पर जो आपका मंदिर है, उसमें पानी घुस आया था, तो विश्राम घाट के मंदिर के बारे में कुछ बताइए। वहां पंडे होते होंगे। भक्त होते होंगे। आरती होती होगी। थाल सजता होगा।
 उत्तर : वह सब बंद होगया था। बाज़ार में भी पानी भर गया था। लक्ष्मीनारायणजी की ऊंची टेक पर से आरती होती थी। सब पंडे और पुजारी भाग गए थे। एक भी नहीं बचा था। बात तब की है जब दादी ने मुझे रख लिया और मां चली गई। पितृभक्त पिताजी मौन रहे, कुछ नहीं कहा। लेकिन जब मथुरा आगए और सैटल होगए तो अम्मा अपने भाई को लेकर आई। पिताजी ने कहा कि तू इतने वर्ष मुझसे अलग रही, अब तेरी पवित्रता पर मैं कैसे विश्वास करूं ? अंगीठी जल रही थी, उसमें से कोयले निकालकर कहा- “हाथ पसार, तेरे हाथ पर कोयला रखकर देखता हूं , जल जाएगी तो समझूंगा कि तू भ्रष्ट है, नहीं जलेगी तो तू सती है।” मां ने हाथ पसार दिए और वो कोयला राख होकर गिर पड़ा और जब वह सत्य साबित होगई तो पहला काम यह किया कि मां ने मुझे छाती से लगा लिया। हाय ! अगर मैं जल गई होती और कलंकिनी सिद्ध होगई होती तो अपने पाए हुए गोपाल को खो नहीं देती क्या ?
उत्तर : वह सब बंद होगया था। बाज़ार में भी पानी भर गया था। लक्ष्मीनारायणजी की ऊंची टेक पर से आरती होती थी। सब पंडे और पुजारी भाग गए थे। एक भी नहीं बचा था। बात तब की है जब दादी ने मुझे रख लिया और मां चली गई। पितृभक्त पिताजी मौन रहे, कुछ नहीं कहा। लेकिन जब मथुरा आगए और सैटल होगए तो अम्मा अपने भाई को लेकर आई। पिताजी ने कहा कि तू इतने वर्ष मुझसे अलग रही, अब तेरी पवित्रता पर मैं कैसे विश्वास करूं ? अंगीठी जल रही थी, उसमें से कोयले निकालकर कहा- “हाथ पसार, तेरे हाथ पर कोयला रखकर देखता हूं , जल जाएगी तो समझूंगा कि तू भ्रष्ट है, नहीं जलेगी तो तू सती है।” मां ने हाथ पसार दिए और वो कोयला राख होकर गिर पड़ा और जब वह सत्य साबित होगई तो पहला काम यह किया कि मां ने मुझे छाती से लगा लिया। हाय ! अगर मैं जल गई होती और कलंकिनी सिद्ध होगई होती तो अपने पाए हुए गोपाल को खो नहीं देती क्या ?
प्रश्न : तब आप कितने बड़े थे, व्यासजी !
उत्तर : उस समय मैं बारह-तेरह बरस का था।
प्रश्न : आपके मन में मातृभक्ति इतनी ज्य़ादा रही है, उस समय आप अपने आपको इस योग्य पाते थे कि पिता से अपनी मां के पक्ष में कुछ कह सकें ?
उत्तर : पिताजी के सामने बोलने का साहस मुझमें नहीं था, लेकिन मैं अनुभव करता हूं कि मैं कितना अभागा हूं कि मां का प्यार न पा सका। वह बीमार रहती थी। मैं न उसकी कोई सेवा कर सका, न देखभाल। उसने गोपाल-गोपाल कहते-कहते ही प्राण छोड़ दिए, लेकिन गोपाल ऐसा कर्महीन निकला कि रुग्ण मां की सेवा, सहायता कुछ नहीं कर सका।
प्रश्न : आज भी आप इतने भावुक हैं कि हम सब भावुक हो सकते हैं आपकी इस कहानी को सुनकर। व्यासजी ! इससे यह बात सिद्ध होती है कि जितने भी महान रचनाकार संसार में हैं उनको कहीं न कहीं पीड़ाओं के दंश एक से ज्य़ादा मिले हैं। मां के पक्ष से आपकी जो यह पीड़ा है, यह आपने सुख बांटकर, दूसरों को सुख देकर पूरी की। मैं यह नहीं समझ पा रहा हूं कि साली पर लिखी हुई कविता, घरवाली पर लिखी हुई कविता, पत्नीवाद, ये सब मां के प्रति जो आपकी प्रवंचनात्मक स्थितियां रही हैं, उससे हुआ है क्या ? हम थोड़ा सहज करें, क्योंकि रोने को मन कर रहा है आपकी बातें सुनकर। आपने जो पत्नीवाद वाली कविताएं लिखना शुरू कीं, वो किस ज़माने में शुरू कीं ?
 उत्तर : जब अंग्रेजों का राज था। उन दिनों कोई अंग्रेजों के संबंध में चूं तक नहीं कर सकता था। जो बोलता था तो उसका मकान, दुकान, व्यवसाय सब कुर्क हो जाता था। तब मैंने पत्नी को माध्यम बनाकर कविताएं लिखीं। उन दिनों राशन पर लिखा, कंट्रोल पर लिखा- “हे मजिस्ट्रेट महाराज ! हमारी पत्नी पर कंट्रोल करो। घी, तेल, सूजी, माचिस तक पर कंट्रोल हुआ। तो ये ही क्यों बचें। प्रभुजी इसका भी कुछ मोल करो।” (पत्नी को परमेश्वर मानो)। यह पत्नीवाद नहीं है। यह तो समाज-परिष्कार था अंग्रेजों के विरुद्ध देश का, असहयोग था देश छोड़ने के लिए। धीरे-धीरे इसको लोगों ने पत्नीवाद कहना शुरू कर दिया। लेकिन कुछ आलोचकों ने इसे पत्नीवाद नहीं, परिवार-रस कहा। अब जो भी कुछ हो, आपसे मेरा अनुरोध है कि मेरी एक पुस्तक आ रही है ‘व्यंग्यायन’। उसमें मैंने पत्नी के संबंध में जो वास्तविकता है, बताई है। पत्नी मेरी नहीं, उसकी है, इसकी है, ज़माने की है, जगत की है, पुरातन नहीं, नूतन है। ऐसा लिखकर अपनी कैफ़ियत दी है।
उत्तर : जब अंग्रेजों का राज था। उन दिनों कोई अंग्रेजों के संबंध में चूं तक नहीं कर सकता था। जो बोलता था तो उसका मकान, दुकान, व्यवसाय सब कुर्क हो जाता था। तब मैंने पत्नी को माध्यम बनाकर कविताएं लिखीं। उन दिनों राशन पर लिखा, कंट्रोल पर लिखा- “हे मजिस्ट्रेट महाराज ! हमारी पत्नी पर कंट्रोल करो। घी, तेल, सूजी, माचिस तक पर कंट्रोल हुआ। तो ये ही क्यों बचें। प्रभुजी इसका भी कुछ मोल करो।” (पत्नी को परमेश्वर मानो)। यह पत्नीवाद नहीं है। यह तो समाज-परिष्कार था अंग्रेजों के विरुद्ध देश का, असहयोग था देश छोड़ने के लिए। धीरे-धीरे इसको लोगों ने पत्नीवाद कहना शुरू कर दिया। लेकिन कुछ आलोचकों ने इसे पत्नीवाद नहीं, परिवार-रस कहा। अब जो भी कुछ हो, आपसे मेरा अनुरोध है कि मेरी एक पुस्तक आ रही है ‘व्यंग्यायन’। उसमें मैंने पत्नी के संबंध में जो वास्तविकता है, बताई है। पत्नी मेरी नहीं, उसकी है, इसकी है, ज़माने की है, जगत की है, पुरातन नहीं, नूतन है। ऐसा लिखकर अपनी कैफ़ियत दी है।
प्रश्न : मेरी अब बात समझ में आती है और आलोचक भी एक चीज को एक स्तर तक लेते हैं और उसकी गहराई में नहीं जा पाते हैं। आपका जो ये परिवारवाद है, यह मूलतः राष्ट्रीय मुक्ति संग्राम आंदोलन का एक बहुत बड़ा औज़ार था, जिसको परिवार के माध्यम से आपने सरकार तक पहुंचाने का एक उपक्रम किया। अभी तक बात हो रही थी आपकी मां के बारे में, उस बाढ़ के बारे में, जिसमें आप भी डूबे हुए थे, लेकिन बचे हुए थे और आपका बचना उनका काव्य था। उनका साया कब तक आपके ऊपर रहा ?
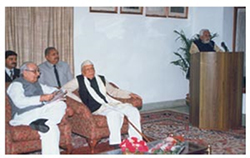 उत्तर : लगभग पंद्रह साल वह रही और उसको क्षयरोग होगया। उस समय क्षयरोग का इलाज नहीं निकला था। निकला होगा तो मथुरा तक नहीं पहुंचा था। पिताजी ने अस्पताल में भी भेजा। फिर उसको सबसे दूर करने के लिए एक अलग जगह में ही रखा गया। फिर मेरी नानी उसे अपने साथ लिवा ले गई। राधाकुंड में ही पैदा हुई और राधाकुंड में ही “राधे, राधे, गुपाल,गुपाल। मेरे गुपाल को बुलाओ, मेरे गुपाल को बुलाओ !” कहते-कहते उसने अपने प्राण त्याग दिए। मैं ऐसा अभागा रहा कि न तो मां की सेवा कर सका और न उसके कोई काम आ सका। क्योंकि तब मैं इस योग्य ही नहीं था। कोई नौकरी नहीं, कोई चाकरी नहीं। आवारा जीवन बिताता था। शतरंज खेलता था। चौपड़ खेलता था। कुश्ती लड़ता था। फिर जिन दिनों मैं चम्पा हाईस्कूल में पढ़ता था, तब सत्येन्द्र नाम के एक वरिष्ठ हिन्दी-विद्वान से भेंट हुई। वह बड़े प्रभावित थे मेरी कविताओं से, जो अक्सर अख़बार में छपती थीं। एक दिन मैं अखाड़े से लौट रहा था, हाथ में गजरा बंधा हुआ था। उन्होंने मुझे देखकर कहा कि “गुपाल, तुम इसके लिए पैदा नहीं हुए हो। तुम मेरे पास आओ। जो करना है, मैं करूंगा।” तो वह रात के नौ बजे से रात के ग्यारह-बारह बजे तक मुझे पढ़ाते थे। स्कूल की पढ़ाई तो दर्जा़ छह तक ही हुई। लेकिन उन्होंने ‘विशारद’ कराया, ‘साहित्य-रत्न’ कराया और ‘साहित्य संदेश’ में मुझे सह-संपादक बनाया। बाद में तो मैं संपादक ही बन गया।
उत्तर : लगभग पंद्रह साल वह रही और उसको क्षयरोग होगया। उस समय क्षयरोग का इलाज नहीं निकला था। निकला होगा तो मथुरा तक नहीं पहुंचा था। पिताजी ने अस्पताल में भी भेजा। फिर उसको सबसे दूर करने के लिए एक अलग जगह में ही रखा गया। फिर मेरी नानी उसे अपने साथ लिवा ले गई। राधाकुंड में ही पैदा हुई और राधाकुंड में ही “राधे, राधे, गुपाल,गुपाल। मेरे गुपाल को बुलाओ, मेरे गुपाल को बुलाओ !” कहते-कहते उसने अपने प्राण त्याग दिए। मैं ऐसा अभागा रहा कि न तो मां की सेवा कर सका और न उसके कोई काम आ सका। क्योंकि तब मैं इस योग्य ही नहीं था। कोई नौकरी नहीं, कोई चाकरी नहीं। आवारा जीवन बिताता था। शतरंज खेलता था। चौपड़ खेलता था। कुश्ती लड़ता था। फिर जिन दिनों मैं चम्पा हाईस्कूल में पढ़ता था, तब सत्येन्द्र नाम के एक वरिष्ठ हिन्दी-विद्वान से भेंट हुई। वह बड़े प्रभावित थे मेरी कविताओं से, जो अक्सर अख़बार में छपती थीं। एक दिन मैं अखाड़े से लौट रहा था, हाथ में गजरा बंधा हुआ था। उन्होंने मुझे देखकर कहा कि “गुपाल, तुम इसके लिए पैदा नहीं हुए हो। तुम मेरे पास आओ। जो करना है, मैं करूंगा।” तो वह रात के नौ बजे से रात के ग्यारह-बारह बजे तक मुझे पढ़ाते थे। स्कूल की पढ़ाई तो दर्जा़ छह तक ही हुई। लेकिन उन्होंने ‘विशारद’ कराया, ‘साहित्य-रत्न’ कराया और ‘साहित्य संदेश’ में मुझे सह-संपादक बनाया। बाद में तो मैं संपादक ही बन गया।
प्रश्न : व्यासजी, आप मुझे बताएंगे कि आपके जो पहले रोज़गार थे, बचपन की क्रीड़ाओं के बाद, मां की गोदी से निकलने के बाद, जो आपके प्रारंभिक रोज़गार थे, वे क्या थे ?
उत्तर : पहले कम्पोजीटर था, कम्पोजीटर से प्रूफरीडरी की, प्रूफरीडरी से मशीनमैनी हुई। मशीनमैनी से कागज का ज्ञान हुआ। फिर प्रेस की कला से पूरा परिचित होगया और हां, तब हमारे यहां कचहरी में म्यूज़ियम था। इसमें प्राचीन मूर्तियां आदि अनेक अदभुत वस्तुएं रखी जाती थीं। मैंने भी उसमें सहयोग किया और मेरे द्वारा दी हुई मूर्तियां, तोरण, स्तंभ आदि आज भी नए म्यूज़ियम में सुरक्षित हैं। वासुदेवशरणजी ने मुझे सिखाया कि कागज कितने प्रकार के होते हैं। जैन-कला क्या और बौद्ध-कला क्या है ? पोद्दारजी ने मुझको अलंकार, रस, रीति, लक्षणा, व्यंजना आदि बताए। जगन्नाथदास ‘रत्नाकर’ आदि का काव्य पढ़ा, जो साहित्य की परंपरा है। लेकिन उसका प्रयोग मैंने अपने साहित्य में नहीं किया। अनजाने में आगया हो तो आगया हो। मैंने अलंकार के लिए अलंकार नहीं लिखे। रस के लिए रस नहीं लिखा। रीति के लिए रीति नहीं लिखी और लिखा आज की परिस्थितियों पर, आज की विषमताओं पर, आज की कुमति पर, भ्रष्टाचार आदि पर।
प्रश्न : ये आपका वह काल था जिसमें आप सीख भी रहे थे, साहित्य का ज्ञान भी प्राप्त कर रहे थे। आप तरह-तरह के हुनर अपने अंदर विकसित कर रहे थे और आपने बताया कि आप कम्पोजीटर थे। इसकी शुरूआत कैसे हुई और इसमें कौन आपके गुरु थे। इस बारे में बताएंगे व्यासजी ?
उत्तर : हमारे मंदिर के पास एक दूसरा मंदिर है कृष्ण-बलदेव का। उसमें पुजारी थे गोपीनाथ। वह एक दिन मेरे पास आए, बोले-“गोपाल दम लगाने के लिए मुझे एक चवन्नी की ज़रूरत है।” उस समय तक मेरा विवाह हो चुका था। घर में खाना बनाने वाला कोई नहीं था, तो मेरा ब्याह कर दिया गया। ब्याह करके आवश्यक बर्तन-भांडे देकर और एक रुपया महीने के किराए वाला एक टूटी छत वाला मकान देकर मुझे अलग कर दिया गया। एक रुपया मेरे पास था। मैंने उसमें से एक चवन्नी उनको दे दी। मैंने कहा- “गोपीनाथजी, आप मुझे कम्पोजीटरी सिखा दें।” वह बोले, “मैंने बड़े-बड़े लोगों को कम्पोजीटरी सिखा दी, तू तो घर का है, कल से आ जाना।” मैं काशीनाथ प्रिटिंग प्रैस में जाने लगा। आठ पेजों के लिए चार रुपए मिलते थे। मैं टाइप-खानों को पहचानने लगा कि किसमें कौन-सा है ? ‘अ’ किसमें है, ‘क’ किसमें है। मात्रा किसमें हैं, स्वर किसमें है। तभी पास में बैठे कम्पोजीटर ने मेरे हाथ में संटी मारी। बिना मिठाई खिलाए तू ये क्या चुनने में लगा है ? पहले मिठाई खिला। अगले दिन मैंने उस एक रुपए में से आठ आने के पेड़े लाकर बंटवा दिए। आठ पेजों के चार रुपए जो मिलने थे। पहले मैंने चार पेज किए, फिर छह पेज किए, फिर आठ पेज तक करने लगा। चार रुपए मिलने लगे। परंतु गुरु तो गुरु निकले। वह उसे अपने हिसाब में डालने लगे। मुझको धेला भी नहीं मिला। तो ऐसे मेरी कम्पोजीटरी की शुरूआत हुई।
प्रश्न : मैं समझता हूं कि यही वो प्रस्थान बिंदु था जहां से आप पत्रकारिता में भी प्रविष्ट हुए और कम्पोजिंग करते-करते, अख़बारों के लिए फौंट लगाते, उन लेखों को सजाते-संवारते। आपके अंदर पत्रकार ने जन्म लिया। जब आपका पत्रकार जन्म ले रहा था, तब प्रारंभिक रचनाएं आपकी किस प्रकार की थीं ?
उत्तर : ऐसा है कि मैं आगरे में बाबू गुलाबरायजी के साथ ‘साहित्य-संदेश’ में सह-संपादन करता था। तब मुझे ब्रज की कविता भी आती थी। उनके सुझाव से गुलाबरायजी की ‘हिमाक़त’ नामक पुस्तक पढ़ता था। मैं नई-नई कविता लिखने लगा, मेरी पहली कविता का विषय था -‘ओ बाबूजी की डबल भैंस !’ ऐसी चार कविताएं मैंने लिखीं तो ‘वीणा’ के संपादक कालिकाप्रसाद एक दफ़ा ‘साहित्य-संदेश’ के दफ्तर में आए और उन चारों कविताओं को ले गए और ‘वीणा’ में उनको छाप दिया। फिर माखनलाल चतुर्वेदी के संपर्क में आया। अब मैं देशभक्ति की कविता भी लिखने लगा। उनको वह छापने लगे। बाबूजी की प्रेरणा से मैंने द्विवेदीजी की ‘रसज्ञ रंजन’ नामक पुस्तक का संपादन किया। नगेन्द्रजी के साथ पांडुलिपियों पर काम किया। इसी तरह मैं कवि-लेखक से पत्रकार बन गया। मेरी गुरु-भाषा की कविता कैसी होती थी। कहें तो उसका एक उदाहरण सुना दूं- “कांटों ने मुझे खुशबू दी है।” “आम के नीचे मयूर का नाच”…………………
प्रश्न : ‘वीणा’ में आपकी कविताएं छपीं और माखनलाल चतुर्वेदीजी भी आपकी कविताएं छापने लगे। आपने ब्रजभाषा की कविता से प्रारंभ किया अपना लेखन या खड़ी बोली की कविता से ?
उत्तर : ब्रजभाषा में कविता लिखना शुरू किया। क्योंकि वही मेरी मातृभाषा और मेरे संस्कारों में रची-बसी थी।
प्रश्न : कौन-सी कविता थी वह ?
उत्तर : पावस वाली थी। खानपान के विषय में थी। आपने यह नहीं पूछा कि आप क्या खाते थे ?
प्रश्न : तो लगे हाथ यह भी बता दीजिए !
उत्तर :
भोजन में भात होय, घी से मुलाकात होय,
दही-बूरा साथ होय, दाल अरहर की।
हरो कछु साग होय, चटनी की लाग होय,
फूले-फूले फुलका, परोसे जाए घर की। <
br/>
रबड़ी जो मिल जाए कहूं, फिर
हमें चाहना, ना विधि हरि हर की।
प्रश्न : ब्रज के आपके जो पूरे संस्मरण हैं, उनमें तो अनन्तकाल तक आप आनंदित होकर हमें बताते रह सकते हैं। मुझे लगता है कि महावीरप्रसाद द्विवेदी की जो भूमिका थी हिन्दी साहित्य में लगभग वैसी ही भूमिका आपकी भी रही है। क्योंकि महावीरप्रसाद द्विवेदी कवियों की सर्जना करते थे कि कवियों को कैसा लिखना चाहिए, कवि क्या लिखें और कैसे विषय चुनें ? कवि सम्मेलनों के माध्यम से आपने भी वही भूमिका निभाई है, क्योंकि कवियों की एक पूरी ज़मात आपने पैदा की है। आपके इर्द-गिर्द जो कवि आए उनको आपने किस प्रकार की कविताएं लिखने की प्रेरणा दी ?
उत्तर : उनको मैंने वास्तव में कविता क्या है, यह बताया और कुछ कविताएं लिखकर उनको दीं भी। पहले मंच पर कविता ही पढ़ी जाती थी, अब नहीं पढ़ी जाती। अब तो कविता के नाम पर नौटंकी होती है। कविता का भी उद्योग बन गया है। लिफाफे के लिए लिखी जाती है। जो मेरे पक्के शिष्य थे, उन्हीं लोगों ने इस कविता को भ्रष्ट कर दिया। महावीरप्रसाद द्विवेदी के बनाए हुए शिष्य तो मैथिलीशरण आदि राष्ट्रकवि होगए। मेरे शिष्य विदूषक होगए और भंडैती करने लगे। वे कविता क्या है, उसको भूल गए। ताली पिटवाना ही उनका परम धर्म रह गया। लिफाफा पाना ही उनका उद्देश्य होगया। कवि सम्मेलन अब रहे ही नहीं, धंधा होगए हैं।
प्रश्न : लेकिन व्यासजी, इसकी शुरूआत तो आपने ही की थी। पैसा दिलवाना तो आपने शुरू किया था। लाल किले के मंच पर जब कवि आते थे तो आप ही नेपथ्य में सबको लिफाफे दिलवाते थे। आप ही उनके लिए ताली बजवाते थे।
उत्तर : मैं उनको उतना ही देता था-गुज़ारे लायक। उनके आने-जाने का किराया, खाने-पीने का खर्चा दिलवाता था। आज की तरह हजारों रुपए नहीं। दो सौ, तीन सौ रुपए से ज्य़ादा मैंने किसी को नहीं दिए।
प्रश्न : आपकी पीड़ा बिलकुल सही है कि लिफाफे और तालियों के मोह में कवि सम्मेलन पतनशीलता को प्राप्त हुए। लेकिन व्यासजी, मेरा मानना ये है कि अभी भी ऐसे लोग हैं, वाचिक परंपरा का आपने जो मार्ग दिखाया, उस पर चल रहे हैं। आपको याद होगा आपने एक पैन मुझे दिया था। सन् 64 या 65 में।
उत्तर : याद है, आप जैसे लोग ही हैं जो सच्ची कविता की ध्वजा को धारण किए हुए हैं। ऐसे ही एक दो कवि और हैं, ज्य़ादा नहीं है।
प्रश्न : प्रयास रहेगा कि ये वाचिक परंपरा जैसा आप चाहते हैं, चलती रहे और श्रेष्ठतम हो ।
उत्तर : उनमें से एक गोविन्द भी है। गोविन्द प्रारंभ से ही बड़ा मेधावी रहा है। दस वर्ष की उम्र में उसने स्वरचित कविता सुनाकर मीर मुश्ताक अहमद से, जो दिल्ली के ज़बरदस्त समाजवादी कांग्रेसी नेता थे, उनसे नकद दस रुपए का पुरस्कार प्राप्त किया और फिर तो उसकी कविताएं ऐसी लोकप्रिय हुईं कि देश में ही नहीं, विदेश में भी उसने नाम कमाया। और अब तो हिन्दी भवन का मंत्री बनकर, मेरा उत्तराधिकारी बनकर, उन्नति के शिखर पर चढ़ता चला जा रहा है। मैं उससे बहुत प्रसन्न हूं।
प्रश्न : इसमें संदेह नहीं कि गोविन्द व्यास हिन्दी भवन के माध्यम से और कवि सम्मेलन के माध्यम से श्रेष्ठ कार्य कर रहे हैं। लाल किले के कवि सम्मेलन आपने पच्चीस साल लगातार कराए। पच्चीस सालों के बाद ज़िम्मा प्रशासन ने ले लिया। जिस समय तक आपके पास रहे उसमें क्या गुण थे और जब आपसे अलग होगए, तब उसमें क्या अवगुण आए, इसका अंतर बताएंगे ?
उत्तर : तब उसमें कविता पढ़ी जाती थी। सच्चे एवं श्रेष्ठ कवि आते थे। पं. जवाहरलाल नेहरू आते थे, पंतजी आते थे, मैथिलीशरण गुप्त आते थे, सोहनलाल द्विवेदी आते थे, भगवतीचरण वर्मा आते थे, उदयशंकर भट्ट आते थे। अब वह कवि सम्मेलन मेरे न रहने पर भ्रष्ट होगया। मगर परंपराएं चलती ज़रूर हैं, जैसे महामूर्ख सम्मेलन चल रहा है। लेकिन बेजान होगए हैं। अब चाटुकारिता होगई है, लिफाफे के लिए कविता लिखी जाती है। कविता के लिए कविता नहीं लिखी जाती।
प्रश्न : व्यासजी, ब्रज का लीलाधाम छोड़कर रास की परंपरा, लोकनाट्य की परंपरा के जुड़ाव के बावजू़द आपका दिल्ली आना हुआ तो ये कैसे संक्रमण हुआ ? इसकी क्या कहानी है ?
उत्तर : ऐसा हुआ कि मैंने स्वतंत्रता संग्राम में ‘करो या मरो’ आंदोलन के दौरान कलम पकड़ ली और लिखने लगा। उन्हीं दिनों हरिद्वार में ‘हिन्दी साहित्य सम्मेलन’ का वार्षिक अधिवेशन शुरू हुआ। उसमें माखनलाल चतुर्वेदी को चांदी के रुपयों से तोला गया। उस समय के सारे प्रमुख साहित्यकार आए। नगेन्द्रजी भी आए। जैनेन्द्रजी भी आए। जैनेन्द्रजी स्वयं नहीं लिखते थे। जैसे मैं बोलकर लिखवाता हूं, ऐसे ही जैनेन्द्रजी भी बोलकर लिखवाते थे। जैनेन्द्रजी का एक पत्र मुझे मिला कि व्यास, ‘साहित्य संदेश’ छूट चुका है और अब खाली हो, दिल्ली आ जाओ। इसके साथ सादा लिफाफे में दस-दस के पांच नोट थे। तो मैं दिल्ली आगया। घर पर राशन-पानी का इंतज़ाम करके रेल का टिकट कटाकर एक चवन्नी बची थी, उस चवन्नी से रिक्शा करके मैं दरियागंज पहुंचा। जैनेन्द्रजी के यहां। जैनेन्द्रजी के पास बैठकर कहानियां लिखवाने लगा। लिखते-लिखते मुझे भी कहानी लिखना आगया। मैंने भी कुछ कहानियां लिखीं। उसके बाद जैनेन्द्रजी ने कहा कि लाओ, मैं इनमें संशोधन कर देता हूं, मैंने दे दीं। बाद में मैंने देखा कि हेर-फेर करके जैनेन्द्रजी ने वे अपने नाम से छपा दीं। ऐसे ही प्रभुदयाल मीतल ने मेरी नायिका भेद, नख-शिख वर्णन की पुस्तक (जब मैं स्वतंत्रता आंदोलन में आगया था) अपने नाम से छपा लीं। मेरा ऐसा भी शोषण हुआ।
प्रश्न : यह तो साहित्य की अंतर्कथाएं हैं। ऐसी चीजें होती रहती हैं। किसी को बढ़ाते हैं उस्ताद लोग तो वे थोड़ी-सी उस्तादी दिखा ही देते हैं। लेकिन जब आप दिल्ली आए तो पहले आप किन्हीं के गणेश बने। फिर देवराजेन्द्र आपके गणेश बन गए। ये तो एक परंपरा है, सिलसिला है, जो आगे चलता रहता है। एक अंतर्कथा आप बताएं, जैनेन्द्रजी के पास आने के बाद आप ‘हिन्दुस्तान टाइम्स’ में कैसे आए ?
उत्तर : जैनेन्द्रजी के साथ ज्य़ादा दिन नहीं पटी और तय हुआ था कि दोनों लिखेंगे और आधा-आधा बांट लेंगे। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, तो मैंने छोड़ दिया। उपेन्द्रनाथ ‘अश्क’ और नगेन्द्रजी ने उनको समझाया तो वह बाल खींचने लगे, रोने लगे कि मैं पापी हूं, मुझसे ग़लती हुई है। व्यास को समझाओ। उन्होंने मुझे समझाया, लेकिन मैं तो छोड़ने का निश्चय कर चुका था। छोड़कर चल दिया और फ्रीलांस करने लगा। नई सड़क पर किताबों की कुंजियां लिखने लगा। रस, अलंकार, छंद पर चार्ट लिखने लगा। ‘साहित्य प्रभाकर’ आदि में लगने वाली पुस्तकों की मीमांसा करने लगा और विद्यार्थियों को पढ़ाने लगा। रेडियो में जाने लगा, ‘हिन्दुस्तान’ में मेरी कविताएं छपने लगीं। तो एक दिन देवदासजी का एक मनीआर्डर मुझे मिला। कर्मचारियों को तो बोनस मिलता है, लेकिन लेखन के रूप में मुझको 200/- रुपये का उन्होंने बोनस भेजा। मैं गदगद होगया कि लेखक को भी बोनस मिलता है। सस्ता साहित्य मंडल के मंत्री मार्तण्ड उपाध्याय का नाम आपने सुना होगा। उनके कहने से एक रोज़ देवदासजी ने मुझे चाय पर बुला लिया और कहा कि हम ज्य़ादा तो आपको दे नहीं सकते, 80 रुपये देंगे, आप ‘हिन्दुस्तान’ में काम करो। हम वार्षिक वृद्धि भी करते हैं और बोनस भी देते हैं। धीरे-धीरे बढ़ जाएगा। मैंने जैनेन्द्रजी से परामर्श किया तो उन्होंने कहा कि इस बड़ी प्रैस की चक्की में पिस जाओगे। परंतु बाक़ी मित्रों ने कहा कि अवश्य जाओ। 80 रुपये पर मैं ‘हिन्दुस्तान’ में काम करने लगा। दिन और रात में डयूटी करने लगा। देवदासजी को मालूम हुआ तो उन्होंने कहा कि नहीं व्यास को दिन और रात की ड्यूटी के लिए नहीं, साहित्य संपादक बना करके मैग्ज़ीन सैक्शन में भेज दो। फिर जब पद्मश्री मिली तो मुझे सह-संपादक बना दिया गया। वहां पर मैंने ‘यत्र-तत्र-सर्वत्र’ लिखा, ‘नारदजी खबर लाए हैं’ लिखा, राजस्थान पत्रिका में ‘बात-बात में बात’ लिखा और आगरे के दैनिक पत्र ‘विकासशील भारत’ में ‘चकाचक’ लिखा। ऐसे स्तंभों में मैं समाज की विकृतियों, विषमताओं एवं आज की परिस्थितियों को लिखता चला आया हूं।
प्रश्न : बहुत बड़ी बात है कि आप आज तक लिखते चले आ रहे हैं ।
उत्तर : नारदजी को पचास वर्ष से ऊपर होगए, अगर कोई मुझे भी रवीन्द्रनाथ जैसा प्रमोटर आज मिल जाए तो मैं भी, मेरा नाम भी सर्वोच्च पुरस्कार के लिए आ सकता है, लेकिन ऐसा कोई नहीं मिला।
प्रश्न : व्यासजी, आप निराश न हों, आगे आने वाली पीढ़ी मूल्यांकन करना जानती है। लेकिन मैं एक बात जानता हूं कि व्यासजी, आप ऐसे दुलर्भ व्यक्तित्व हैं जो दोनों क्षेत्रों में समान महत्व रखते हैं। लेखन में भी और वाचिक परंपरा में भी। आपने कवि सम्मेलन के माध्यम से वाचिक परंपरा को आगे बढ़ाया और लेखन के माध्यम से पत्रकारिता में भी अपना एक स्थान बनाया। इसके अलावा आप जीवन में बड़े प्रयोगवादी भी रहे। आपने एक सिलसिला शुरू किया जो शायद ब्रज से आप लेकर आए होंगे, महामूर्ख सम्मेलन। ये सिलसिला कैसे शुरू हुआ ?
उत्तर : मैं घूमता-घामता स्वतंत्रता-आंदोलन में इटावा पहुंच गया। इटावा में श्रीनारायणजी चतुर्वेदी के पिताजी द्वारिकानाथ चतुर्वेदी के साथ मिलकर मैंने ब्रजभाषा कोश का संपादन किया। होली पर इटावा में ‘नंग-नाच’ हुआ करता था। इधर द्वारिकानाथ चतुर्वेदीजी ने मुझसे कहा कि तुम वहां मत जाना। बड़ा अश्लील दृश्य होता है। तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। उधर बनारसीदास चतुर्वेदीजी का पत्र आया कि तुम इटावा आए हो तो ‘नंग-नाच’ अवश्य देखना और उसकी रिपोर्ट मुझे भेजना। तो मैंने नंग-नाच देखा। दिन में भी देखा और रात में भी देखा। तीन दिन देखा और उसकी रिपोर्ट बनारसीदास चतुर्वेदी के पास भेज दी। बनारसीदासजी मुझको धमकाया करते थे कि यदि तुमने कोई शरारत की या मुझसे ज्य़ादा छेड़छाड़ की तो मैं तुम्हारी रिपोर्ट छाप दूंगा। मैंने उत्तर में कहा कि ध्यान रहे मैं भी तुम्हारी ओरछा नरेश के दरबार में वेश्याओं को देखने के बाद लिखा गया लेख छाप दूंगा। याद है न तुमने लिखा था-‘रूप ब्रह्मचर्य भंग भयौ……।’ तो हंसी-मज़ाक में वह खेल ख़त्म होगया। मैंने इटावा में देखा कि ‘नंगनाच’ में बड़े-बड़े लोगों के जो काले-कारनामे थे, उनको हंसी-हंसी में दर्ज़ किया करते थे। मैंने दिल्ली में भी आकर उसकी परंपरा डाली। दिनभर के रंग के बाद शाम को मैंने बड़े-बड़े नेताओं को, बड़े-बड़े दिल्ली के साहित्यमना और बुद्धिजीवियों को मूर्ख बनाया और उनका जुलूस निकाला। उसमें हाथी-घोड़े, हिजड़े सब निकलते थे। जगजीवनराम का एक प्रसंग बताता हूं कि उनके सामने जुलूस के लोग कहते थे- मूर्ख हो तो कैसा हो ? तो जगजीवनराम अपने सीने पर हाथ रखकर कहते थे कि ऐसा हो। हमारी महामूर्खा एवं चतुर नेत्री तारकेश्वरी सिन्हा पर जब लोग फूल फेंकते थे तो वह कहती थी कि तुम बड़े अनजान मूर्ख आदमी हो, यह नहीं जानते कि फूल कहां फेंकते हैं। यहां फेंको यानी कुचों पर मारो। महामूर्ख सम्मेलन में मैं नेताओं की और बड़े-बड़े बुद्धिजीवियों और समाजसेवियों की पोल खोलता रहा और रिपोर्ट पढ़ता रहा। वह रिपोर्टें छपने लगीं। बिकने लगीं।
प्रश्न : महामूर्ख सम्मेलन का एक बहुत बड़ा योगदान और रहा कि आपने मज़ाक-मज़ाक में व्यंग्य-विनोद में हिन्दी का प्रचार और प्रसार कराया। नेताओं को बुलाया, नेताओं के माध्यम से हिन्दी को बढ़ाया। तब अगला सिलसिला यह बताएं कि नेताओं की सहायता से हिन्दी की विकास यात्रा में आपने क्या रणनीति अपनाई और किस तरह से हिन्दी को लाने के लिए राजनेताओं का भी संरक्षण प्राप्त किया ?
उत्तर : मैंने केन्द्रीय मंत्री राजबहादुरजी के संपर्क में आकर ब्रज में आकाशवाणी केन्द्र की स्थापना कराई और ‘ब्रजमाधुरी’ कार्यक्रम चला दिया। शास्त्रीजी से सहयोग पाकर मैंने टंडनजी का अभिनंदन ग्रंथ प्रकाशित किया और उसको प्रथम राष्ट्रपति राजेन्द्र बाबू के द्वारा टंडनजी को भेंट कराया। उस वक्त मेरी प्रतिष्ठा में चार चांद लग गए।
प्रश्न : आज चार से ज्य़ादा चांद लग चुके हैं इस हिन्दी के भवन में। सिर्फ हिन्दी भवन में ही नहीं, हिन्दी के पूरे पर्यावरण में आपकी सुवास चारों तरफ फैली हुई है, जिसको हम कहेंगे ‘व्यास की सुवास’ तो उस सुवास में आपने हास्य-व्यंग्य को अपना हथियार बनाया और एक बहुत बड़ी शिष्य-परंपरा आपने विकसित की। ये बात दूसरी है कि आज आपको लगता है कि चेले और ज्य़ादा अच्छा काम करें। वे निश्चित रूप से करेंगे। आप मुझे यह बताइए कि क्या आपका मन भंग चढ़ाने और रबड़ी खाने का होता है ?
उत्तर : नहीं, अब तो सब छोड़ दिया। अब तो एक ही कामना रह गई है। पहले तो यह कामना थी कि मैं दर्ज़ा सात तक ही पढ़ा, आगे पढूं, लेकिन वह कामना पूरी नहीं हुई। बनारसीदासजी ने मुझसे कहा- “तुम किसी ऐंग्लो इंडियन लड़की से प्रेम करो तो तुम्हें अंग्रेजी आ जाएगी।” न कोई लड़की मिली और न अंग्रेजी सीखी। लेकिन सुन-सुनकर, पढ़-पढ़कर मैं इतनी अंग्रेजी जान गया कि पी.टी.आई. की, यू.एन.आई.की खबरों का अनुवाद हिन्दी में करने लगा। अब तो एक ही कामना शेष है कि विषमताओं पर, भ्रष्टाचार पर, आतंकवाद पर एक बड़ा ‘व्यंग्य-ग्रंथ’ लिखूं, जिससे आज के युग की पहचान भविष्य में आने वाले लोगों को हो सके।
प्रश्न : आपने एक बात कही कि अगर एक ऐंग्लो इंडियन लड़की मिली होती तो आप अंग्रेजी जल्दी सीख जाते और आपने अंग्रेजी सीखी जीवनानुभव से। ऐंग्लो इंडियन तो नहीं मिली, पर यह बताइए कि इंडियन महिलाएं कितनी मिलीं आपको, जिन्होंने आपके जीवन को रसमय किया ?
उत्तर : इंडियन महिलाओं का तो हाल यह था कि मैं दिल्ली में महिलाओं के लिए हीरो था। लाल किले के कवि सम्मेलन से जब मैं उठकर चलने लगता तो मेरे पीछे महिलाओं की भीड़ चलने लगती थी। और मुझको जब कांग्रेस और जनसंघ ने लोकसभा का टिकट देना चाहा तो मेरी विशेषताओं में एक विशेषता यह भी मानी गई थी कि महिलाओं के मत तो व्यास को सबसे अधिक मिलेंगे।
प्रश्न : आपका निजी स्नेह किन-किन पर रहा, जो आपकी बहुत निकट की महिला मित्र रहीं ? उनमें से शायद एक-आध आदरणीय ऊपर पहुंच गईं हों, या रहीं हों अभी ? अंतरंग बात । गोपनीयम् गोपनीयम्।
उत्तर : महिलाएं जीवन में बहुत आईं, परंतु वे अपने-अपने स्वार्थ के लिए आईं। कोई नौकरी के लिए आई, कोई डॉक्टरेट प्राप्त करने के लिए आई। वे सब अपना स्वार्थ सिद्ध करके चली गईं, किसी ने वास्तविक और सच्चा प्रेम मुझसे नहीं किया। मेरे प्रेम की प्यास तो……….
प्रश्न : जो वास्तविक और सच्चा प्रेम करने वाला होता है, उस पर आपने एक कविता लिखी थी। आशिकों की शक्ल कैसी होनी चाहिए ? क्या थी वो कविता याद है, आपको ?
उत्तर : हां याद है, सुनिए-
आशिकों की शक्ल कुछ-कुछ भूत होनी चाहिए
अक्ल उनकी नाप में छह सूत होनी चाहिए।
इश्क करने के लिए काफी कलेजा ही नहीं,
आशिकों की चांद भी मज़बूत होनी चाहिए।
प्रश्न : यह सत्य तो हर युग का सत्य है कि ‘आशिकों की चांद मज़बूत होनी चाहिए’ आपको सपने में भी कभी महिलाएं सताती हैं क्या ?
उत्तर : नहीं, मुझे सपने आते हैं तो प्रभु के आते हैं। सदाचार के आते हैं। कविता सपने में आती है और भारतेन्दु बाबू को कविता जब सपने में आती थी तो कोयले से दीवारों पर लिख दिया करते थे और सवेरे उसको उतार लिया करते थे। लेकिन मुझे तो यह सुविधा प्राप्त नहीं है। रात को आई हुई कविता सवेरे भूल जाता हूं। लेकिन आज भी सपने मुझे साहित्य के आते हैं। कविता के आते हैं।