 मेरी आत्मकथा ‘सत्य के प्रयोग’ नहीं है। न असत्य को गल्प रूप देने वाली कोई सत्यकथा। ‘विश्व-इतिहास की झलक’ भला मैं कैसे लिख सकता हूं ? ‘मेरी कहानी’ नेहरूजी की जुबानी भी नहीं है। न यह राम-कहानी है, न कृष्ण-कथा। आधुनिक साहित्य के नाम पर रोमांटिक काम-कथा भी नहीं है। यह तो एक कामगार की कहानी है। एक मसिजीवी लेखक के जीवन का लेखाजोखा है।
मेरी आत्मकथा ‘सत्य के प्रयोग’ नहीं है। न असत्य को गल्प रूप देने वाली कोई सत्यकथा। ‘विश्व-इतिहास की झलक’ भला मैं कैसे लिख सकता हूं ? ‘मेरी कहानी’ नेहरूजी की जुबानी भी नहीं है। न यह राम-कहानी है, न कृष्ण-कथा। आधुनिक साहित्य के नाम पर रोमांटिक काम-कथा भी नहीं है। यह तो एक कामगार की कहानी है। एक मसिजीवी लेखक के जीवन का लेखाजोखा है।
यह कहानी उस व्यक्ति की है जिसने बीस वर्ष की अवस्था तक बनियान का मुंह नहीं देखा था। जब उसके पिता ने गौना करके अलग किया तो उसके पास केवल एक रुपये की पूंजी थी। जो एक रुपये माहवार के टूटी छत वाले कमरे में जाकर बसा था। यहीं उसकी मधुयामिनियां मनीं।
 यह उस व्यक्ति की कहानी है जिसने चवन्नी से अपना रोज़गार शुरू किया था। संयोग देखिए कि जब दिल्ली को चला तो टिकट के पैसे चुकाने के बाद एक चवन्नी ही बची थी। उस व्यक्ति जैसे न जाने कितने लोग होंगे जो एक रुपए पर प्रतिदिन चार आने का ब्याज देते थे। मैं तो एक मुनीमजी से पर्चा लिखकर दस रुपये लेता और महीने-भर बाद पंद्रह लौटाता। लेना आसान था, पर देना बड़ा कठिन था। इस देनदारी में पत्नी के टूम-छल्ले तक चुक गए। खाना एक बार बनता था। बचा तो शाम को खा लिया, नहीं तो -हरिओम तत्सत् ! मैं तो एक जोड़ा धोती-कुर्ते से काम चला लेता था, परंतु अठहत्थी धोती में पत्नी के लिए अपने अंगों को छिपाना मुश्किल हो जाता। पीहर से प्राप्त बिछुओं की डंडियां टूट-टूट जातीं और उन्हें वे डोरों से बांध-बांधकर पहना करती थीं। पहली नौकरी आठ रुपये महीने की मिली।
यह उस व्यक्ति की कहानी है जिसने चवन्नी से अपना रोज़गार शुरू किया था। संयोग देखिए कि जब दिल्ली को चला तो टिकट के पैसे चुकाने के बाद एक चवन्नी ही बची थी। उस व्यक्ति जैसे न जाने कितने लोग होंगे जो एक रुपए पर प्रतिदिन चार आने का ब्याज देते थे। मैं तो एक मुनीमजी से पर्चा लिखकर दस रुपये लेता और महीने-भर बाद पंद्रह लौटाता। लेना आसान था, पर देना बड़ा कठिन था। इस देनदारी में पत्नी के टूम-छल्ले तक चुक गए। खाना एक बार बनता था। बचा तो शाम को खा लिया, नहीं तो -हरिओम तत्सत् ! मैं तो एक जोड़ा धोती-कुर्ते से काम चला लेता था, परंतु अठहत्थी धोती में पत्नी के लिए अपने अंगों को छिपाना मुश्किल हो जाता। पीहर से प्राप्त बिछुओं की डंडियां टूट-टूट जातीं और उन्हें वे डोरों से बांध-बांधकर पहना करती थीं। पहली नौकरी आठ रुपये महीने की मिली।
सट्टे-पानी के लिए बीस की आवश्यकता थी, तो चार-आठ आने पानी के और अंकों के सट्टों पर लगाता। कभी बढ़कर मिल जाते, कभी डूब जाते।
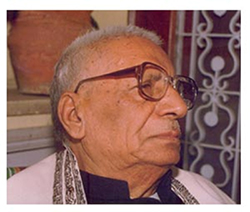 लेकिन क्या मज़ाल कि मेरे या मेरे घर की हालत की भनक किसी को पड़ जाए। बाजार में अंगोछा पहनकर ताश खेलता। कहीं चौपड़ के फड़ जमते तो कहीं शतरंज की बिसात। सती बुर्ज पर रोज छनती। यमुना पार बगीची जाता। सूखे दंड पेलता। जिन-जिन दुकानों पर, मकानों पर, मंदिरों और मठों पर, घाटों के ठाठों पर और पेड़ों के सहारे कवियों की ज़मात जुड़ती तो ऐसी ज़ोर-ज़ोर से कविताएं पढ़ता जो फर्लांगों तक सुनी जा सकती थीं।
मेरे चाहने वालों की शुरू से ही कमी नहीं रही। इत्रवाला मुफ्त में फोया देता। मालिन कलाई में खुशबूदार फूलों का कड़ा पहना देती। हलवाई कहते-गुपालजी, आज चमचम बढ़िया बनी है। चखकर देखो। मैं कहता कि पिताजी बाजार में खाता देखेंगे तो बरस पड़ेगे। दो टुकड़े एक दोने में रख दो। एक मेरा और एक मेरी पत्नी का। मटके में भरा हुआ कुएं का जल। चमचम खाई और जल पिया-हो गई ब्यालू।
लेकिन क्या मज़ाल कि मेरे या मेरे घर की हालत की भनक किसी को पड़ जाए। बाजार में अंगोछा पहनकर ताश खेलता। कहीं चौपड़ के फड़ जमते तो कहीं शतरंज की बिसात। सती बुर्ज पर रोज छनती। यमुना पार बगीची जाता। सूखे दंड पेलता। जिन-जिन दुकानों पर, मकानों पर, मंदिरों और मठों पर, घाटों के ठाठों पर और पेड़ों के सहारे कवियों की ज़मात जुड़ती तो ऐसी ज़ोर-ज़ोर से कविताएं पढ़ता जो फर्लांगों तक सुनी जा सकती थीं।
मेरे चाहने वालों की शुरू से ही कमी नहीं रही। इत्रवाला मुफ्त में फोया देता। मालिन कलाई में खुशबूदार फूलों का कड़ा पहना देती। हलवाई कहते-गुपालजी, आज चमचम बढ़िया बनी है। चखकर देखो। मैं कहता कि पिताजी बाजार में खाता देखेंगे तो बरस पड़ेगे। दो टुकड़े एक दोने में रख दो। एक मेरा और एक मेरी पत्नी का। मटके में भरा हुआ कुएं का जल। चमचम खाई और जल पिया-हो गई ब्यालू।
यह कहानी उस व्यक्ति की है जो स्टूल पर बैठकर आठ घंटे कंपोज करता। बगल से बहने वाली नाली की संड़ाध नाक से सीधे दिमाग तक पहुंचती। साथियों की परस्पर गाली-गलौज और अश्लील रसियों और लोकगीतों के टुकड़े सुनता। प्रतीक्षा करता रहता कि वेतन किस दिन मिलेगा और कितना मिलेगा। नेहरूजी अक्सर कहा करते थे- ”इस तरह तय की हैं हमने मंजिलें, गिर पड़े, गिरकर उठे, उठकर चले।”
होंगे नेहरूजी बड़े बाप के बेटे, मैं भी किसी से कम नहीं था। घर में ओढ़ने-पहनने के कपड़े न के बराबर थे। लेकिन कंधे पर खादी के थान लटकाकर उन्हें बेचकर शाम को पैसे जमा कराया करता था। ”घर में भूंजी भांग नहीं, कठौती में चून नहीं, पैसा-धेला पास नहीं, गोझा हिलावै।” लेकिन कांग्रेस का मेंबर बनाने के लिए चवन्नियां इकट्ठा किया करता था।
मेरी कमाई का महीना वर्ष में एक बार आता था, तब जब रामलीला हुआ करती थी। तब छह आने या आठ आने रोज़ मुझे सीता-लक्ष्मण और राम बनने पर मिला करते थे। पहले तालीम में और बाद में लीला में जमकर खिलाई-पिलाई होती थी। एक महीने पहले से दूध बंध जाया करता था। आज इसके यहां तो कल उसके यहां स्वरूपों की पधरावनी होती थी। चकाचक भोजन और ऊपर से ताम्बूल तथा दक्षिणा भी। भरत-मिलाप और राजगद्दी के दिन जो आरती की थाली में पड़ जाए वह स्वामी का और जो स्वरूपों के हाथ में आ जाए वह उनका, इस प्रकार पच्चीस-पचास मिल जाया करते थे। साथ में बड़े-बड़े श्रीमंतों और साधु-संतों द्वारा चरणस्पर्श और जय-जयकार अलग से। कविता शुरू की थी ब्रजभाषा से। नुमायश के कवि-सम्मेलन में तो एक रुपया मिल गया, बाकी ठन-ठन पाल मदन गोपाल। आगरा में मुंशी प्रेमचंद के सान्निध्य में बच्चन के साथ कविता पढ़ी, मिला सिर्फ किराया। इंदौर से प्रकाशित होने वाली ‘वीणा’ ने मेरी पहली चार व्यंग्य-विनोद की कविताएं लगातार छापीं, कैसा पारिश्रमिक ! छप गईं यही क्या कम था ? कविता पर पहला पुरस्कार मिला पांच रुपए का दैनिक ‘हिन्दुस्तान’ से। जब प्रति सप्ताह छपने लगीं तो मेहनताना होगया तीस रुपए माहवार। कविता से मन तो भर सकता है, पेट नहीं भर सकता। पहला लेख छपा प्रयाग के ‘देशदूत’ साप्ताहिक में। मनीआर्डर आया सात रुपये का। दूसरा छपा साप्ताहिक ‘वीर अर्जुन’ में। मिले दस रुपये। तीसरा छपा दिल्ली के ‘नवयुग’ साप्ताहिक में। पांच रुपये की वृद्धि होगई, यानि कुल पंद्रह रुपये मिले। यह था उस समय के साहित्य-लेखन का हाल।
तब कुंजियां लिखीं। ट्यूशन किए। पहली पुस्तक निकली ‘उनका पाकिस्तान’, लेकिन रायल्टी के नाम पर एक मीठी मुस्कान। हूं न कामगार और श्रमजीवी ! ऐसा कामगार जिसे कभी भरपेट सदाम काम नहीं मिला। ऐसा श्रमजीवी कि जिसने श्रम तो किया, लेकिन उससे जीविका नहीं चली।
ऐसे असाधारण व्यक्ति की कहानी को लिखकर मैं साधारण बनना चाह रहा हूं। इससे बढ़कर और ग़लतफ़हमी क्या हो सकती है ? ग़लतफ़हमी माने भ्रम। मेरी यह पुस्तक भी लोगों को भरमाने वाली है कि वैसा आदमी ऐसा हो सकता है ? अच्छा है, भ्रम बना रहे। कविता की दो पंक्तियां – “नाम ही भ्रम का है, यह विस्फोट अहम् का है।” और अहम् के बिना क्या व्यक्तित्व और क्या कृतित्व ? आत्मकथा तो बिना अहंता के लिखी ही नहीं जा सकती। इसीलिए संत-समीक्षक कह गए हैं कि आत्मकथा लिखना बहुत कठिन है। क्योंकि इसके लेखन में अहंकार से नहीं बचा जा सकता। मैं भी नहीं बचा। क्योंकि जब ढेर सारे अहंकार मेरे पास ज़मा हैं तो जाते-जाते मैं उन्हें आप पर क्यों न लुटा दूं ?
(‘कहो व्यास, कैसी कटी ?’, सन् 1994)