 हिन्दी केवल मातृभाषा नहीं, भारत की राष्ट्रवाणी है- वह वाणी जो राष्ट्र की आत्माभिव्यक्ति है, उसके विचारों-संस्कारों की प्रवाहिका है। वह प्रेम और सेवा की प्रतीक है। उसे शासकों ने नहीं गढ़ा, न सत्ता ने फैलाया। वह झोंपड़ी से गांव में, गांव से कस्बे में, कस्बे से नगर अर्थात् जन-पथ से होकर राज-पथ की ओर अग्रसर हुई है। इसने अपना पथ सत्ता या श्रीमंतों की पालकी पर बैठकर तय नहीं किया। यह संतों के साथ-साथ भारत के सुदूर तीर्थों की लंबी-लंबी यात्राओं पर गई है। कवियों, समाज-सुधारकों, राष्ट्रनेताओं की वाणी बनकर हिन्दी ने जन-जागरण, स्वातंत्र्य समता और लोकतंत्र का अलख जगाया है। हिन्दी का बीज गमलों में नहीं सींचा गया। इसकी देख-रेख और बढ़ोतरी किसी नर्सरी में नहीं हुई। अश्वत्थ वृक्ष की तरह हिन्दी का बीज सदैव विषम परिस्थितियों में भी सहजभाव से फूटा है। बाहर की बड़ी-बड़ी शिलाओं ने सोचा कि वह हिन्दी के बीज को नहीं पनपने देंगी, लेकिन हिन्दी के अंकुर सदैव चट्टानों की दरारों के बीच से अंकुरित हुए हैं। हिन्दी के वट-वृक्ष ने अपनी छाया से पत्थरों को भी शीतल किया है। हिन्दी क्लेशकर नहीं, तापहर है। यह पत्थर मारने वालों को भी फल देने वाली है।
हिन्दी केवल मातृभाषा नहीं, भारत की राष्ट्रवाणी है- वह वाणी जो राष्ट्र की आत्माभिव्यक्ति है, उसके विचारों-संस्कारों की प्रवाहिका है। वह प्रेम और सेवा की प्रतीक है। उसे शासकों ने नहीं गढ़ा, न सत्ता ने फैलाया। वह झोंपड़ी से गांव में, गांव से कस्बे में, कस्बे से नगर अर्थात् जन-पथ से होकर राज-पथ की ओर अग्रसर हुई है। इसने अपना पथ सत्ता या श्रीमंतों की पालकी पर बैठकर तय नहीं किया। यह संतों के साथ-साथ भारत के सुदूर तीर्थों की लंबी-लंबी यात्राओं पर गई है। कवियों, समाज-सुधारकों, राष्ट्रनेताओं की वाणी बनकर हिन्दी ने जन-जागरण, स्वातंत्र्य समता और लोकतंत्र का अलख जगाया है। हिन्दी का बीज गमलों में नहीं सींचा गया। इसकी देख-रेख और बढ़ोतरी किसी नर्सरी में नहीं हुई। अश्वत्थ वृक्ष की तरह हिन्दी का बीज सदैव विषम परिस्थितियों में भी सहजभाव से फूटा है। बाहर की बड़ी-बड़ी शिलाओं ने सोचा कि वह हिन्दी के बीज को नहीं पनपने देंगी, लेकिन हिन्दी के अंकुर सदैव चट्टानों की दरारों के बीच से अंकुरित हुए हैं। हिन्दी के वट-वृक्ष ने अपनी छाया से पत्थरों को भी शीतल किया है। हिन्दी क्लेशकर नहीं, तापहर है। यह पत्थर मारने वालों को भी फल देने वाली है।
 हिन्दी एक ओर गुरु नानकदेव की भाषा है तो दूसरी ओर अमीर खुसरो, जायसी, खानखाना रहीम, रसखान और इंशाअल्लाखां की भी भाषा है। इसलिए हिन्दी का संबंध केवल हिन्दुओं से जोड़ना या उसे हिन्दी-प्रदेशों की भाषा कहना उसके साथ अन्याय करना है। राष्ट्रीय परिवेश में देखें तो सिंध की सिंधी, पंजाब की पंजाबी, कश्मीर की कश्मीरी, असम की असमिया, बंगाल की बंगला, उड़ीसा की उड़िया, भारत के मलय प्रदेश की मलयालम, तेलंगाना की तेलुगू, तमिलनाडु की तमिल, महाराष्ट्र की मराठी और गुजरात की गुजराती भाषाएं पहले भी प्रचलित थीं और आज भी प्रचलित हैं। हिन्दी-प्रदेशों में तब भी और आज भी हरियाणवी, राजस्थानी, ब्रज, अवधी, भोजपुरी, मैथिली आदि भाषाएं और बोलियां पहले भी चलती थीं और आज भी प्रचलित हैं। हिन्दी-प्रदेशों के शासकों, नेताओं और भाषाविदों ने अपने तथाकथित साम्राज्य का विस्तार करने के लिए या अपनी ज्ञात अथवा अज्ञात किन्हीं महत्त्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए हिन्दी को मढ़ा हो, ऐसा कहीं देखने या सुनने में नहीं आया।
हिन्दी एक ओर गुरु नानकदेव की भाषा है तो दूसरी ओर अमीर खुसरो, जायसी, खानखाना रहीम, रसखान और इंशाअल्लाखां की भी भाषा है। इसलिए हिन्दी का संबंध केवल हिन्दुओं से जोड़ना या उसे हिन्दी-प्रदेशों की भाषा कहना उसके साथ अन्याय करना है। राष्ट्रीय परिवेश में देखें तो सिंध की सिंधी, पंजाब की पंजाबी, कश्मीर की कश्मीरी, असम की असमिया, बंगाल की बंगला, उड़ीसा की उड़िया, भारत के मलय प्रदेश की मलयालम, तेलंगाना की तेलुगू, तमिलनाडु की तमिल, महाराष्ट्र की मराठी और गुजरात की गुजराती भाषाएं पहले भी प्रचलित थीं और आज भी प्रचलित हैं। हिन्दी-प्रदेशों में तब भी और आज भी हरियाणवी, राजस्थानी, ब्रज, अवधी, भोजपुरी, मैथिली आदि भाषाएं और बोलियां पहले भी चलती थीं और आज भी प्रचलित हैं। हिन्दी-प्रदेशों के शासकों, नेताओं और भाषाविदों ने अपने तथाकथित साम्राज्य का विस्तार करने के लिए या अपनी ज्ञात अथवा अज्ञात किन्हीं महत्त्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए हिन्दी को मढ़ा हो, ऐसा कहीं देखने या सुनने में नहीं आया।
 हिन्दी-प्रदेशों ने तो उसके विपरीत एक राष्ट्रभाषा के निर्माण के लिए अपनी समर्थ भाषाओं की एक प्रकार से बलि ही दी है, नहीं तो विभूतिमयी ब्रजभाषा, जायसी और तुलसी की वाणी अवधी, चंदबरदाई से लेकर मीराबाई की राजस्थानी, महाकवि विद्यापति की मैथिली और लोक तथा साहित्य दोनों में समृद्ध भोजपुरी की क्षमता देश की अनेक प्रादेशिक भाषाओं से कम महत्त्व की नहीं थी। हिन्दी-प्रदेशों के बहुभाषा-भाषियों ने तो राष्ट्रभाषा के निर्माण के लिए आत्मत्याग का एक दुर्लभ उदाहरण देश के सामने प्रस्तुत किया है, जिसे आज की स्वार्थपरक राजनीति दुर्भाग्य से गलत चश्मे से देख रही है।
हिन्दी-प्रदेशों ने तो उसके विपरीत एक राष्ट्रभाषा के निर्माण के लिए अपनी समर्थ भाषाओं की एक प्रकार से बलि ही दी है, नहीं तो विभूतिमयी ब्रजभाषा, जायसी और तुलसी की वाणी अवधी, चंदबरदाई से लेकर मीराबाई की राजस्थानी, महाकवि विद्यापति की मैथिली और लोक तथा साहित्य दोनों में समृद्ध भोजपुरी की क्षमता देश की अनेक प्रादेशिक भाषाओं से कम महत्त्व की नहीं थी। हिन्दी-प्रदेशों के बहुभाषा-भाषियों ने तो राष्ट्रभाषा के निर्माण के लिए आत्मत्याग का एक दुर्लभ उदाहरण देश के सामने प्रस्तुत किया है, जिसे आज की स्वार्थपरक राजनीति दुर्भाग्य से गलत चश्मे से देख रही है।
 एक समय था जब उर्दू हिन्दी से अलग नहीं समझी जाती थी। पंजाबी की तरह वह भी हिन्दी की एक शैली थी। यह मान्यता आज के हिन्दी-प्रचारकों की नहीं है, इसके पीछे लगभग चार सौ वर्षों की पुरानी परंपरा है और अब से पांच-छः दशक पहले तक इस शैली-सिद्धांत को मान्यता भी प्राप्त थी। हिन्दी का नामकरण हिन्दीतर बंधुओं ने किया। इसके प्रचार का कार्य भी हिन्दीतर महामनाओं के द्वारा आगे बढ़ाया गया। यह आज की बात नहीं, स्वराज्य से भी दशाब्दियों पूर्व की बात है, जब पूर्वी भारत में ब्रह्मसमाज, दक्षिणी भारत में वैदिक समाज, पश्चिमी भारत में प्रार्थनासमाज और उत्तर पश्चिमी भारत में स्वामी दयानन्द का आर्यसमाज, हिन्दी को राष्ट्रभाषा मानकर, चारों दिशाओं से हिन्दी के लिए अनथक कार्य कर रहे थे। हिन्दी को क्षेत्रिय सीमाओं में संकुचित करनेवालों को इस तथ्य की अनदेखी नहीं करनी चाहिए कि हिन्दी के अंकुर दिल्ली, जयपुर, लखनऊ, पटना और भोपाल के बजाय स्वातंत्र्य-युद्ध का पहला शंख फूंकने वाले बंगप्रदेश में अंकुरित हुए थे। बीसवीं शताब्दी में स्वराज्य के बाद अंग्रेजी की हिमायत करनवालों की सेवा में हमारा निवेदन है कि सन् 1826 में ‘उदन्त मार्तण्ड’, सन् 1829 में ‘बंगदूत’, सन् 1850 में ‘सुधाकर’ तथा सन् 1854 में ‘समाचार सुधा-वर्षण’ नामक हिन्दी की पत्र-पत्रिकाएं सबसे पहले बंगभूमि से ही प्रकाशित हुई थीं। जब देश में राष्ट्रीय आंदोलन पूरे वेग पर था तो स्वयं स्वर्गीय चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य ने तमिलनाडु के गांव-गांव में घूमकर हिन्दी का प्रचार किया था। अगर हिन्दी साम्राज्यवादिनी होती तो अंग्रेजी साम्राज्यवाद को उखाड़ फेंकनेवाले लोकमान्य तिलक, लाला लाजपतराय, विपिनचंद्र पाल और महात्मा गांधी इसके समर्थन में असाधारण रूप से आगे बढ़ते ? स्वामी दयानंद की भाषा तो गुजराती थी, वह क्यों अपना ‘सत्यार्थ प्रकाश’ हिन्दी में लिखते ? क्यों उनका आर्यसमाज हिन्दी-प्रचार को अपना प्रमुख उद्देश्य बनाता ? अगर महर्षि दयानंद को यह ज्ञात होगया होता कि हिन्दी काशी-प्रयाग के सनातनी पंडितों और पंडों की कट्टरता और संकीर्णता की प्रतीक है तो वह क्रांतद्रष्टा महर्षि हिन्दी के झमेले में कदापि न पड़ता। श्री पुरुषोत्तमदास टंडन की घर की जुबान भी अवधी थी। वह फारसी और अंग्रेजी के विलक्षण विद्वान थे। राष्ट्रीयता उनकी नस-नस में कूट-कूटकर भरी थी। वह किसी प्रांतीय भाषा के प्रचार के लिए अपने राजनैतिक और राष्ट्रीय महत्त्व को कदापि दांव पर न लगाते। ताजा उदाहरण आचार्य विनोबा भावे का है। लोकमान्य तिलक के प्रयत्नों से मराठी की लिपि देवनागरी बन गई। विनोबाजी शेष भारतीय भाषाओं की लिपि देवनागरी करने में अहर्निश प्रयत्नशील थे। विनोबाजी उत्तम कोटि के तत्ववेत्ता और विचारक ही नहीं, मराठी के सुप्रसिद्ध लेखक भी थे। उन्हें हिन्दी के झमेले में पड़ने की क्या आवश्यकता थी ! लेकिन उनका कहना था कि हिन्दी के उपकारों को वह कभी नहीं भूल सकते-”यदि हिन्दी भाषा का आधार न होता तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक और असम से केरल तक के गांव-गांव में जाकर भूदान, ग्रामदान का क्रांतिकारी संदेश मैं नहीं पहुंचा सकता था। इसलिए हिन्दी भाषा का मुझ पर उपकार है और हिन्दी भाषा ने मेरी बहुत सेवा की है। अगर मैं मराठी भाषा लेकर जाता तो महाराष्ट्र से बाहर काम नहीं होता।”
एक समय था जब उर्दू हिन्दी से अलग नहीं समझी जाती थी। पंजाबी की तरह वह भी हिन्दी की एक शैली थी। यह मान्यता आज के हिन्दी-प्रचारकों की नहीं है, इसके पीछे लगभग चार सौ वर्षों की पुरानी परंपरा है और अब से पांच-छः दशक पहले तक इस शैली-सिद्धांत को मान्यता भी प्राप्त थी। हिन्दी का नामकरण हिन्दीतर बंधुओं ने किया। इसके प्रचार का कार्य भी हिन्दीतर महामनाओं के द्वारा आगे बढ़ाया गया। यह आज की बात नहीं, स्वराज्य से भी दशाब्दियों पूर्व की बात है, जब पूर्वी भारत में ब्रह्मसमाज, दक्षिणी भारत में वैदिक समाज, पश्चिमी भारत में प्रार्थनासमाज और उत्तर पश्चिमी भारत में स्वामी दयानन्द का आर्यसमाज, हिन्दी को राष्ट्रभाषा मानकर, चारों दिशाओं से हिन्दी के लिए अनथक कार्य कर रहे थे। हिन्दी को क्षेत्रिय सीमाओं में संकुचित करनेवालों को इस तथ्य की अनदेखी नहीं करनी चाहिए कि हिन्दी के अंकुर दिल्ली, जयपुर, लखनऊ, पटना और भोपाल के बजाय स्वातंत्र्य-युद्ध का पहला शंख फूंकने वाले बंगप्रदेश में अंकुरित हुए थे। बीसवीं शताब्दी में स्वराज्य के बाद अंग्रेजी की हिमायत करनवालों की सेवा में हमारा निवेदन है कि सन् 1826 में ‘उदन्त मार्तण्ड’, सन् 1829 में ‘बंगदूत’, सन् 1850 में ‘सुधाकर’ तथा सन् 1854 में ‘समाचार सुधा-वर्षण’ नामक हिन्दी की पत्र-पत्रिकाएं सबसे पहले बंगभूमि से ही प्रकाशित हुई थीं। जब देश में राष्ट्रीय आंदोलन पूरे वेग पर था तो स्वयं स्वर्गीय चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य ने तमिलनाडु के गांव-गांव में घूमकर हिन्दी का प्रचार किया था। अगर हिन्दी साम्राज्यवादिनी होती तो अंग्रेजी साम्राज्यवाद को उखाड़ फेंकनेवाले लोकमान्य तिलक, लाला लाजपतराय, विपिनचंद्र पाल और महात्मा गांधी इसके समर्थन में असाधारण रूप से आगे बढ़ते ? स्वामी दयानंद की भाषा तो गुजराती थी, वह क्यों अपना ‘सत्यार्थ प्रकाश’ हिन्दी में लिखते ? क्यों उनका आर्यसमाज हिन्दी-प्रचार को अपना प्रमुख उद्देश्य बनाता ? अगर महर्षि दयानंद को यह ज्ञात होगया होता कि हिन्दी काशी-प्रयाग के सनातनी पंडितों और पंडों की कट्टरता और संकीर्णता की प्रतीक है तो वह क्रांतद्रष्टा महर्षि हिन्दी के झमेले में कदापि न पड़ता। श्री पुरुषोत्तमदास टंडन की घर की जुबान भी अवधी थी। वह फारसी और अंग्रेजी के विलक्षण विद्वान थे। राष्ट्रीयता उनकी नस-नस में कूट-कूटकर भरी थी। वह किसी प्रांतीय भाषा के प्रचार के लिए अपने राजनैतिक और राष्ट्रीय महत्त्व को कदापि दांव पर न लगाते। ताजा उदाहरण आचार्य विनोबा भावे का है। लोकमान्य तिलक के प्रयत्नों से मराठी की लिपि देवनागरी बन गई। विनोबाजी शेष भारतीय भाषाओं की लिपि देवनागरी करने में अहर्निश प्रयत्नशील थे। विनोबाजी उत्तम कोटि के तत्ववेत्ता और विचारक ही नहीं, मराठी के सुप्रसिद्ध लेखक भी थे। उन्हें हिन्दी के झमेले में पड़ने की क्या आवश्यकता थी ! लेकिन उनका कहना था कि हिन्दी के उपकारों को वह कभी नहीं भूल सकते-”यदि हिन्दी भाषा का आधार न होता तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक और असम से केरल तक के गांव-गांव में जाकर भूदान, ग्रामदान का क्रांतिकारी संदेश मैं नहीं पहुंचा सकता था। इसलिए हिन्दी भाषा का मुझ पर उपकार है और हिन्दी भाषा ने मेरी बहुत सेवा की है। अगर मैं मराठी भाषा लेकर जाता तो महाराष्ट्र से बाहर काम नहीं होता।”
 आज की राजनीति में तो विनोबा-वाक्य भी प्रमाण नहीं रहे। यदि भारत में अंग्रेजी के समर्थकों को अंग्रेजों के कथनों और क्रिया-कलापों से ही सदबुद्धि आती हो तो उन्हें यह जानना चाहिए कि भारत में ईसाई धर्म का प्रवर्तन करने के लिए और यहां की प्रजा से अपना संपर्क स्थापित करने के लिए तत्कालीन अंग्रेज शासकों ने हिन्दी के कोश, व्याकरण और लेखन का निर्माण प्रारंभ करा दिया था। यह काम उन्होंने हिन्दी-प्रदेश में या दिल्ली को अपनी राजधानी बनाकर नहीं, वरन् बंग प्रदेश में, जब उनकी राजधानी कोलकाता थी, तभी उन्होंने हिन्दी को राष्ट्र की भाषा के रूप में अपना लिया था। हिन्दी के महत्व और शक्ति को प्रकट करने वाले प्रसिद्ध अंग्रेज विद्वान् डॉ. ग्रियर्सन के ये वचन क्या आज के अंग्रेजीदां लोगों की आंखें खोल सकेंगे- ”जिन बोलियों से भी हिन्दी का निर्माण हुआ हो, वह मानव-मस्तिष्क के किसी भी विचार को स्फटिक-सदृश स्पष्ट रूप में अभिव्यक्त करने के लिए समर्थ है और पांच सौ वर्षों से रही है। हिन्दी का अपना वृहद् शब्द-भंडार है और गूढ़ विचारों को प्रकट करने के लिए भी उसके पास पूर्ण साधन हैं।”
आज की राजनीति में तो विनोबा-वाक्य भी प्रमाण नहीं रहे। यदि भारत में अंग्रेजी के समर्थकों को अंग्रेजों के कथनों और क्रिया-कलापों से ही सदबुद्धि आती हो तो उन्हें यह जानना चाहिए कि भारत में ईसाई धर्म का प्रवर्तन करने के लिए और यहां की प्रजा से अपना संपर्क स्थापित करने के लिए तत्कालीन अंग्रेज शासकों ने हिन्दी के कोश, व्याकरण और लेखन का निर्माण प्रारंभ करा दिया था। यह काम उन्होंने हिन्दी-प्रदेश में या दिल्ली को अपनी राजधानी बनाकर नहीं, वरन् बंग प्रदेश में, जब उनकी राजधानी कोलकाता थी, तभी उन्होंने हिन्दी को राष्ट्र की भाषा के रूप में अपना लिया था। हिन्दी के महत्व और शक्ति को प्रकट करने वाले प्रसिद्ध अंग्रेज विद्वान् डॉ. ग्रियर्सन के ये वचन क्या आज के अंग्रेजीदां लोगों की आंखें खोल सकेंगे- ”जिन बोलियों से भी हिन्दी का निर्माण हुआ हो, वह मानव-मस्तिष्क के किसी भी विचार को स्फटिक-सदृश स्पष्ट रूप में अभिव्यक्त करने के लिए समर्थ है और पांच सौ वर्षों से रही है। हिन्दी का अपना वृहद् शब्द-भंडार है और गूढ़ विचारों को प्रकट करने के लिए भी उसके पास पूर्ण साधन हैं।”
 विनोबाजी ने अपने संत-स्वभाव के कारण हिन्दी के उपकार को सहज भाव से स्वीकार किया, परन्तु जिन्होंने हिन्दी से सर्वाधिक लाभ उठाकर अपनी और अपने दल की स्थिति को मजबूत किया, उन राजनीतिज्ञों की विडम्बना को हम किन शब्दों में व्यक्त करें ? ये महानुभाव हिन्दी में वोट मांगते हैं, परन्तु कुर्सी पर बैठते ही अंग्रेजी की हिमायत करने लगते हैं। जनता के सामने अंग्रेजी का समर्थन करने की तो हिम्मत जुटा नहीं पाते, किंतु अंग्रेजी-समर्थक अफसरों के सामने अपने को पढ़ा-लिखा सिद्ध करने और कुछ प्रदेशों के मुट्ठीभर हिन्दी-विरोधियों के सामने अल्पसंख्यकों की भाषा के संरक्षक और राष्ट्रीय एकता का दम्भ भरने के लिए राष्ट्रीय स्वाभिमान और अपनी शर्म को भी ताक पर रखकर कहते हैं कि हिन्दी किसी पर लादी नहीं जाएगी। कोई उनसे पूछे कि देश पर और देशी भाषाओं की छाती पर अंग्रेजी लादी जा रही है या हिन्दी ? स्वराज्य के बाद के हमारे शासकों ने हिन्दी की दुर्गति करने में अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी। महात्मा गांधी ने हिन्दी को राष्ट्रभाषा कहा था, लेकिन हमारे ये उदारमना नेता देश की सभी छोटी-बड़ी भाषाओं को राष्ट्रभाषा कहते हैं। संविधान ने हिन्दी को राजभाषा कहा था, लेकिन आज के हमारे शासक और नेता दबी जुबान से, आंखें नीची करके कहते हैं- हां, हिन्दी इस देश की संपर्क-भाषा हो सकती है। इनके कोष में अंग्रेजी के लिए तो अमित आश्वासन भरे हुए हैं, किन्तु हिन्दी पर जो पिछले पांच-छः दशकों से घोर अन्याय हो रहा है उसका प्रतिकार करना तो दूर की बात है, उसके लिए कोई मीठा बोल भी इनके श्रीमुख से नहीं फूटता। कभी ये हिन्दी को क्लिष्ट और असरल कहते हैं, कभी संकीर्ण और दरवाजा बंद करके बैठी हुई भाषा बताते हैं। हिन्दी के चतुर्दिक बढ़ते हुए साहित्य और ज्ञान-विज्ञान के प्रकाशनों से अपरिचित ये लोग बड़े विश्वास के साथ फरमाते हैं कि हिन्दी तो केवल कविता-कहानी की भाषा है। इसमें तकनीकी और विज्ञान-साहित्य की पुस्तकें कहां हैं ? जिन्हें अपने प्रदेश की राजनीति की भी पूरी जानकारी नहीं है, वे संपूर्ण भारत की भाषायी जानकारी का ज्ञान बघारते हुए बतलाते हैं कि भारत की कई प्रादेशिक भाषाओं की क्षमता हिन्दी से बढ़ी-चढ़ी हुई है। भारत का स्वतंत्र कहा जानेवाला प्रेस भी ”नेता-वाक्य प्रमाण” मानकर इन्हें सुर्खियों में छापता रहता है। अज्ञान का ऐसा चमत्कार हम भारत में ही देख सकते हैं, जहां नेता और मंत्री कुर्सी पर बैठते ही सभी विषयों के रातों-रात विशेषज्ञ बन जाते हैं और समाज, साहित्य तथा संस्कृति के विशेषज्ञों के प्रामाणिक निष्कर्षों की ओर भूले से भी यहां ध्यान नहीं दिया जाता।
विनोबाजी ने अपने संत-स्वभाव के कारण हिन्दी के उपकार को सहज भाव से स्वीकार किया, परन्तु जिन्होंने हिन्दी से सर्वाधिक लाभ उठाकर अपनी और अपने दल की स्थिति को मजबूत किया, उन राजनीतिज्ञों की विडम्बना को हम किन शब्दों में व्यक्त करें ? ये महानुभाव हिन्दी में वोट मांगते हैं, परन्तु कुर्सी पर बैठते ही अंग्रेजी की हिमायत करने लगते हैं। जनता के सामने अंग्रेजी का समर्थन करने की तो हिम्मत जुटा नहीं पाते, किंतु अंग्रेजी-समर्थक अफसरों के सामने अपने को पढ़ा-लिखा सिद्ध करने और कुछ प्रदेशों के मुट्ठीभर हिन्दी-विरोधियों के सामने अल्पसंख्यकों की भाषा के संरक्षक और राष्ट्रीय एकता का दम्भ भरने के लिए राष्ट्रीय स्वाभिमान और अपनी शर्म को भी ताक पर रखकर कहते हैं कि हिन्दी किसी पर लादी नहीं जाएगी। कोई उनसे पूछे कि देश पर और देशी भाषाओं की छाती पर अंग्रेजी लादी जा रही है या हिन्दी ? स्वराज्य के बाद के हमारे शासकों ने हिन्दी की दुर्गति करने में अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी। महात्मा गांधी ने हिन्दी को राष्ट्रभाषा कहा था, लेकिन हमारे ये उदारमना नेता देश की सभी छोटी-बड़ी भाषाओं को राष्ट्रभाषा कहते हैं। संविधान ने हिन्दी को राजभाषा कहा था, लेकिन आज के हमारे शासक और नेता दबी जुबान से, आंखें नीची करके कहते हैं- हां, हिन्दी इस देश की संपर्क-भाषा हो सकती है। इनके कोष में अंग्रेजी के लिए तो अमित आश्वासन भरे हुए हैं, किन्तु हिन्दी पर जो पिछले पांच-छः दशकों से घोर अन्याय हो रहा है उसका प्रतिकार करना तो दूर की बात है, उसके लिए कोई मीठा बोल भी इनके श्रीमुख से नहीं फूटता। कभी ये हिन्दी को क्लिष्ट और असरल कहते हैं, कभी संकीर्ण और दरवाजा बंद करके बैठी हुई भाषा बताते हैं। हिन्दी के चतुर्दिक बढ़ते हुए साहित्य और ज्ञान-विज्ञान के प्रकाशनों से अपरिचित ये लोग बड़े विश्वास के साथ फरमाते हैं कि हिन्दी तो केवल कविता-कहानी की भाषा है। इसमें तकनीकी और विज्ञान-साहित्य की पुस्तकें कहां हैं ? जिन्हें अपने प्रदेश की राजनीति की भी पूरी जानकारी नहीं है, वे संपूर्ण भारत की भाषायी जानकारी का ज्ञान बघारते हुए बतलाते हैं कि भारत की कई प्रादेशिक भाषाओं की क्षमता हिन्दी से बढ़ी-चढ़ी हुई है। भारत का स्वतंत्र कहा जानेवाला प्रेस भी ”नेता-वाक्य प्रमाण” मानकर इन्हें सुर्खियों में छापता रहता है। अज्ञान का ऐसा चमत्कार हम भारत में ही देख सकते हैं, जहां नेता और मंत्री कुर्सी पर बैठते ही सभी विषयों के रातों-रात विशेषज्ञ बन जाते हैं और समाज, साहित्य तथा संस्कृति के विशेषज्ञों के प्रामाणिक निष्कर्षों की ओर भूले से भी यहां ध्यान नहीं दिया जाता।
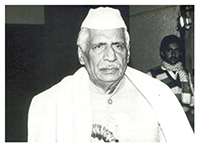 हम देश को प्रांतीयता की परिधि में बांधना उचित नहीं समझते, परन्तु जिन्होंने भाषावार प्रदेशों की रचना करके, प्रदेशों से चुनकर आए संसद-सदस्यों के बहुमत के आधार पर सरकारों का निर्माण किया है, उन्हें यह सोचना चाहिए कि यदि समस्त हिन्दी-प्रदेश और देश के अन्य हिन्दी-प्रेमी प्रदेश तथा अंग्रेजी का समर्थन करने वाले एकाध प्रदेश में बसने वाले हिन्दी-प्रेमियों के मन में यदि लगातार हिन्दी की उपेक्षा के कारण कभी कोई विपरीत भाव पैदा होगया तो उस आक्रोश की भयंकर बाढ़ में किस-किसकी कुर्सी बचेगी, यह कौन कह सकता है ? जनता की आकांक्षा की निरंतर अवहेलना करना, उसकी आस्था को निरंतर आघात पहुंचाना, राष्ट्र के निर्माताओं और स्वप्नद्रष्टाओं के नामों का शोषण करते हुए उनके विचारों के साथ छल करना यदि देशद्रोह नहीं तो देश-प्रेम भी नहीं है। स्वराज्य के बाद की राजनीति ने बात तो की देश की एकता की, लेकिन काम प्रायः एकता को तोड़ने वाले ही किए हैं। राष्ट्र की एकता के प्रतीक होते हैं- राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान और राष्ट्र-संस्कृति। आज की राजनीति सोचती है कि झंडा और राष्ट्रगान ही काफी है। जब राष्ट्रभाषा और सच्ची भावात्मक एकता के बिना देश चल रहा है तो हम यह व्यर्थ का सिरदर्द क्यों मोल लें ? मिश्रित संस्कृति और दुहरी भाषा-नीति से देश की एकता न कहीं कायम हुई है और न कभी कायम होगी। क्षमा कीजिए, हम अत्यंत संकोच के साथ यह कह रहे हैं कि स्वराज्य के बाद देश का पाला ऐसे राजनेताओं से पड़ा है जो भाषा के प्रश्न का सामना करने में अपने को समर्थ नहीं पाते। वे सदैव उससे कतराते रहे हैं। हिन्दी के प्रश्न को उन्होंने हमेशा टाला है और सदैव ‘किन्तु, परन्तु’ से काम लिया है। उन्हें स्मरण रखना चाहिए कि भाषा मातृ-स्वरूपा है। उसके अस्तित्व में सपूतों की जाति कभी संदेह नहीं किया करती। परन्तु हमारे राजनीतिज्ञ भाषा के संबंध में अत्यंत संदेहास्पद रवैया अख्तियार किए हुए हैं। यदि ऐसा नहीं तो हम पूछना चाहते हैं कि पहले राजभाषा आयोग के बाद दूसरा और तीसरा आयोग क्यों नहीं बिठाया गया ? पहले आयोग की सिफारिशें और संसदीय समिति के निर्णय किन परिस्थितियों में और किन दबावों में होते हैं, इसको फिलहाल छोड़ दिया जाए तो हम यह पूछना चाहते हैं कि इन सिफारिशों पर क्या पूरे मन से अमल होता है ? उन निर्णयों के आधार पर जो राजभाषा संबंधी नियम-उपनियम बनाए गए हैं उनका परिचालन कब होता है और कब दबा दिया जाता है, इसकी जांच-पड़ताल कौन करे ? एक प्रदेश के कुछ मुट्ठीभर लोगों को यह आश्वासन दे दिया गया है कि
हम देश को प्रांतीयता की परिधि में बांधना उचित नहीं समझते, परन्तु जिन्होंने भाषावार प्रदेशों की रचना करके, प्रदेशों से चुनकर आए संसद-सदस्यों के बहुमत के आधार पर सरकारों का निर्माण किया है, उन्हें यह सोचना चाहिए कि यदि समस्त हिन्दी-प्रदेश और देश के अन्य हिन्दी-प्रेमी प्रदेश तथा अंग्रेजी का समर्थन करने वाले एकाध प्रदेश में बसने वाले हिन्दी-प्रेमियों के मन में यदि लगातार हिन्दी की उपेक्षा के कारण कभी कोई विपरीत भाव पैदा होगया तो उस आक्रोश की भयंकर बाढ़ में किस-किसकी कुर्सी बचेगी, यह कौन कह सकता है ? जनता की आकांक्षा की निरंतर अवहेलना करना, उसकी आस्था को निरंतर आघात पहुंचाना, राष्ट्र के निर्माताओं और स्वप्नद्रष्टाओं के नामों का शोषण करते हुए उनके विचारों के साथ छल करना यदि देशद्रोह नहीं तो देश-प्रेम भी नहीं है। स्वराज्य के बाद की राजनीति ने बात तो की देश की एकता की, लेकिन काम प्रायः एकता को तोड़ने वाले ही किए हैं। राष्ट्र की एकता के प्रतीक होते हैं- राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान और राष्ट्र-संस्कृति। आज की राजनीति सोचती है कि झंडा और राष्ट्रगान ही काफी है। जब राष्ट्रभाषा और सच्ची भावात्मक एकता के बिना देश चल रहा है तो हम यह व्यर्थ का सिरदर्द क्यों मोल लें ? मिश्रित संस्कृति और दुहरी भाषा-नीति से देश की एकता न कहीं कायम हुई है और न कभी कायम होगी। क्षमा कीजिए, हम अत्यंत संकोच के साथ यह कह रहे हैं कि स्वराज्य के बाद देश का पाला ऐसे राजनेताओं से पड़ा है जो भाषा के प्रश्न का सामना करने में अपने को समर्थ नहीं पाते। वे सदैव उससे कतराते रहे हैं। हिन्दी के प्रश्न को उन्होंने हमेशा टाला है और सदैव ‘किन्तु, परन्तु’ से काम लिया है। उन्हें स्मरण रखना चाहिए कि भाषा मातृ-स्वरूपा है। उसके अस्तित्व में सपूतों की जाति कभी संदेह नहीं किया करती। परन्तु हमारे राजनीतिज्ञ भाषा के संबंध में अत्यंत संदेहास्पद रवैया अख्तियार किए हुए हैं। यदि ऐसा नहीं तो हम पूछना चाहते हैं कि पहले राजभाषा आयोग के बाद दूसरा और तीसरा आयोग क्यों नहीं बिठाया गया ? पहले आयोग की सिफारिशें और संसदीय समिति के निर्णय किन परिस्थितियों में और किन दबावों में होते हैं, इसको फिलहाल छोड़ दिया जाए तो हम यह पूछना चाहते हैं कि इन सिफारिशों पर क्या पूरे मन से अमल होता है ? उन निर्णयों के आधार पर जो राजभाषा संबंधी नियम-उपनियम बनाए गए हैं उनका परिचालन कब होता है और कब दबा दिया जाता है, इसकी जांच-पड़ताल कौन करे ? एक प्रदेश के कुछ मुट्ठीभर लोगों को यह आश्वासन दे दिया गया है कि
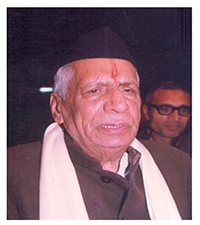 जब तक वे चाहेंगे, अंग्रेजी चलती रहेगी, लेकिन शेष देश के सभी प्रदेशों को अपनी-अपनी भाषा और राजभाषा हिन्दी में काम करने पर तरह-तरह की कानूनी और गैरकानूनी रुकावटें आए दिन डाली जाती हैं। हम पूछना चाहते हैं कि हिन्दी-प्रदेशों में कार्य करनेवाले केंद्रीय सरकार के कार्यालय उन-उन प्रदेशों की सेवाओं के लिए हैं या केंद्र में बैठे हुए कुछ अंग्रेजीदां अफसरों की तानाशाही का हुक्म बजा लाने के लिए हैं ? यदि नहीं तो उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, राजस्थान, बिहार आदि में केंद्रीय कार्यालय वहां की जनता के साथ हिन्दी में कार्य क्यों नहीं करते ? स्वतंत्रता के चौवन वर्ष बाद हिन्दी अभी तक केंद्रीय कार्यालयों में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों तक ही क्यों सीमित है ? क्यों केवल हिन्दी-पत्रों का कृपापूर्वक हिन्दी में उत्तर दे देना ही उनके दायित्व की इतिश्री बन गया है ? क्यों अभी तक योजनाओं के प्रारूप, घोषणाओं और आदेशों के मूलरूप और सरकारी पत्रों के उत्तर पहले अंग्रेजी में ही तैयार होते हैं ? वास्तविकता तो यह है कि यद्यपि भारत सरकार की कथनी में राजकाज द्विभाषी है, परंतु करनी में अभी तक अंग्रेजी ही चल रही है। न कहीं त्रिभाषा सूत्र है और न द्विभाषा फार्मूला। कहने को हिन्दी और करने को अंग्रेजी। क्या इसी का नाम लोकतंत्र है ? लोकमत और लोकभाषा के निरादर से क्या लोकतंत्र की रक्षा हो सकेगी ? जब तक परदेशी की भाषा चलती रहेगी, तब तक स्वदेश में सच्चा लोकतंत्र स्थापित नहीं हो सकता। समाजवाद का नारा भी तब तक खोखला है, जब तक भारतीय समाज को अपनी भाषा के द्वारा प्रेरित और प्रबुद्ध न किया जाए। हम सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता की बात करते हैं और उसके लिए कष्ट तथा हानि भी सहते हैं, परन्तु परहेज हमें है तो सिर्फ भाषायी स्वावलंबन से। हमें तो कभी-कभी ऐसा लगता है कि देश को राजनैतिक गुलामी से मुक्त करके हमारे लोगों ने अपने मन के बंध नहीं काटे हैं, उनका दिल और दिमाग अंग्रेजों के यहां गिरवी रखा हुआ है।
जब तक वे चाहेंगे, अंग्रेजी चलती रहेगी, लेकिन शेष देश के सभी प्रदेशों को अपनी-अपनी भाषा और राजभाषा हिन्दी में काम करने पर तरह-तरह की कानूनी और गैरकानूनी रुकावटें आए दिन डाली जाती हैं। हम पूछना चाहते हैं कि हिन्दी-प्रदेशों में कार्य करनेवाले केंद्रीय सरकार के कार्यालय उन-उन प्रदेशों की सेवाओं के लिए हैं या केंद्र में बैठे हुए कुछ अंग्रेजीदां अफसरों की तानाशाही का हुक्म बजा लाने के लिए हैं ? यदि नहीं तो उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, राजस्थान, बिहार आदि में केंद्रीय कार्यालय वहां की जनता के साथ हिन्दी में कार्य क्यों नहीं करते ? स्वतंत्रता के चौवन वर्ष बाद हिन्दी अभी तक केंद्रीय कार्यालयों में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों तक ही क्यों सीमित है ? क्यों केवल हिन्दी-पत्रों का कृपापूर्वक हिन्दी में उत्तर दे देना ही उनके दायित्व की इतिश्री बन गया है ? क्यों अभी तक योजनाओं के प्रारूप, घोषणाओं और आदेशों के मूलरूप और सरकारी पत्रों के उत्तर पहले अंग्रेजी में ही तैयार होते हैं ? वास्तविकता तो यह है कि यद्यपि भारत सरकार की कथनी में राजकाज द्विभाषी है, परंतु करनी में अभी तक अंग्रेजी ही चल रही है। न कहीं त्रिभाषा सूत्र है और न द्विभाषा फार्मूला। कहने को हिन्दी और करने को अंग्रेजी। क्या इसी का नाम लोकतंत्र है ? लोकमत और लोकभाषा के निरादर से क्या लोकतंत्र की रक्षा हो सकेगी ? जब तक परदेशी की भाषा चलती रहेगी, तब तक स्वदेश में सच्चा लोकतंत्र स्थापित नहीं हो सकता। समाजवाद का नारा भी तब तक खोखला है, जब तक भारतीय समाज को अपनी भाषा के द्वारा प्रेरित और प्रबुद्ध न किया जाए। हम सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता की बात करते हैं और उसके लिए कष्ट तथा हानि भी सहते हैं, परन्तु परहेज हमें है तो सिर्फ भाषायी स्वावलंबन से। हमें तो कभी-कभी ऐसा लगता है कि देश को राजनैतिक गुलामी से मुक्त करके हमारे लोगों ने अपने मन के बंध नहीं काटे हैं, उनका दिल और दिमाग अंग्रेजों के यहां गिरवी रखा हुआ है।
 कहने को बहुत कुछ है, लेकिन परस्पर दोषारोपण से कोई लाभ नहीं। अगर हम प्रारंभ में ही हिन्दी के लिए चौदह वर्ष का स्वेच्छा वनवास स्वीकार न कर लेते और हिन्दी के प्रचार तथा राजभाषा के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी सरकार पर डालकर निश्चिंत न हो जाते तो आज हमें ये दिन न देखने पड़ते। अंग्रेजों की बनाई मशीनरी वाले शासन तंत्र से अंग्रेजी को उखाड़ फेंकना न तब संभव था और न आज सहज है। अंग्रेजी और ब्यूरोक्रेसी एक-दूसरे के पर्याय हैं। जब तक इस देश की लगाम ब्यूरोक्रेसी के हाथों में रहेगी तब तक देश की छाती पर अंग्रेजी के घोड़े दौड़ते ही रहेंगे। इसके विपरीत हिन्दी भारतीयता की, राष्ट्रीय स्वाभिमान की, परंपरा और प्रगति की प्रतीक है। जिस दिन राजकाज की बागडोर हिन्दी के हाथ में आई, उसी दिन राष्ट्रीयता, भावात्मक एकता, मौलिक अनुसंधान और ठोस उपलब्धियों तथा विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति के पथ उजागर हो उठेंगे। हिन्दी विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की भाषा होने के कारण शीघ्र ही ‘तीसरे विश्व’ की संपर्क भाषा बनकर एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में विश्व-मंच पर अवतीर्ण हो जाएगी। वह क्षण विश्व-शांति और विश्वबंधुत्व के लिए एक ऐतिहासिक वरदान बन जाएगा।
कहने को बहुत कुछ है, लेकिन परस्पर दोषारोपण से कोई लाभ नहीं। अगर हम प्रारंभ में ही हिन्दी के लिए चौदह वर्ष का स्वेच्छा वनवास स्वीकार न कर लेते और हिन्दी के प्रचार तथा राजभाषा के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी सरकार पर डालकर निश्चिंत न हो जाते तो आज हमें ये दिन न देखने पड़ते। अंग्रेजों की बनाई मशीनरी वाले शासन तंत्र से अंग्रेजी को उखाड़ फेंकना न तब संभव था और न आज सहज है। अंग्रेजी और ब्यूरोक्रेसी एक-दूसरे के पर्याय हैं। जब तक इस देश की लगाम ब्यूरोक्रेसी के हाथों में रहेगी तब तक देश की छाती पर अंग्रेजी के घोड़े दौड़ते ही रहेंगे। इसके विपरीत हिन्दी भारतीयता की, राष्ट्रीय स्वाभिमान की, परंपरा और प्रगति की प्रतीक है। जिस दिन राजकाज की बागडोर हिन्दी के हाथ में आई, उसी दिन राष्ट्रीयता, भावात्मक एकता, मौलिक अनुसंधान और ठोस उपलब्धियों तथा विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति के पथ उजागर हो उठेंगे। हिन्दी विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की भाषा होने के कारण शीघ्र ही ‘तीसरे विश्व’ की संपर्क भाषा बनकर एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में विश्व-मंच पर अवतीर्ण हो जाएगी। वह क्षण विश्व-शांति और विश्वबंधुत्व के लिए एक ऐतिहासिक वरदान बन जाएगा।
राजनीति का मूल धर्म यद्यपि जन-सेवा है, लेकिन हमें यह नहीं भूल जाना चाहिए कि उसका नाम राजनीति है, समाजनीति, संस्कृतिनीति या भाषानीति नहीं है। राजनयिक पहले राज की बात सोचते हैं कि वह कैसे शांतिपूर्वक तरीके से चले और किस तरह उस पर उनका कब्जा बना रहे। इस रास्ते में जो भी वस्तु उनके लिए बाधा या असहज होती है, वे या तो उसे नष्ट कर देते हैं या फिर पंगु बनाकर एक कोने में पटक देते हैं। राज चलाने के लिए वे किसी से समझौता कर सकते हैं और किसी से संघर्ष भी कर सकते हैं। आज की राजनीति का स्वर संसारभर में भौतिक ही है। जिस रीति से भौतिक समृद्धि बढ़े वही उनका प्रथम कर्त्तव्य है। सांस्कृतिक, साहित्यिक और भाषायी प्रगति तो उनके लिए ‘अघाये की ब्यालू’ है। लेकिन जो राष्ट्र को व्यापक परिवेश में स्वीकारते हैं, जो उसकी आत्मा को पहचानते हैं अथवा जो सच्चे राष्ट्रीय स्वाभिमान से अनुप्राणित हैं, उनका यह काम नहीं कि सरकार के मुखापेक्षी बन जाएं। भारत में भारतीयता का, ऊंचे सिद्धांतों का, मानवता का, सदविचारों का और सत्साहित्य एवं सर्वसम्मत भाषा का प्रचार कभी किसी सरकार ने नहीं किया। यह कार्य किया है संतों ने, राष्ट्र-निर्माता और समाज-सुधारक नेताओं ने, या फिर धुन के दीवानों ने। हिन्दी को ही लें, आज हमारा मानस यह बन गया है कि हम कुछ न करें, सरकार और नेता हिन्दी के संबंध में यह करें और वह कर दें। जैसा हमने ऊपर कहा वैसे ही दोषारोपण की प्रवृत्ति हिन्दी के लोगों में बढ़ गई है- सरकार ने वह नहीं किया और यह नहीं करती, संस्थाओं ने वह नहीं किया और यह नहीं करतीं तथा हमें छोड़कर शेष सभी को वह करना चाहिए और यह करना चाहिए। लेकिन हम यह कभी नहीं सोचते कि हमारा भी कोई कर्तव्य है या नहीं ? हम लोग स्वयं अपनी सुविधा के लिए अंग्रेजी का व्यवहार करते हैं, लेकिन दूसरों के अंग्रेजी व्यवहार करने पर आपत्ति उठाते हैं।
अपने बच्चों को कॉन्वेंटों में पढ़ाते हैं और मांग करते हैं ऐसे अंग्रेजी स्कूलों को बंद करने की। हिन्दी-प्रदेश के निवासी भी जब अपने नामपट्ट अंग्रेजी से हिन्दी में नहीं बदलवाते हैं, अपने उत्सवों और संस्कारों के पत्र अभी तक अंग्रेजी में छपवाते हैं, हिन्दी की पत्र-पत्रिकाओं को छोड़कर अंग्रेजी पत्र-पत्रिकाएं पढ़ते हैं और मुंह से हिन्दी की बात करते हुए अंग्रेजी के मुकाबिले हिन्दी को हीन मानते हैं तो हिन्दी का प्रचार कैसे होगा ? हम केंद्रीय सरकार से तो हिन्दी के व्यवहार को बढ़ाने की अपील करते हैं, लेकिन हिन्दी-प्रदेशों की सरकारों में, वहां के न्यायालयों में, शिक्षण-संस्थाओं में, व्यापार और व्यवहार में धड़ल्ले से जो अंग्रेजी चल रही है, उसके लिए कुछ नहीं करते। हम प्रदेश सरकारों की हिन्दी संबंधी घोषणाओं से संतुष्ट हो जाते हैं, लेकिन हिन्दी की संस्थाएं या हिन्दी के नेता तथा कार्यकर्ता कभी ऐसा कष्ट नहीं करते कि वे सरकारों के अंग्रेजी-कार्य पर निगरानी रखें और जहां-जहां वह अनुचित रूप से थोपी जा रही है, उसका वैध तरीके से जनमत बनाकर प्रतिकार करें।
 अब हिन्दी के संबंध में कहने, लिखने और तर्क देने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा कौन सा तर्क है जो हिन्दी के संबंध में देने से बच गया हो ? हिन्दी के संबंध में गांधीजी ने जितना कहा है उतना कोई क्या कहेगा ? जब भाषा के संबंध में गांधीजी की बात नहीं सुनी जाती, तब हमारी-आपकी कौन सुनेगा। इसलिए कहो मत, करो ! गांधीजी ने कहा ही नहीं, किया भी। उन्होंने हिन्दी साहित्य सम्मेलन के दो बार सभापति रहकर हिन्दी को बल प्रदान किया। ‘दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा’ का निर्माण करके दक्षिण के चारों प्रदेशों में घर-घर हिन्दी की ज्योति जगाई। शेष हिन्दीतर राज्यों में हिन्दी के प्रचार के लिए उन्होंने वर्धा में ‘राष्ट्रभाषा प्रचार समिति’ का गठन किया। वह हिन्दी की प्रतिष्ठा के लिए उसका नाम हिन्दुस्तानी तक करने के लिए तैयार होगए, लेकिन अपने को हिन्दीजन कहने वाले लोगों ने न तब कुछ किया और न आज हिन्दी के लिए कुछ कर रहे हैं। उन्होंने हिन्दी-संस्थाओं पर कब्जा करने और उनके कार्यों में रुकावट डालने का ही सतत् प्रयत्न किया है। कथनी और करनी से उन्होंने हिन्दीतर भाइयों को हिन्दी के प्रति उदासीन होने में ही अपनी विशिष्ट भूमिका निभाई है।
अब हिन्दी के संबंध में कहने, लिखने और तर्क देने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा कौन सा तर्क है जो हिन्दी के संबंध में देने से बच गया हो ? हिन्दी के संबंध में गांधीजी ने जितना कहा है उतना कोई क्या कहेगा ? जब भाषा के संबंध में गांधीजी की बात नहीं सुनी जाती, तब हमारी-आपकी कौन सुनेगा। इसलिए कहो मत, करो ! गांधीजी ने कहा ही नहीं, किया भी। उन्होंने हिन्दी साहित्य सम्मेलन के दो बार सभापति रहकर हिन्दी को बल प्रदान किया। ‘दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा’ का निर्माण करके दक्षिण के चारों प्रदेशों में घर-घर हिन्दी की ज्योति जगाई। शेष हिन्दीतर राज्यों में हिन्दी के प्रचार के लिए उन्होंने वर्धा में ‘राष्ट्रभाषा प्रचार समिति’ का गठन किया। वह हिन्दी की प्रतिष्ठा के लिए उसका नाम हिन्दुस्तानी तक करने के लिए तैयार होगए, लेकिन अपने को हिन्दीजन कहने वाले लोगों ने न तब कुछ किया और न आज हिन्दी के लिए कुछ कर रहे हैं। उन्होंने हिन्दी-संस्थाओं पर कब्जा करने और उनके कार्यों में रुकावट डालने का ही सतत् प्रयत्न किया है। कथनी और करनी से उन्होंने हिन्दीतर भाइयों को हिन्दी के प्रति उदासीन होने में ही अपनी विशिष्ट भूमिका निभाई है।
उन्होंने उनका और अंग्रेजी समर्थकों का दिल जीतने की कभी कोशिश नहीं की। अपनी अहंमन्यता और यहां तक कहें कि दुर्बुद्धि से उन्होंने हिन्दी के दुश्मन ही बढ़ाए हैं, मित्र नहीं। इसलिए यह आवश्यक है कि ऐसे सब लोग फिर से सोचें और अपने कर्तव्य का पुनर्निधारण करें। जो अपना मत न बदल सकें, उन्हें कृपया हिन्दी-आंदोलन से हट जाना चाहिए। हिन्दी सेवा का पथ है, प्राप्ति का साधन नहीं। हिन्दी प्रेम से आगे बढ़ेगी, सरकार की तलवार या संविधान की ढाल लेकर नहीं। हिन्दी के कार्य को सद्धर्म-बुद्धि से करने की आवश्यकता है। राजनैतिक तरीके से प्रपंच, गुटबंदी, वक्तव्य, भाषण और लेखनों से हिन्दी का भला होने वाला नहीं है।
हिन्दी के पक्षधरों को देश में सुमति के भाव जागृत करने हैं। देशवासियों में राष्ट्रीयता की भावना पैदा करनी है। राष्ट्रीय स्वाभिमान को फिर से जागृत करना है। राष्ट्रभाषा का यही पुनीत धर्म है। हिन्दी अगर राजभाषा न बन पाए तो इसमें कोई आपत्ति नहीं, किंतु सच्चे अर्थों में हिन्दी को राष्ट्रवाणी बनाने के कार्य में प्रत्येक राष्ट्रभक्त को लग जाना चाहिए। हिन्दी और राष्ट्र यानी हिन्द दो भिन्न वस्तुएं नहीं हैं। हिन्दी हिन्द का पर्याय है। हिन्दी को सच्चे अर्थों में भारत की आत्मा बनना चाहिए। राष्ट्रभाषा वही हो सकती है जो राष्ट्र की वाणी बनने के उत्तरदायित्व का सही रूप में वहन कर सके। हिन्दी के लेखक, प्रकाशक, पत्रकार अपना दिल टटोलें और सोचें कि हिन्दी को राष्ट्रवाणी बनाने में उनकी भूमिका क्या है ? पुरानी पीढ़ी अपना काम जितना कर सकती थी, कर चुकी। अब हिन्दी को नए तेज से प्रदीप्त करने के लिए आज की तरुणाई को आगे आना चाहिए और यह तय करना चाहिए कि हम हिन्द की सेवा हिन्दी के माध्यम से करें, भले ही इसके लिए उनकी समूची पीढ़ी को नौकरियों और सुविधाओं से वंचित ही क्यों न हो जाना पड़े।
जो बात सबसे महत्वपूर्ण है, वह यह है कि राष्ट्रभाषा समूचे देश के लिए है, केवल कुछ प्रदेशों के लिए नहीं। जब तक हम अन्य हिन्दीतर प्रदेशों को राष्ट्रभाषा के लिए अग्रसर नहीं करेंगे, तब तक हिन्दी सच्चे अर्थों में राष्ट्रभाषा नहीं बनेगी।
यह तभी होगा जब हिन्दी-आंदोलन के सूत्र हिन्दीवालों से निकलकर हिन्दीतर क्षेत्रों में पहुंचेंगे। ये तभी पहुंचेंगे जब हमारे हिन्दीतर भाइयों को यह विश्वास हो जाए कि हिन्दी उनकी मातृभाषा का नहीं, अंग्रेजी का स्थान लेने वाली है। यह तभी हो सकेगा जब हम हिन्दीवाले लोग हिन्दीतर भाइयों के राष्ट्रप्रेम और राष्ट्र-निर्माण में उनकी साझेदारी के प्रति संदेह के भाव रखना छोड़ दें। हम उनके प्रति विश्वास बनाकर ही अपने प्रति उन्हें विश्वासी बना सकते हैं। हम यह क्यों नहीं समझते कि हिन्दी यदि निखिल हिन्द की भाषा है तो उसे बनाने, बढ़ाने और फैलाने का दायित्व भी समूचे हिन्द का है। हिन्दीवालों की भूमिका इसमें पक्षधरों की न होकर सहायक निष्पक्षों की होनी चाहिए। जब हम विदेशों से और पड़ोसी देशों से सद्व्यवहार बढ़ा सकते हैं, उनके साथ सांस्कृतिक संबंध मजबूत कर सकते हैं तो अपने ही देश के हिन्दीतर प्रदेशों में बसने वाले कदाचित् हमसे भी अधिक भारतीय लोगों के साथ हार्दिक सौमनस्य स्थापित क्यों नहीं कर सकते ? हिन्दी को लेकर अपने और पराए का भाव देश में पैदा हो- इससे अधिक अनिष्टकर बात और क्या हो सकती है ? स्मरण रखिए, हिन्दी जोड़ने वाली भाषा है, तोड़ने वाली नहीं। हिन्दीवालों के किसी भी कदम से हिन्दी को, उसकी भावात्मक एकता को तोड़ने की गंध तक नहीं आनी चाहिए। हिन्दीवाले भला या बुरा, अपना कार्य कर चुके। अब उन्हें उदारता से यह घोषित कर देना चाहिए कि समस्त देश की सभी भाषाएं, उनके लेखक और बुद्धिजीवी मिलकर इस राष्ट्रीय यज्ञ की ज्योति-शिखा को प्रदीप्त करें। जैसे भारत की स्वतंत्रता में देश के हर नागरिक ने, प्रत्येक प्रदेश के निवासियों ने और भारत के सभी नेताओं ने मिलकर सामूहिक प्रयत्न किया था, वैसे ही हिन्दी के गोवर्धन को उठाने का अकेला दायित्व हिन्दी प्रदेश नहीं उठा सकते। इसमें भी प्रदेश-प्रदेश के गोपी-ग्वालों की लकुटिया लगनी ही चाहिए, तभी गोवर्धन उठ पाएगा और देश की रक्षा अंग्रेजी की प्रलंयकारी बाढ़ से हो सकेगी।
(‘बिन हिन्दी सब सून’ से, सन् 2002)