 न मैं हास्यरसावतार हूं और न हास्यसम्राट। आज के वैज्ञानिक युग में अवतारवादिता और लोकतंत्रीय व्यवस्था में साम्राज्य स्थापित करने की या उस पर डटे रहने की गुंजाइश ही कहां बची है ? जब मेरे लिए लोग इन विशेषणों का प्रयोग करते हैं तो मैं जानता हूं कि या तो वे मुझे मक्खन लगा रहे हैं अथवा मूर्ख बना रहे हैं। मैंने हिन्दी में हास्यरस का प्रारंभ किया है, यह कहना और समझना भी सही नहीं है। सच तो यह है कि मुझसे पहले बाबू भारतेन्दु हरिश्चंद्र (अंधेर नगरी चौपट राजा), प्रतापनारायण मिश्र, बाबू बालमुकुंद गुप्त (शिव-शंभु का चिट्ठा), जी0 पी0 श्रीवास्तव (दुमदार आदमी), अकबर इलाहाबादी आदि हास्य-पादप का बीजारोपण कर चुके थे। मेरे बारे में सही सिर्फ इतना है कि मैंने हास्यरस लिखा है और जिया भी है। साहित्य लिखना एक अलग बात है। उसे बहुतों ने लिखा है और लिखते रहेंगे। लेकिन साहित्यिक जीवन जीना शायद लेखन-कर्म से भी कठिन कार्य है। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं जो लिखने के लिए व्यंग्य-विनोद लिखते हैं, लेकिन उनके व्यक्तित्व में, परिवार में या सामाजिक परिवेश में उसका नामोनिशान नहीं मिलता। क्योंकि मैं पिछले पचास वर्षों से ऊपर इस ‘हास्य-सागर’ में अवगाहन करता रहा हूं, इसलिए हास्य मेरे जीवन का अंग बन गया है। मेरी रुचि, स्वभाव और संस्कार बहुत दिनों से ऐसे होगए हैं कि मैं जो लिखता हूं या कहता हूं और करता आया हूं, उसमें अनायास व्यंग्य-विनोद का पुट आ ही जाता है। इसके कारण मेरे कृतित्व और व्यक्तित्व के संपर्क में आने वाले लोग जहां गदगद होते हैं, मुस्कराते हैं और ठहाके लगाते हैं, वहां गंभीरता का मुखौटा पहने हुए कुछ लोग दुःखी भी कम नहीं होते। क्योंकि हास्य-व्यंग्य साहित्य की ऐसी मनमोहिनी विधा है कि इसको लिखने वाला जल्दी ही सिद्ध और प्रसिद्ध हो जाता है। इससे समानधर्मी लोगों और कुंठित व्यक्तित्वों में ईर्ष्या भी पैदा होती है। मैं भी जीवन में शायद इसी कारण ईर्ष्या का शिकार हुआ हूं। परंतु यह मेरे वश की बात नहीं। हां, इतना अवश्य कह सकता हूं कि मेरा मन जानबूझकर किसी के प्रति विकारी नहीं रहा। मैं उनके प्रति क्षमाप्रार्थी हूं, जिनके कदली-पत्र जैसे कोमल तथा भावुक मन को मेरे सहज-स्वभावी व्यंग्य-बाणों ने छेद दिया हो।
न मैं हास्यरसावतार हूं और न हास्यसम्राट। आज के वैज्ञानिक युग में अवतारवादिता और लोकतंत्रीय व्यवस्था में साम्राज्य स्थापित करने की या उस पर डटे रहने की गुंजाइश ही कहां बची है ? जब मेरे लिए लोग इन विशेषणों का प्रयोग करते हैं तो मैं जानता हूं कि या तो वे मुझे मक्खन लगा रहे हैं अथवा मूर्ख बना रहे हैं। मैंने हिन्दी में हास्यरस का प्रारंभ किया है, यह कहना और समझना भी सही नहीं है। सच तो यह है कि मुझसे पहले बाबू भारतेन्दु हरिश्चंद्र (अंधेर नगरी चौपट राजा), प्रतापनारायण मिश्र, बाबू बालमुकुंद गुप्त (शिव-शंभु का चिट्ठा), जी0 पी0 श्रीवास्तव (दुमदार आदमी), अकबर इलाहाबादी आदि हास्य-पादप का बीजारोपण कर चुके थे। मेरे बारे में सही सिर्फ इतना है कि मैंने हास्यरस लिखा है और जिया भी है। साहित्य लिखना एक अलग बात है। उसे बहुतों ने लिखा है और लिखते रहेंगे। लेकिन साहित्यिक जीवन जीना शायद लेखन-कर्म से भी कठिन कार्य है। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं जो लिखने के लिए व्यंग्य-विनोद लिखते हैं, लेकिन उनके व्यक्तित्व में, परिवार में या सामाजिक परिवेश में उसका नामोनिशान नहीं मिलता। क्योंकि मैं पिछले पचास वर्षों से ऊपर इस ‘हास्य-सागर’ में अवगाहन करता रहा हूं, इसलिए हास्य मेरे जीवन का अंग बन गया है। मेरी रुचि, स्वभाव और संस्कार बहुत दिनों से ऐसे होगए हैं कि मैं जो लिखता हूं या कहता हूं और करता आया हूं, उसमें अनायास व्यंग्य-विनोद का पुट आ ही जाता है। इसके कारण मेरे कृतित्व और व्यक्तित्व के संपर्क में आने वाले लोग जहां गदगद होते हैं, मुस्कराते हैं और ठहाके लगाते हैं, वहां गंभीरता का मुखौटा पहने हुए कुछ लोग दुःखी भी कम नहीं होते। क्योंकि हास्य-व्यंग्य साहित्य की ऐसी मनमोहिनी विधा है कि इसको लिखने वाला जल्दी ही सिद्ध और प्रसिद्ध हो जाता है। इससे समानधर्मी लोगों और कुंठित व्यक्तित्वों में ईर्ष्या भी पैदा होती है। मैं भी जीवन में शायद इसी कारण ईर्ष्या का शिकार हुआ हूं। परंतु यह मेरे वश की बात नहीं। हां, इतना अवश्य कह सकता हूं कि मेरा मन जानबूझकर किसी के प्रति विकारी नहीं रहा। मैं उनके प्रति क्षमाप्रार्थी हूं, जिनके कदली-पत्र जैसे कोमल तथा भावुक मन को मेरे सहज-स्वभावी व्यंग्य-बाणों ने छेद दिया हो।
 जीवन में हास्यरस मुझे वरदान की तरह प्राप्त हुआ है। इससे मुझे सहज में ही सिद्धि और प्रसिद्धि, यानी यश और जीवन-साधन प्राप्त हुए हैं। यदि मेरे लेखन में हास्य नहीं आता तो हिन्दी में और साहित्य-समाज में मेरी पैठ नहीं होती। इसी के बल पर मुझे पत्रकारिता में प्रवेश मिला। इसी के कारण मुझे ‘पद्मश्री’ सहित अनेक राजकीय एवं सामाजिक अलंकरणों और पुरस्कारों की भी प्राप्ति संभव हुई। इसी वजह से देश और विदेश में, जहां हिन्दीप्रेमी बसते हैं, मैं भी पांचवें सवार की तरह पहुंच गया। इन बातों को लगभग सभी लोग जानते हैं। जिन बातों को नहीं जानते उनमें से कुछेक लिख रहा हूं- अगर हास्यरस का संबल मेरे पास नहीं होता तो जीवन में जो अभाव, उपेक्षा और शोषण का शिकार मुझे होना पड़ा, उनसे मैं टूट ही जाता। मेरी मां क्षय रोग से दिवंगत हुई थीं। एक बार डॉक्टरों ने मुझमें भी इसके रोगाणु खोज निकाले। कई महीनों तक खांसी, बलगम, बुखार आदि का शिकार रहा। मैंने कोई खास दवा नहीं की। तब आज की तरह इसका कोई सक्षम उपचार भी विकसित नहीं हुआ था। मैंने इसको दूर करने के लिए हास्यरस के डोज़ लिए और
भला-चंगा होगया।
जीवन में हास्यरस मुझे वरदान की तरह प्राप्त हुआ है। इससे मुझे सहज में ही सिद्धि और प्रसिद्धि, यानी यश और जीवन-साधन प्राप्त हुए हैं। यदि मेरे लेखन में हास्य नहीं आता तो हिन्दी में और साहित्य-समाज में मेरी पैठ नहीं होती। इसी के बल पर मुझे पत्रकारिता में प्रवेश मिला। इसी के कारण मुझे ‘पद्मश्री’ सहित अनेक राजकीय एवं सामाजिक अलंकरणों और पुरस्कारों की भी प्राप्ति संभव हुई। इसी वजह से देश और विदेश में, जहां हिन्दीप्रेमी बसते हैं, मैं भी पांचवें सवार की तरह पहुंच गया। इन बातों को लगभग सभी लोग जानते हैं। जिन बातों को नहीं जानते उनमें से कुछेक लिख रहा हूं- अगर हास्यरस का संबल मेरे पास नहीं होता तो जीवन में जो अभाव, उपेक्षा और शोषण का शिकार मुझे होना पड़ा, उनसे मैं टूट ही जाता। मेरी मां क्षय रोग से दिवंगत हुई थीं। एक बार डॉक्टरों ने मुझमें भी इसके रोगाणु खोज निकाले। कई महीनों तक खांसी, बलगम, बुखार आदि का शिकार रहा। मैंने कोई खास दवा नहीं की। तब आज की तरह इसका कोई सक्षम उपचार भी विकसित नहीं हुआ था। मैंने इसको दूर करने के लिए हास्यरस के डोज़ लिए और
भला-चंगा होगया।
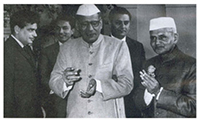 इसी तरह जवानी उतरते-उतरते आंखों ने धोखा दिया और कान भी आनाकानी करने लगे। कहावत है कि ‘कान गए अहंकार गया और आंख गईं संसार गया।’ जब देखते-देखते संसार अचानक धूमिल हो जाए तो आदमी पर क्या बीतती है ? इसे कोई भुक्तभोगी ही जान सकता है। अगर हास्यरस मेरे पास न होता तो मैं भी इस अनभ्र वज्रपात से टूटकर बिखर गया होता। लेकिन विधाता के इस क्रूर व्यंग्य पर मैं रोया नहीं, मुस्कराकर खड़ा होगया। आंखों के अभाव को मैंने अभिशाप न मानकर, वरदान के रूप में ही ग्रहण किया। मेरे जीवन में जो उल्लेखनीय सफलताएं आईं, वे सब नेत्र-रोग से ग्रसित हो जाने के बाद ही सुलभ हुईं। पत्रकारिता में आंखों की कमजोरी के बावजूद उपसंपादक से मुख्य उपसंपादक और मुख्य उपसंपादक से सह-संपादक तक
पहुंचा। उसके बाद कुछ महीनों के लिए ही सही, एक दैनिक पत्र का प्रधान संपादक भी बन गया। मुझे ‘पद्मश्री’ भी इसी अवधि में मिली। मेरे स्वर्ण-जयंती और हीरक-जयंती समारोह भी राजधानी तथा देश के कई नगरों में धूमधाम से मनाए गए। विशाल अभिनंदन-ग्रंथ भी मुझे इसी समय में भेंट किया गया। मेरी छहों संतानों की उच्च शिक्षा, शादी-विवाह और नौकरियां आदि भी इसी अवधि में संपन्न हुईं।
इसी तरह जवानी उतरते-उतरते आंखों ने धोखा दिया और कान भी आनाकानी करने लगे। कहावत है कि ‘कान गए अहंकार गया और आंख गईं संसार गया।’ जब देखते-देखते संसार अचानक धूमिल हो जाए तो आदमी पर क्या बीतती है ? इसे कोई भुक्तभोगी ही जान सकता है। अगर हास्यरस मेरे पास न होता तो मैं भी इस अनभ्र वज्रपात से टूटकर बिखर गया होता। लेकिन विधाता के इस क्रूर व्यंग्य पर मैं रोया नहीं, मुस्कराकर खड़ा होगया। आंखों के अभाव को मैंने अभिशाप न मानकर, वरदान के रूप में ही ग्रहण किया। मेरे जीवन में जो उल्लेखनीय सफलताएं आईं, वे सब नेत्र-रोग से ग्रसित हो जाने के बाद ही सुलभ हुईं। पत्रकारिता में आंखों की कमजोरी के बावजूद उपसंपादक से मुख्य उपसंपादक और मुख्य उपसंपादक से सह-संपादक तक
पहुंचा। उसके बाद कुछ महीनों के लिए ही सही, एक दैनिक पत्र का प्रधान संपादक भी बन गया। मुझे ‘पद्मश्री’ भी इसी अवधि में मिली। मेरे स्वर्ण-जयंती और हीरक-जयंती समारोह भी राजधानी तथा देश के कई नगरों में धूमधाम से मनाए गए। विशाल अभिनंदन-ग्रंथ भी मुझे इसी समय में भेंट किया गया। मेरी छहों संतानों की उच्च शिक्षा, शादी-विवाह और नौकरियां आदि भी इसी अवधि में संपन्न हुईं।
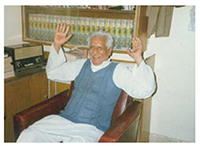 यही नहीं, नई दिल्ली के गुलमोहर पार्क में मेरा मकान भी आखिर बन ही गया। इसी आलम में मेरे द्वारा ‘राजर्षि टंडन अभिनंदन ग्रंथ’, ‘गांधी हिन्दी दर्शन’ नामक वृहद ग्रंथ और ‘ब्रज विभव’ महाग्रंथ संपादित हुए। इन उपलब्धियों के अतिरिक्त मैंने इसी बीच दो दर्जन से अधिक पुस्तकें लिखीं और हास्यरस का खंडकाव्य ‘अनारी नर’ भी लिख डाला। अपने व्यंग्य-विनोदी स्तंभों की एक-साथ छह पुस्तकें भी इसी बीच संकलित करके प्रकाशित करा दीं। जैसे महाकवि सूरदास ने महाप्रभु वल्लभाचार्य की प्रेरणा से ब्रज में गोवर्धन पर्वत पर अपनी देखरेख में श्रीनाथजी का मंदिर बनवाकर खड़ा कर दिया था, उसी प्रकार मैंने सूरदासजी की निर्वाणस्थली और अपनी जन्मस्थली परासौली (परम रासस्थली) में एक सारस्वत पीठ और मां शारदा का मंदिर बनवा दिया तथा उनके कर-कमलों में महारासस्थली की कल्पना के अनुसार वीणा के स्थान पर वेणु थमा दी। ये सब हास्यरस की कृपा के फल हैं। मैंने जीवन में से मस्ती को नहीं जाने दिया। उस अहं को भी विकसित करता रहा जो कृतिकार के सृजन को प्रेरित करता है और प्रतिपक्षी की उपेक्षा के प्रति सक्षम होता है। ऐसा वही कर सकता है, जिसके अंदर आनंद का सागर लहराता हो और जिसके मन-मानस में उत्साह के कमल खिलते रहते हों। ये आनंदीवृत्ति और अटूट उत्साह मुझे हास्यरस की अनुकंपा से ही प्राप्त हुए हैं। जब भाई स्व0 प्रफुल्लचंद्र ओझा ‘मुक्त’ मुझे आनंदमूर्ति कहकर संबोधित करते थे तो छिपाऊंगा नहीं, बहुत अच्छा लगता था। सबसे पहले यह आनंदमूर्ति का अलंकरण मुझे आदरणीया बहन महादेवी वर्मा ने दिया था। मैं चाहता हूं और ईश्वर से प्रार्थना भी करता हूं कि वास्तव में आनंदमूर्ति बनने की क्षमता मुझमें आ जाए। आनंद ही जीवन का परम इष्ट है। वही चिदानंद है, नित्यानंद है और सच्चिदानंद है। मुक्ति-पथ क्या है ? परमानंद की डगर ही तो है ! इस आनंद से ही मनुष्य कर्म-विपाक से छूटता है। इस आनंद से ही जगत की माया उसे नहीं व्यापती। वह इसी आनंद से सच्चिदानंद की शाश्वत शरण में पहुंच जाता है। हास्यरस इस आनंद तक पहुंचने का सबसे सुगम मार्ग है।
यही नहीं, नई दिल्ली के गुलमोहर पार्क में मेरा मकान भी आखिर बन ही गया। इसी आलम में मेरे द्वारा ‘राजर्षि टंडन अभिनंदन ग्रंथ’, ‘गांधी हिन्दी दर्शन’ नामक वृहद ग्रंथ और ‘ब्रज विभव’ महाग्रंथ संपादित हुए। इन उपलब्धियों के अतिरिक्त मैंने इसी बीच दो दर्जन से अधिक पुस्तकें लिखीं और हास्यरस का खंडकाव्य ‘अनारी नर’ भी लिख डाला। अपने व्यंग्य-विनोदी स्तंभों की एक-साथ छह पुस्तकें भी इसी बीच संकलित करके प्रकाशित करा दीं। जैसे महाकवि सूरदास ने महाप्रभु वल्लभाचार्य की प्रेरणा से ब्रज में गोवर्धन पर्वत पर अपनी देखरेख में श्रीनाथजी का मंदिर बनवाकर खड़ा कर दिया था, उसी प्रकार मैंने सूरदासजी की निर्वाणस्थली और अपनी जन्मस्थली परासौली (परम रासस्थली) में एक सारस्वत पीठ और मां शारदा का मंदिर बनवा दिया तथा उनके कर-कमलों में महारासस्थली की कल्पना के अनुसार वीणा के स्थान पर वेणु थमा दी। ये सब हास्यरस की कृपा के फल हैं। मैंने जीवन में से मस्ती को नहीं जाने दिया। उस अहं को भी विकसित करता रहा जो कृतिकार के सृजन को प्रेरित करता है और प्रतिपक्षी की उपेक्षा के प्रति सक्षम होता है। ऐसा वही कर सकता है, जिसके अंदर आनंद का सागर लहराता हो और जिसके मन-मानस में उत्साह के कमल खिलते रहते हों। ये आनंदीवृत्ति और अटूट उत्साह मुझे हास्यरस की अनुकंपा से ही प्राप्त हुए हैं। जब भाई स्व0 प्रफुल्लचंद्र ओझा ‘मुक्त’ मुझे आनंदमूर्ति कहकर संबोधित करते थे तो छिपाऊंगा नहीं, बहुत अच्छा लगता था। सबसे पहले यह आनंदमूर्ति का अलंकरण मुझे आदरणीया बहन महादेवी वर्मा ने दिया था। मैं चाहता हूं और ईश्वर से प्रार्थना भी करता हूं कि वास्तव में आनंदमूर्ति बनने की क्षमता मुझमें आ जाए। आनंद ही जीवन का परम इष्ट है। वही चिदानंद है, नित्यानंद है और सच्चिदानंद है। मुक्ति-पथ क्या है ? परमानंद की डगर ही तो है ! इस आनंद से ही मनुष्य कर्म-विपाक से छूटता है। इस आनंद से ही जगत की माया उसे नहीं व्यापती। वह इसी आनंद से सच्चिदानंद की शाश्वत शरण में पहुंच जाता है। हास्यरस इस आनंद तक पहुंचने का सबसे सुगम मार्ग है।
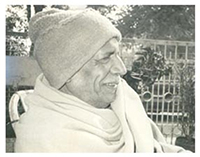 किसी और की नहीं जानता, कम से कम मैंने तो हास्यरस को इसी रूप में वरण किया है। लिखते-लिखते अपने कुल-धर्म के अनुसार मैंने ‘रास रसामृत’ नामक एक काव्य-संगीतात्मक पुस्तक भी लिखी है, जो केवल श्रीकृष्ण की लीला तक ही सीमित नहीं है, पाठक को उनके कर्मयोग ‘गीता-ज्ञान’ तक ले जाती है।
किसी और की नहीं जानता, कम से कम मैंने तो हास्यरस को इसी रूप में वरण किया है। लिखते-लिखते अपने कुल-धर्म के अनुसार मैंने ‘रास रसामृत’ नामक एक काव्य-संगीतात्मक पुस्तक भी लिखी है, जो केवल श्रीकृष्ण की लीला तक ही सीमित नहीं है, पाठक को उनके कर्मयोग ‘गीता-ज्ञान’ तक ले जाती है।
अपनी मधुमेही शारीरिक अक्षमता को ललकारते हुए मैंने अपनी आत्मकथा भी लिख डाली- ‘कहो व्यास, कैसी कटी ?’
हास्यरस का दूसरा नाम है- मन की उमंग। जब यह उमंग विकारी होती है तो रति से जुड़ती है, ओज को उत्साहित करती है तथा उसके मार्ग में बाधा उत्पन्न होने पर आक्रोश को जन्म देती है। यानी, व्यंग्य बन जाती है। जब यह उमंग शुद्ध और अविकारी होती है तो उल्लास का रूप धारण कर लेती है, या कहूं कि निर्मल हास्य बन जाती है। जब आत्मानंद की ऊर्जा मुख-मंडल को आभायित करती है तो व्यक्तित्व की रेखाएं ऊपर उठने लगती हैं। जब यह ऊर्जा या उमंग मंद पड़ जाती है तो मुख पर उदासी की रेखाएं नीचे को लटकने लगती है, यानि झुर्रियां पड़ जाती हैं। किसी व्यक्ति के रेखाचित्र अथवा कार्टून से इन उतार-चढ़ावों का रहस्य समझा जा सकता है। वैसे भी जब आदमी प्रसन्न होता है और उसका रोम-रोम अपने को उल्लसित अनुभव करता है तो उसका वक्ष तन जाता है, लटकता हुआ मुंह ऊपर उठ जाता है, अधरों पर मुस्कान खेलने लगती है। हंसने से फेफड़ों में बल आता है और मनुष्य के शरीर में नवीन रक्त का संचार होने से वह पुष्ट और गदगद हो जाता है। लेकिन मनहूसियत में ऐसा नहीं होता। तब आदमी सामने नहीं, नीचे की ओर देखता है। उसका मुंह लटक जाता है और वक्ष सिकुड़ जाता है। कहना यह चाहता हूं कि हास्य उर्ध्वगामी है, जबकि अन्य रसों के बारे में ऐसी बात पूरे विश्वास के साथ नहीं कही जा सकती। श्रृंगार का संबंध वयः विशेष तक ही सीमित है। निर्विकार, भले और भोले बच्चों पर उसका वैसा असर नहीं होता। तन से क्षीण और मन से विरक्त या तन-मन दोनों से टूटे हुए प्रौढ़ों और वृद्धों में तो इसके प्रति नफरत तक देखी जा सकती है। लेकिन रसराज हास्य वय के सभी सोपानों पर अपना रंग चढ़ाने में प्रभावी है। वह बच्चों की किलक, युवक-युवतियों की मुस्कान है, प्रौढ़ों का ठहाका है और सज्जनेतर व्यक्तियों के हृदय में वह अट्टहास के रूप में प्रकट होता है।
 जी, मैंने अनुभव किया है और जीव तथा पदार्थ-विज्ञानी भी यह सिद्ध कर चुके हैं कि पेड़-पौधे भी प्रसन्नता से झूमने लगते हैं। छोटी-छोटी चिड़ियां और जमीन पर रेंगनेवाले जीव भी कभी-कभी चुहल और अठखेली करते देखे गए हैं। गाय, कुत्ता, बिल्ली और खरगोश पर आप प्यार से हाथ फेरिए और उनकी आंखों में झांकिए तो आपको खुशियां नाचती नजर आएंगी। हां, हास्यरस का प्रभाव हिंसक किस्म के जीवों पर उतना नहीं होता। लेकिन जब वे इच्छित शिकार मार लेते हैं और उनका पेट भरा होता है तब वे भी केवल अपनी मादाओं को ही नहीं, अपने आसपास के वातावरण को और जहां तक दृष्टि जाती है, प्रकृति के वैभव को ऐसे मुग्धभाव से देखते हैं जैसे उनके पास भी खुशियों के खजाने की कमी नहीं। हास्यरस का क्षेत्र असीमित है। मुझे तो विधाता की यह चराचर सृष्टि ही हास्य की रंगस्थली लगती है। ये मुस्कराती हुई कलियां, खिलते हुए फूल, लहराती हुई लताएं, झूमती हुई वृक्षों की शाखाएं, उन पर पक्षियों का मधुर कलरव, मोद-विनोद के उत्सव ही तो हैं। खारे समुद्र में मोतियों का जन्म, पाषाण-पर्वतों से कल-कल, छल-छल बहती हुई नदियां और झरने, उनके शिखरों पर हिममंडित रजत मुकुट, मेरे लिए तो प्रकृति की प्रसन्नता के ही द्योतक हैं। सुबह-सुबह प्राची में हौले-हौले उषा-सुंदरी का आगमन, थिरक-थिरककर आकाश से उतरती हुई ये सूर्य की स्वर्ण-रश्मियां, सुखद समीरण के साथ सहमी आती और जाती संध्या, ये झिलमिल करते तारे, ये भुवनमोहिनी चांदनी और चन्द्रहास क्या हैं ? जगती-तल में व्यापक, उदात्त और आनंदमय हास्यरस की विराट अभिव्यक्ति ही है न ! कम-से-कम मुझे तो जगत के कण-कण में व्याप्त इस हास्य में दिव्य सत्ता की आनंदमयी झांकी ही परिलक्षित होती है।
जी, मैंने अनुभव किया है और जीव तथा पदार्थ-विज्ञानी भी यह सिद्ध कर चुके हैं कि पेड़-पौधे भी प्रसन्नता से झूमने लगते हैं। छोटी-छोटी चिड़ियां और जमीन पर रेंगनेवाले जीव भी कभी-कभी चुहल और अठखेली करते देखे गए हैं। गाय, कुत्ता, बिल्ली और खरगोश पर आप प्यार से हाथ फेरिए और उनकी आंखों में झांकिए तो आपको खुशियां नाचती नजर आएंगी। हां, हास्यरस का प्रभाव हिंसक किस्म के जीवों पर उतना नहीं होता। लेकिन जब वे इच्छित शिकार मार लेते हैं और उनका पेट भरा होता है तब वे भी केवल अपनी मादाओं को ही नहीं, अपने आसपास के वातावरण को और जहां तक दृष्टि जाती है, प्रकृति के वैभव को ऐसे मुग्धभाव से देखते हैं जैसे उनके पास भी खुशियों के खजाने की कमी नहीं। हास्यरस का क्षेत्र असीमित है। मुझे तो विधाता की यह चराचर सृष्टि ही हास्य की रंगस्थली लगती है। ये मुस्कराती हुई कलियां, खिलते हुए फूल, लहराती हुई लताएं, झूमती हुई वृक्षों की शाखाएं, उन पर पक्षियों का मधुर कलरव, मोद-विनोद के उत्सव ही तो हैं। खारे समुद्र में मोतियों का जन्म, पाषाण-पर्वतों से कल-कल, छल-छल बहती हुई नदियां और झरने, उनके शिखरों पर हिममंडित रजत मुकुट, मेरे लिए तो प्रकृति की प्रसन्नता के ही द्योतक हैं। सुबह-सुबह प्राची में हौले-हौले उषा-सुंदरी का आगमन, थिरक-थिरककर आकाश से उतरती हुई ये सूर्य की स्वर्ण-रश्मियां, सुखद समीरण के साथ सहमी आती और जाती संध्या, ये झिलमिल करते तारे, ये भुवनमोहिनी चांदनी और चन्द्रहास क्या हैं ? जगती-तल में व्यापक, उदात्त और आनंदमय हास्यरस की विराट अभिव्यक्ति ही है न ! कम-से-कम मुझे तो जगत के कण-कण में व्याप्त इस हास्य में दिव्य सत्ता की आनंदमयी झांकी ही परिलक्षित होती है।
लेकिन इस हास्य को अनुभव करना, इसके प्रसाद से आनंदित होना, जितना आसान है, उसे कलम से उतारना उतना ही कठिन है। ईश्वरीय सत्ता अनुभव की जा सकती है, लेकिन उसकी सही-सही व्याख्या तो नहीं की जा सकती। जैसे ईश्वर के संबंध में ‘नेति-नेति’ का सहारा लिया गया है, वैसे ही हास्यरस की व्याख्या तो नहीं की जा सकती, लेकिन यह अवश्य बताया जा सकता है कि यह हास्य नहीं है, वह हास्य नहीं है। जैसे काले को कुरूप कहना, अपने विचारों से साम्य न रखने वाले को मंदबुद्धि कहना अथवा किसी के पतन पर प्रसन्न होने को हास्यरस नहीं का जा सकता। आप पैंट पहनते हैं तो मैं आपको पैंटागन कहूं और मैं धोती पहनता हूं तो आप मुझे धोतीप्रसाद कहें, यह तो हास्य नहीं हुआ। आपका पेट पीठ से लगा हुआ है और मेरा पेट शारीरिक विकार के कारण आगे बढ़ गया है, तो इसमें हास्य की क्या बात है ?
अगर कोई लगातार कोशिश करने के बाद भी सत्ता के शिखर तक नहीं पहुंच पाता तो यह करुणा का विषय है, हास्य का नहीं। बच्चे नहीं सुनते तो बुढ़िया टर्राती रहती है, बूढ़ा खांसता रहता है या बर्राता रहता है तो उसकी सेवा-सहायता कीजिए। उसे हास्यरस का आलंबन क्यों बनाते हैं ? इसी प्रकार असफल प्रेमी, उदास पति और निराश पत्नियों को हास-परिहास के दायरे में लाना उचित नहीं है। ये सब आपकी मानवीय संवेदना के अधिकारी है, परिहास के पात्र नहीं। हास्यरस तो व्यक्ति और समाज की असंबद्धताओं, विसंगतियों, अनाचार, पाखंड, मद और मत्सर जैसी तमसावृत वृत्तियों और घटनाओं के लिए ज्योतिर्मय अंजन है। उसका प्रयोग समाज के हित और परिष्कार के लिए कीजिए। व्यक्ति के सुधार के लिए उसे आजमाइए। यह प्रसन्नता बिखेरने वाली विधा है। इसमें कल्मष और कटुता को मिलाकर इसे अपवित्र, गंदला और प्रदूषित मत बनाइए। हास्यरस समाज के लिए संजीवनी है और व्यक्ति के लिए जिंदादिली। इसीलिए एक लोकगायक हंसते-हंसाते बड़ी ऊंची बात कह गया है –
“हंस-बोल बखत कटि जायगौ,
जानैं को कितकूं रम जायगौ ?”
 और व्यंग्य ? वही तो हास्य का वास्तविक रंग है। जैसे मोती में आब, पुष्प में पराग और तरुणियों की बड़ी-बड़ी अंखियों में चितवन का महत्त्व होता है, वैसे ही हास्य में व्यंग्य का महत्त्व है। जैसे नृत्य में तोड़, ताल, सम, संगीत में लयकारी का अपना एक अलग आनंद है, वैसे ही हास्यरस में व्यंग्य का अपना अलग मज़ा है। ये जो काव्यशास्त्र के श्लेष, अन्योक्ति, वक्रोक्ति आदि उक्तिवैचित्र्य हैं, वे व्यंग्य की परख के लिए ही स्थापित हुए हैं। रीति-साहित्य की लक्षणा और व्यंजना तथा विद्वज्जनों की जो वचन-विदग्धता है, वे चुटीले व्यंग्य के ही सरस उपादान हैं। जैसे गुलाब के पास कांटा, मयूर के पास पैनी चोंच और असुंदरियों के पास तीखे बोल होते हैं, वैसे ही हास्य के पास उसे धार देने के लिए सृष्टा ने व्यंग्य की व्यवस्था कर दी है। व्यंग्य न हो तो हास्य सपाट-बयानी बन जाए, अनर्गल हो जाए और बेतुका लगने लगे। चतुर्भुज विष्णु के हाथ में केवल नीलकमल ही नहीं, शंख, चक्र, गदा और शंख भी हैं। इसी प्रकार चक्रवर्ती हास्य के पास चोज़, आयरनी, तंज़ और व्यंग्य के आयुध रहते हैं। पर भयावह रूप में नहीं, दिव्य रूप में अत्यंत शोभायमान।
और व्यंग्य ? वही तो हास्य का वास्तविक रंग है। जैसे मोती में आब, पुष्प में पराग और तरुणियों की बड़ी-बड़ी अंखियों में चितवन का महत्त्व होता है, वैसे ही हास्य में व्यंग्य का महत्त्व है। जैसे नृत्य में तोड़, ताल, सम, संगीत में लयकारी का अपना एक अलग आनंद है, वैसे ही हास्यरस में व्यंग्य का अपना अलग मज़ा है। ये जो काव्यशास्त्र के श्लेष, अन्योक्ति, वक्रोक्ति आदि उक्तिवैचित्र्य हैं, वे व्यंग्य की परख के लिए ही स्थापित हुए हैं। रीति-साहित्य की लक्षणा और व्यंजना तथा विद्वज्जनों की जो वचन-विदग्धता है, वे चुटीले व्यंग्य के ही सरस उपादान हैं। जैसे गुलाब के पास कांटा, मयूर के पास पैनी चोंच और असुंदरियों के पास तीखे बोल होते हैं, वैसे ही हास्य के पास उसे धार देने के लिए सृष्टा ने व्यंग्य की व्यवस्था कर दी है। व्यंग्य न हो तो हास्य सपाट-बयानी बन जाए, अनर्गल हो जाए और बेतुका लगने लगे। चतुर्भुज विष्णु के हाथ में केवल नीलकमल ही नहीं, शंख, चक्र, गदा और शंख भी हैं। इसी प्रकार चक्रवर्ती हास्य के पास चोज़, आयरनी, तंज़ और व्यंग्य के आयुध रहते हैं। पर भयावह रूप में नहीं, दिव्य रूप में अत्यंत शोभायमान।
अलग करके देखें तो हास्य मधुर और व्यंग्य थोड़ा कषाय। दिल्ली की चसकदार कॉफी की तरह कि जिसमें दूध भी है, क्रीम भी है, चीनी भी है और सुस्वादु चाकलेट पाउडर भी। इसके अलावा जो व्यंग्य है, उसका ढंग मुझे स्वीकार नहीं। वह या तो गाली-गलौज होता है या फिर उसका काम टांग खींचना या पगड़ी उछालना बन जाता है। साहित्य का मूल गुण शिष्टता या शालीनता है। उसका एकमात्र लक्ष्य मानवीय संवेदना की सरस अभिव्यक्ति है। लेकिन जैसे व्यंग्य का आज साहित्य में प्रचलन हो चला है, उसमें शील और सौजन्य, संवेदना और मानवता के दर्शन प्रायः कम ही होते हैं। वह समाज की संरचना में कम, उसकी विकृतियों के बहाने उसके विनाश की ओर अधिक उन्मुख दिखाई देता है। यह पश्चिमी के भौतिकवाद और उससे उत्पन्न असंतोष तथा विकृतियों की ही देन है। इसका हृदय-परिवर्तन में विश्वास नहीं। यह पुरातत्त्व के खंडहरों की मरम्मत करके उसे खड़ा रखना नहीं चाहता। विनाश के इस मसान पर सपनों के राजमहल खड़ा करके ही दम लेना चाहता है। गलत क्यों कहें, सामाजिक क्रांति का यह भी एक तरीका है। इसने कई जगह अभूतपूर्व सफलता भी प्राप्त की है। परंतु भारतीय संस्कृति और पुराने साहित्यिक एवं सामाजिक संस्कारों में पले मुझ-जैसे लोगों को आज यह रास नहीं आ रहा है। कल की कल जाने !
लीजिए, ऊपर मैंने बड़े-बड़े सिद्धांत बघार दिए। पर सिद्धांतों का बखान करना जितना आसान है, उन पर अमल करना उतना आसान नहीं। मैंने इन पर कितना अमल किया है और इसमें कितना सफल रहा हूं, यह बात न मैं जानता हूं और न कहूंगा। मेरे न रहने पर मेरा कितना साहित्य छनकर बचता है और समाज के पाठक और साहित्य के समीक्षक उसे किस रूप में स्वीकार करते हैं, यह वे जानें और उनका काम जानें। मैं तो इतना जानता हूं कि हास्यरस की पतवार लेकर मैं जीवन-नैया में सवार हुआ और हंसते-गाते उसे खूब खेया। पत्नीवाद चला या नहीं चला, चला तो कहां से कहां पहुंचा ? लेकिन उसके बहाने मैंने देश को लूटने वालों, सताने वालों और इस पर कब्जा बनाए रखने वालों की खूब खबर ली। लगे हाथ सामाजिक विषमताओं और अन्यायों की बात भी कहता गया। साहित्य में मैंने नई जमीन तोड़ी या नहीं, इसका पता तो ठीक से वे बताएंगे जिनकी भूमि पर मेरे हल चले हैं।
लेकिन इतना अवश्य बता सकता हूं कि मैंने किसी की नकल नहीं की। न किसी से उधार लिया और न किसी की जूठन खाई। जो सूझा, जो महसूसा, उसे निर्भीकता से कहा और परिणाम झेले। जनता से बहुत प्रेम पाया। भगवान ने जैसी मेरी सुनी, वैसी सबकी सुने। व्यंग्य-विनोद के लिखने वाले सुखी रहें और सबको सुख देते रहें। कृपया वह मेरी यह बात गांठ बांध लें कि यह दुनिया नाना प्रकार के दारुण दुःखों से पीड़ित है। सुखी से सुखी, समृद्ध से समृद्ध और शक्तिशाली से शक्तिशाली व्यक्ति के जीवन में कहीं-न-कहीं, कोई-न-कोई ऐसा डंक लगा है, जिससे वह मन ही मन विह्वल है, उदास है और ग़मगीन है। यदि उसके मुख पर एक क्षण के लिए भी हल्की-सी हंसी उभार सकते हों तो इससे बड़ा पुण्य कार्य कोई और नहीं। मैंने एक छोटा-सा ‘हास्य-गीतम्’ लिखा है। इसे पढ़ें और गुनें-
(‘हास्य सागर’ से, सन् 1996)