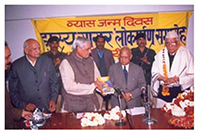 भारत सहित विश्व की सभी भाषाओं के विद्वानों, आलोचकों, हास्यरस की विवेचना करने वालों, उसके लक्षण और उदाहरण प्रस्तुत करने वालों ने इस रसराज हास्य की बहुविध और उदात्त स्वरों में मार्मिक व्याख्या की है। इन सबके अनुशीलन को मैं देख-सुन आया हूं और इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि हास्यरस चाहे जन्मजात या आनुवंशिक उतना न हो, जितना वह रचयिता के संस्कारों और परिस्थितिजन्य कारणों से उदभासित होता है।
भारत सहित विश्व की सभी भाषाओं के विद्वानों, आलोचकों, हास्यरस की विवेचना करने वालों, उसके लक्षण और उदाहरण प्रस्तुत करने वालों ने इस रसराज हास्य की बहुविध और उदात्त स्वरों में मार्मिक व्याख्या की है। इन सबके अनुशीलन को मैं देख-सुन आया हूं और इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि हास्यरस चाहे जन्मजात या आनुवंशिक उतना न हो, जितना वह रचयिता के संस्कारों और परिस्थितिजन्य कारणों से उदभासित होता है।
 हास्यरस करुणा से उत्पन्न होता है और उसका मुख्य लक्ष्य अनीति को उदघाटित करना है। यह भी एक व्यंग्य है कि साहित्य में दोष-दर्शन करनेवालों ने यह स्वीकार किया है कि विधाता की सृष्टि में जहां दोष और असंबद्धताएं पाई जाती हैं, वे सब हास्य के विभाव हैं।
हास्यरस करुणा से उत्पन्न होता है और उसका मुख्य लक्ष्य अनीति को उदघाटित करना है। यह भी एक व्यंग्य है कि साहित्य में दोष-दर्शन करनेवालों ने यह स्वीकार किया है कि विधाता की सृष्टि में जहां दोष और असंबद्धताएं पाई जाती हैं, वे सब हास्य के विभाव हैं।
मुझे यह कहने में कोई हिचक नहीं कि संस्कृत से लेकर विश्व की विशिष्ट भाषाओं में हास्यरस की महत्ता को तो स्वीकार किया गया है, उसके भेद और उपभेद भी बड़ी सूक्ष्मता से बताए गए हैं, लेकिन हास्य अधिकतर लक्षण-ग्रंथों तक ही सीमित रहा है। उसमें उत्कृष्ट साहित्य की रचना नहीं पाई जाती। संस्कृत में वेदों की वचन-विदग्धता से लेकर भरत के नाट्यशास्त्र और संस्कृत के साहित्य-शास्त्र संबंधी ‘साहित्य दर्पण’ आदि में यही सब कुछ देखने को मिलता है। लेकिन एक बात स्वीकार करनी पड़ेगी कि इन साहित्य-शास्त्रियों और व्यंग्य-विनोद के विवेचकों ने अवश्य ही लेखकों का पथ-प्रदर्शन किया है।
 महान दार्शनिक अरस्तू ने विनोद-वचन को काव्यशास्त्र के अंतर्गत नहीं, वक्तृत्व-शास्त्र में अलंकारशास्त्र के अंतर्गत माना है। उसने विनोद का समावेश वाइवासिटी अर्थात भाषा की प्रफुल्लता या तेजस्विता में किया है और चटकीले शब्द-प्रबंध के लक्षणों में हास्य का उल्लेख स्पष्ट रूप से किया है।
महान दार्शनिक अरस्तू ने विनोद-वचन को काव्यशास्त्र के अंतर्गत नहीं, वक्तृत्व-शास्त्र में अलंकारशास्त्र के अंतर्गत माना है। उसने विनोद का समावेश वाइवासिटी अर्थात भाषा की प्रफुल्लता या तेजस्विता में किया है और चटकीले शब्द-प्रबंध के लक्षणों में हास्य का उल्लेख स्पष्ट रूप से किया है।
अरस्तू का मत है कि जिन ”चटकीले शब्द प्रबंधों’ की लोग बहुत प्रशंसा करते हैं, वे अनुनयी और चतुर मनुष्यों द्वारा रचे हुए होते हैं।” ‘चमत्कृतिजनक रूपक’ नाम का एक विशिष्ट प्रकार अरस्तू को बहुत पसंद था, जिसका वर्णन उसने इस प्रकार किया है- ”ऐसा आनंददायक समय ढूंढ निकालना जो पहले कभी न देखा गया हो।” ऐसे चमत्कारिक और आनंददायक शब्द-प्रयोग से हास्यरस की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार कह सकते हैं कि अरस्तू द्वारा बताया गया ‘चमत्कृतिजनक रूपक’ निःसंदेह हिन्दी के ‘चोज़’ और अंग्रेजी के ‘विट’ की ही प्रतिकृति है।
 अंग्रेजी ग्रंथकार एडीसन ने ‘सिक्स पेपर्स ऑनविट’ नामक लेखमाला में ‘उक्ति चमत्कार’ को प्रधान विषय बनाते हुए चोज़ (विट) और विनोद या परिहास (ह्यूमर) का अलग-अलग विवेचन नहीं किया है। फिर भी उसका मत है कि ये दोनों एक दूसरे से भिन्न होकर भी परस्पर विशिष्ट संबंध रखते हैं और प्रायः एक दूसरे पर अवलंबित रहते हैं। अपने ह्यूमर नामक लेख में एडीसन ने चोज़ और विनोद के संबंध में एक दिलचस्प और सटीक वंशावली का उल्लेख किया है जो इस प्रकार है- ”परिहास या विनोद के श्रेष्ठ घराने का मूल पुरुष ‘सत्य’ है। ‘सत्य’ के शोभनार्थ नामक पुत्र हुआ। ‘शोभनार्थ’ के यहां उक्ति-चमत्कार नामक बेटा हुआ। ‘उक्ति-चमत्कार’ ने अपने वंश की ‘आनंदी’ नामक लड़की से विवाह किया। इस दम्पति के यहां ‘विनोद’ नामक पुत्ररत्न हुआ। ‘विनोद’ का जन्म भिन्न-भिन्न स्वभाव वाले माता-पिता से हुआ था, इसलिए उसका स्वभाव भी विलक्षण होगया। कभी वह देखने में गंभीर, कभी चंचल और कभी विलासी मालूम पड़ता था। लेकिन उसमें विशेषतः अपनी माता (आनंदी) के स्वभाव का ही अंश अधिक आया। इसीलिए वह स्वयं चाहे जिस चित्तवृत्ति में रहता हो, दूसरों को उल्लसित किए बिना नहीं रहता।”
अंग्रेजी ग्रंथकार एडीसन ने ‘सिक्स पेपर्स ऑनविट’ नामक लेखमाला में ‘उक्ति चमत्कार’ को प्रधान विषय बनाते हुए चोज़ (विट) और विनोद या परिहास (ह्यूमर) का अलग-अलग विवेचन नहीं किया है। फिर भी उसका मत है कि ये दोनों एक दूसरे से भिन्न होकर भी परस्पर विशिष्ट संबंध रखते हैं और प्रायः एक दूसरे पर अवलंबित रहते हैं। अपने ह्यूमर नामक लेख में एडीसन ने चोज़ और विनोद के संबंध में एक दिलचस्प और सटीक वंशावली का उल्लेख किया है जो इस प्रकार है- ”परिहास या विनोद के श्रेष्ठ घराने का मूल पुरुष ‘सत्य’ है। ‘सत्य’ के शोभनार्थ नामक पुत्र हुआ। ‘शोभनार्थ’ के यहां उक्ति-चमत्कार नामक बेटा हुआ। ‘उक्ति-चमत्कार’ ने अपने वंश की ‘आनंदी’ नामक लड़की से विवाह किया। इस दम्पति के यहां ‘विनोद’ नामक पुत्ररत्न हुआ। ‘विनोद’ का जन्म भिन्न-भिन्न स्वभाव वाले माता-पिता से हुआ था, इसलिए उसका स्वभाव भी विलक्षण होगया। कभी वह देखने में गंभीर, कभी चंचल और कभी विलासी मालूम पड़ता था। लेकिन उसमें विशेषतः अपनी माता (आनंदी) के स्वभाव का ही अंश अधिक आया। इसीलिए वह स्वयं चाहे जिस चित्तवृत्ति में रहता हो, दूसरों को उल्लसित किए बिना नहीं रहता।”
 बद्ध पदार्थों की सुसंबद्धता दिखाई देती है। ले हंट और एडीसन दोनों का यह मानना है कि चोज़ और विनोद (विट और ह्यूमर) दोनों ही स्वभावतः भिन्न लक्षणात्मक हैं, परंतु दोनों का संयोग या मिलाप दूध-चीनी की तरह होता है। चोज़ का विषय ‘पदार्थों की असंबद्धता है’ तो विनोद का विषय ‘मानवीय स्वभाव और परिस्थिति संबंधी असंबद्धता’ है।
बद्ध पदार्थों की सुसंबद्धता दिखाई देती है। ले हंट और एडीसन दोनों का यह मानना है कि चोज़ और विनोद (विट और ह्यूमर) दोनों ही स्वभावतः भिन्न लक्षणात्मक हैं, परंतु दोनों का संयोग या मिलाप दूध-चीनी की तरह होता है। चोज़ का विषय ‘पदार्थों की असंबद्धता है’ तो विनोद का विषय ‘मानवीय स्वभाव और परिस्थिति संबंधी असंबद्धता’ है।
एक और भाषा विषयक टीकाकार विलियम हेजलिट ने भी चोज़ और विनोद (विट और ह्यूमर) के भेद पर विचार करते हुए कहा है- ”चोज़ और विनोद दोनों के विषय हास्यमूलक होते हैं।
लेकिन विनोद (ह्यूमर) में हास्यमूलक विषय का वर्णन स्वभावोक्ति से किया जाता है और चोज़ (विट) में वह वर्णन कुछ वक्रोक्ति से किया जाता है। विनोद में जो चमत्कार होता है वह स्वाभाविक होता है, परंतु चोज़ के लिए एक प्रकार की सुसंस्कृत कल्पनाशक्ति और कला-ज्ञान की ज़रूरत होती है।”
 इंग्लैंड के सुप्रसिद्ध चोज़-सिद्ध सिडनी स्मिथ का चोज के बारे में कहना है कि ‘चोज़’ में जब तक चमत्कार या विलक्षणता न हो, तब तक काम नहीं चल सकता, उसे चोज़ नहीं कह सकते। चोज में बुद्धिमत्ता का उपयोग पदार्थों के सुंदर या उपयुक्त संबंध ढूंढ निकालने के लिए नहीं, बल्कि वह संबंध ढूंढ निकालने के लिए होना चाहिए जो अनपेक्षित, अदभुत और चमत्कारजनक हो।
इंग्लैंड के सुप्रसिद्ध चोज़-सिद्ध सिडनी स्मिथ का चोज के बारे में कहना है कि ‘चोज़’ में जब तक चमत्कार या विलक्षणता न हो, तब तक काम नहीं चल सकता, उसे चोज़ नहीं कह सकते। चोज में बुद्धिमत्ता का उपयोग पदार्थों के सुंदर या उपयुक्त संबंध ढूंढ निकालने के लिए नहीं, बल्कि वह संबंध ढूंढ निकालने के लिए होना चाहिए जो अनपेक्षित, अदभुत और चमत्कारजनक हो।
अंग्रेजी साहित्य में विट और ह्यूमर के विषय में विशद और बहुविध व्याख्या की गई है और इनके लिए विविध शब्दों का प्रयोग किया गया है। लेकिन हमारे संस्कृत-साहित्य में विट के लिए सुभाषित, सुप्रलाप, सुवचन (देखो अमरकोश) सुनृत, सूक्ति, चतुरालाप, विनोद-वचन आदि शब्द मिलते हैं। इसके लिए ठेठ हिन्दी का शब्द चोज़ ही रखा जा सकता है। अंग्रेजी में विट और ह्यूमर दोनों अलग-अलग शब्द हैं। कोई एक ऐसा शब्द अंग्रेजी में नहीं है जिसके अंतर्गत इन दोनों शब्दों के भाव आ जाएं। लेकिन हमारी संस्कृत भाषा में विनोद के अंतर्गत विट और ह्यूमर दोनों का भाव समाविष्ट है।
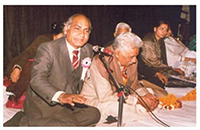 संस्कृत भाषा में काव्य के तीन भेद माने गए हैं- उत्तम, मध्यम और अधम। उत्तम काव्य में व्यंग्यार्थ प्रधान होता है, मध्यम काव्य में व्यंग्यार्थ गौण होता है और अधम काव्य में केवल शब्दों का वाच्यार्थ चमत्कारपूर्ण होता है।
संस्कृत-साहित्यकारों ने हास्यरस के आलंबन विदूषक, मूर्ख मनुष्य और बहुरूपिया बताए हैं और हास्यरस का उपकारक रस यानी वह रस जिसके सम्मिलन से उसका उत्कर्ष होता है श्रृंगार रस माना है। हास्य का विरोधी रस भयावह वीभत्स बताया गया है।
संस्कृत भाषा में काव्य के तीन भेद माने गए हैं- उत्तम, मध्यम और अधम। उत्तम काव्य में व्यंग्यार्थ प्रधान होता है, मध्यम काव्य में व्यंग्यार्थ गौण होता है और अधम काव्य में केवल शब्दों का वाच्यार्थ चमत्कारपूर्ण होता है।
संस्कृत-साहित्यकारों ने हास्यरस के आलंबन विदूषक, मूर्ख मनुष्य और बहुरूपिया बताए हैं और हास्यरस का उपकारक रस यानी वह रस जिसके सम्मिलन से उसका उत्कर्ष होता है श्रृंगार रस माना है। हास्य का विरोधी रस भयावह वीभत्स बताया गया है।
संस्कृत भाषा के प्रसिद्ध ग्रंथ ‘साहित्य दर्पण’ में हास्यरस के उदाहरण के रूप में जो श्लोक दिए गए हैं उनमें से एक इस प्रकार है-
गुरोगिर्रः पंच दिनान्यधीत्य
वेदांतशास्त्राणि दिनत्रयं च ।
अमी समाघ्राय च तर्कवादान्
समागता कुक्कुटमिश्रपादा :॥
(अर्थात-यह देखिए, कुक्कुट मिश्र आए हैं। इन्होंने गुरु से कुल जमा पांच दिन शिक्षा पाई है। सारा वेदांतशास्त्र तीन दिन में पढ़ा है और तर्कशास्त्र तो फूल की तरह सूंघ डाला है।)
इसी प्रकार संस्कृत के ‘सुभाषित रत्न भाण्डागार’ में एक श्लोक आता है-
सामगानातिपूतं मे नोच्छिष्टमधरं कुरु ।
उत्कण्ठितासि चेद् भद्रे वामं कर्णं दशस्व मे॥
(अर्थात-एक अरसिक वैदिक ब्राह्मण किसी रमणी से कहता है- हे भद्रे ! मेरे ये ओंठ सामवेद का गान करते-करते बहुत पवित्र होगए हैं। इन्हें तुम व्यर्थ जूठे मत करो। यदि तुमसे किसी प्रकार रहा न जाता हो तो तुम मेरा बायां कान ही मुंह में लेकर चुभला लो।)
‘सुभाषित रत्न भाण्डागार’ का एक श्लोक और देखिए-
सदा वक्रः सदा क्रूरः सदा पूजामपेक्षते ।
कन्याराशिस्थितो नित्यं जामाता दशमो ग्रहः ॥
(अर्थात्- दामाद दसवां ग्रह है। वह सदा वक्र और क्रूर रहता है। सदा पूजा चाहता है और सदा ‘कन्या’ राशि पर स्थित रहता है।)
संस्कृत-साहित्य में इसी प्रकार के अनेक हास्य-संबंधी उदाहरण यत्र-तत्र खोज निकाले जा सकते हैं जो कालिदास के ‘मेघदूत’ में भी मिलेंगे। भारवि की अर्थवत्ता में भी पाए जा सकते हैं। ‘मृच्छकटिकम्’ नाटक में भी व्यंग्य-विनोद-संबंधी सामग्री मिलती है। परंतु संस्कृत के नाट्य साहित्य में व्यंग्य-विनोद के उदाहरण प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। हास्य के जितने भेद-प्रभेद हैं, इस प्रकार बताए गए हैं-
1. स्मित – स्मित हास में गालों पर कुछ सिकुड़न पड़ती है। आंखें कुछ विकसित होती हैं। नीचे का ओंठ कुछ फड़कने लगता है। दांत दिखाई नहीं देते। दृष्टि कुछ कटाक्षपूर्ण हो जाती है। यह श्रेष्ठ लोगों के योग्य है।
2. हसित – श्रेष्ठ लोगों के योग्य इस हसित हास में मुख, गाल और आंखें कुछ फूली सी दिखाई देती हैं। दांतों की पंक्तियां कुछ-कुछ नज़र आती हैं।
3. विहसित – मध्यम श्रेणी के लोगों के योग्य इस विहसित नाम की हास-क्रिया में शब्द सुनाई देते हैं। इसमें आंखें कुछ सिकुड़ जाती हैं।
4. उपहसित – इसमें नथुने फूल जाते हैं। सिर और कंधे सिकुड़ जाते हैं तथा दृष्टि कुछ वक्र हो जाती है। यह भी मध्यम श्रेणी के लोगों के योग्य होता है।
5. अपहसित -यह हास अधम कोटि का माना जाता है। इसमें हंसते-हंसते आंखों में पानी आ जाता है। सिर और कंधे स्पष्ट रूप में हिलने लगते हैं तथा हंसते-हंसते मनुष्य पेट पकड़ लेता है।
6. अतिहसित – इसे भी अधम कोटि का हास माना गया है। इसमें हास्य के सारे लक्षण और परिणाम बहुत ही स्पष्ट होते हैं। इसे अट्टहास भी कह सकते हैं।
संस्कृत-नाट्यशास्त्रों में हास्य की अभिनय योग्य दृष्टि को ‘हास्या’ कहते हैं। संस्कृत नाटकों में तो हास्य सोने में सुहागे के समान है। प्रायः सभी संस्कृत नाटककारों ने एक ऐसे मनोरंजक पात्र की कल्पना की है जिसकी परंपरा बाद के हिन्दी-नाटकों और लोक-लीलाओं में आज तक अक्षुण्ण रूप से विद्यमान है। इसे विदूषक कहते थे जो नायक का अत्यंत विश्वासपात्र सहयोगी और उसके दूषणों को भी अपने मीठे वचनों से परिष्कृत करने वाला तथा देखने में अज्ञ और वास्तव में विज्ञ हुआ करता था। वह हर संकट में नायक के साथ नहीं, आगे रहता था। उसकी पहुंच रनिवास तक थी। वह नायिकाओं और मित्रों के मनमुटाव को दूर करनेवाला होता था। वह भविष्य की चेतावनी देने वाला होता था और वर्तमान का मार्गदर्शक भी होता था। लेकिन विडंबना देखिए कि उसे पेटू, मूर्ख, नक्काल और अपने शब्दों से ही नहीं, करतबों से भी दर्शकों के समक्ष अटपटे काम करने वाला बताकर विदूषक शब्द को आज विकृत कर दिया गया है। उसे जब नाटकों में ही महत्वपूर्ण स्थान नहीं मिला तो साहित्य में क्या खाक मिलता ! उसे तो सिर्फ ‘भाण’ कहकर छोड़ दिया गया। उसने कुछ लिखा भी तो ‘भड़उआ’ कह दिया। आज के कविता-मंच पर जनता में हास्य की लहर फैलाने वाले और गंभीर कवियों के पैर उखाड़ने वाले हास्यकवियों को जोकर और चुटकुलेबाज बताकर साहित्य से बहिष्कृत कर दिया गया है, यानि जो जनता में लोकप्रिय है, उसे साहित्य से बहिष्कृत करने की ठान आज के तथाकथित कुसमालोचकों और कुबुद्धियों ने ठान ली है। इसमें हास्यरस के कवियों का भी दोष कम नहीं है। वे कमर्शियल होगए हैं।
बाजार में जो माल बिकता है, वही बनाते हैं। लेकिन प्राचीन हिन्दी-साहित्य में ऐसा नहीं था। तुलसीदासजी ने शिव-पार्वती विवाह, परशुराम-लक्ष्मण संवाद, अंगद-रावण संवाद तथा स्थान-स्थान पर जो व्यंग्य-विनोदपूर्ण चुटकियां ली हैं, वे हिन्दी साहित्य की निधि हैं। सूरदासजी यद्यपि विशुद्ध भक्तकवि थे- विनय, भक्ति और दासवृत्ति ही उनके अभीष्ट लेखकीय विषय थे, परंतु ब्रज की मस्ती भी उनके पदों में जहां-तहां बोल ही पड़ती है, जैसे- ‘श्याम पिबइया घी कौ’ अथवा ‘गजी फटी और पौ’। लेकिन रीतिकालीन ब्रज-साहित्य में हास्यरस में मौलिक लेखन नहीं हुआ। अधिकतर संस्कृत के हास्यपरक श्लोकों का भाषांतर हुआ है।, जैसे-
“विधि, हरि, हर बढ़ि इनते न केऊ,
तेऊ खाट पै न सोवैं खटमलन के डर ते।”
अथवा कंजूसों, मनहूसों, काने-कुरूपों पर ही भौंडे कवित्त लिखे गए हैं। परंतु कुछ कवियों ने यमक द्वारा, शब्द-श्लेष द्वारा कभी-कभी बड़े मौलिक छंद भी लिख डाले हैं, जैसे-
“चींटी न चाटत, मूसे न सूंघत,
बास तैं माछी न आवत नेरे।
आनि धरे जब तैं घर में,
तब तैं रहे हैजा परोसिन घेरे।
माटिहु में कछु स्वाद मिलै,
इन्हैं खाय कैं ढूंढत हर्र-बहेरे।
चौंकि पर्यो पितलोक में बाप,
सपूत के देखि सराध के पेरे।”
अथवा
“सूम सिरोमणि नागो लला
कन्हराय खुराय तुला पै चढ़ायौ।
चाउर की कनकी किनकी अरु,
उर्द की चुन्नी सैं पल्ला भरायौ।
बालक तोल में भारी भयौ
तब याकौ उपाय यही ठहरायौ।
मूंड मुड़ाय कैं, दस्त कराय कैं,
फस्त खुलाय कैं, पूरौ करायौ।”
सूम-शिरोमणि का एक उदाहरण और लीजिए। वह लक्ष्मी से कहता है-
” दाता-घर जाती तौ कदर ऐसी नायँ पाती,
मेरे घर आई तो बधाई बांट बावरी।
खाने-तहखाने दस खाने में छिपाय राखौं,
होउ न उदास मेरौ यही चित्त चाव री।
खाऊं न खवाऊं, मर जाऊं तौ सिखाय जाऊं,
नाती अरु पूतन कौं अपनौ सुभाव री !
दमड़ी हू न दैंय कबौं सपने में भिखारी कौं,
सूम कहैं लक्ष्मी तू बैठी गीत गाव री !”
ब्रजभाषा के रीतिकाल में कुलटा, कुलच्छिनी, कुरूपा और कलही नारियों की भी खासी खबर ली गई है। पद्माकर कवि कहते हैं- “सापने हू कियो अपराध, आपने हाथन सेज बिछाई। तऊ कुलटा कूं दया नहिं आई,” आदि। अथवा कुरूपा स्त्री का यह खाका देखिए-
“लोहे के जेहर, लोहे के तेहर,
लोहे के पायँ पयॅंजनि बाढ़ी।
नाक में कौड़ी औ कान में कौड़ी,
कौड़िन की गजरा गति गाढ़ी।
रूप में ऐसी लखाई पड़ै, मनों
नील के मांट में बोर कै काढ़ी।
ईंट लियैं बतरावै भतार सौं,
भामिनि भौन में भूत-सी ठाड़ी।”
उक्त छंदों में हास्य प्रच्छन्न रूप में ही मिलता है। लेकिन इन्हें शुद्ध हास्य की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। ऐसा ही एक कवित्त मुझे और याद आ रहा है जो लिखा तो गया है कामिनी नायिका की मनोदशा पर, लेकिन इसकी अंतिम पंक्तियां इसे हास्य में अनुपम रूप से परिवर्तित कर देती हैं-
“वा दिन ते निकस्यौ न बहोरि,
कि जा दिन आग दै अंदर पैठ्यौ।
पीर सहौं न कहौं तुम सौं कछु,
मन माखत मार मरोर उमैठ्यौ।
‘सरदार’ विचारत चारु कुटैठ्यौ
न कुच कंचुकि छेड़ो लला,
कुच-कंदर अंदर बंदर बैठ्यौ।”
उरोजों को बंदर की उपमा देने वाले सरदार कवि अकेले नहीं हैं। सूरदास के कन्हैया ने जैसे ही राधा के उरोजों पर हाथ रखा तो अचानक यशोदा को देखकर बोल उठे- ”यानैं मेरी गेंद चुराई।” ऐसे कौतुकी छंदों में लोग अश्लीलता के दर्शन कर सकते हैं। किंतु ऐसे रसिकों की भी कमी नहीं जो अश्लीलता के यथार्थ को स्वीकार करते हुए इनके पदांशों से उत्पन्न हास्य को ही अधिक महत्व देते हैं।
इसी प्रकार बाबू जगन्नाथदास ‘रत्नाकर’ से लेकर ग्वाल और नवनीत चतुर्वेदी के छंदों में भी व्यंग्य-विनोद की छटा यत्र-तत्र बिखरी हुई है। सेनापति के रूपकों में जो हास्य प्रस्फुटित हुआ है उससे सभी परिचित हैं- ” ‘सेनापति’ सबदन की रचना बिचारौ यामैं, दाता और सूम दोनों कीन्हें इकसार हैं।” आदि-आदि।
मराठी के प्रसिद्ध विद्वान और व्यंग्य-विनोद पर व्यापक रूप से विचार करने वाले स्व0 नृसिंह चिंतामणि केलकर ने इन्द्रियविज्ञान की दृष्टि से व्यंग्य-विनोद का क्या महत्व है और जीवन में उसकी क्या उपयोगिता है इस पर शोधपूर्ण निबंध लिखे हैं। श्री रामचंद्र वर्मा ने श्री केलकर की मौलिक कृति ‘सुभाषित आणि विनोद’ का ‘हास्यरस’ के नाम से हिन्दी में भाषांतर किया है। मैंने चालीस वर्ष पूर्व इस पुस्तक को पढ़ा था, काव्यशास्त्र के अध्ययन के रूप में। तब सोचा भी नहीं था कि मुझे कभी हास्य के शास्त्रीय स्वरूप से लेकर इसकी लोक-परंपराओं पर भी ऐसी भूमिका बांधनी पड़ेगी।
हां तो हास्यरस क्या है ? इस पर विचार करें। शास्त्रों में लिखा कि हास्य का रंग शुभ्र, यानी गोरा है। इसका देवता प्रमथ है। प्रमथ का अर्थ है देवाधिदेव महादेव, जिन्हें विष नहीं व्यापता। उनके शरीर पर सर्प रेंगते रहते हैं, परंतु वे प्रसन्नानन हैं। अपनी साधना में समाधिरत हैं। परंतु इस सुंदर योगिराज के मस्तक के एक कोने में कलानिधि भी विराजमान हैं। वह मंत्रदाता ही नहीं, तंत्र-कला में भी पारंगत हैं। रुद्रवीणा बजाते हैं। श्रृंगी-नाद करते हैं। डमरू डिमडिमाते हैं। नृत्य-कला के अधिष्ठाता हैं। स्वयं तांडव नृत्य करते हैं और पार्वती को लास्य नृत्य की शिक्षा देते हैं। कामदेव को अनंग बनाने वाले शिव के समान कौन ऐसा प्रेमी होगा जो अपनी मृत पत्नी सती की देह को लेकर पर्वतों को लांघता हुआ देश-देशांतर में उसके विरह में व्याकुल दौड़ता फिरा हो ! शिव योगियों के लिए विरागी, प्रेमियों के लिए अनुरागी, अशिव वेश होने पर भी ‘ श्रृंगार’ के प्रतीक, वीर रस की साक्षात प्रतिमूर्ति ‘रौद्र’ रूप धारण करके अपना तीसरा नेत्र खोलकर सृष्टि में प्रलय कर देने वाले, ऐसे महानतम कलाकार ही हास्यरस के देवता हो सकते हैं। स्वयं हरि इन्हें देखकर हंसे थे। इनकी बारात को देखकर वह ऐसे बोले कि तुलसीदासजी ने लिखा- ”हरि के बिंग वचन नहिं जाई।” हमारे पुराणों में जो शिव की कल्पना की गई है, वह हास्य के रूप में ही नहीं, व्यंग्य के रूप में भी उन्हें प्रतिष्ठित करने वाली है।
हास्य के संबंध में यह बात उल्लेखनीय है कि विद्वानों ने इसमें पुरुषत्व का आरोप किया है- ऐसा पुरुष जो अपने को श्रेष्ठ और दूसरों को निम्न, बुद्धिहीन अथवा मूर्ख समझता हो। यों भी साहित्य-सृजन अपने आपमें अहं से प्रेरित होता है। हास्यरस भी इसमें अपवाद नहीं है। उसके दो मुख्य भेद किए गए हैं- आत्मस्थ और परस्थ। आत्मस्थ रूप को हम ‘कला कला के लिए’ और परस्थ रूप को हम ‘कला जीवन के लिए’ रूप में स्वीकार करते हैं। जीवन यानी जन-जन। जन-जन का कल्याण, समाज की समुन्नति, उसके दोषों का परिष्कार, जनवाणी उसके हृदय का हार, जनाकांक्षा उसकी अभिव्यक्ति का विषय, पुरुषार्थ उसका संबल, जनोपकार ही उसके लिए सबसे बड़ा उपहार। जो अपने लिए ‘स्वातः सुखाय’ लिखता है, वह शुतुरमुर्ग है, जो अपने कल्याण के लिए अपनी गर्दन को रेत में दबाकर समाज में उठ रही क्रांति की आंधी से बचने की असफल चेष्टा करता है। परंतु कला को जीवनोपयोगी बनाने वाले को हम उस वटवृक्ष की तरह मानते हैं जो बवंडरों में भी अडिग खड़ा रहता है। सबको अपनी सुखद और शीतल छाया प्रदान करता है। हास्य मानस का राजहंस है, जो दूध का दूध और पानी का पानी करने में निपुण है। शिकारी या मांसाहारी नहीं है, चुन-चुनकर मोती लाता है और ‘हास्य-सागर’ में मंद-मंद विचरण करके जन-जन को नयनानंद और हर्षातिरेक से अभिभूत कर देता है। जैसे हंस को पक्षियों में सर्वोच्च स्थान प्राप्त है, वैसे ही सभी रसों में हास्यरस को प्रथम स्थान प्राप्त है। यदि नहीं है तो इस गलती को जल्दी से जल्दी सुधार लेना चाहिए। हम पहले भी बता चुके हैं कि श्रृंगार का महत्व सर्वाधिक युवाओं के लिए है, बच्चों और बूढ़ों के लिए नहीं। परंतु सभी अवस्थाओं में, सभी परिस्थितियों में हास्य सभी को ग्राह्य है। श्रृंगार काम उत्पन्न करता है, वीर विग्रह को जन्म देता है, रौद्र और वीभत्स से सभी डरते हैं तथा शांतरस का सुख तो विरलों को ही प्राप्त होता है। लेकिन हास्य, लोक से लेकर परलोक तक आनंदमय है। लोक में वह लेखक को यश व अर्थ प्रदान करने वाला और व्यवहार कुशल बनाने वाला है- यशसेऽर्थकृते व्यवहारविदे’ है। और यदि परलोक है और उसका सृष्टा परब्रह्म है तो हास्य का सच्चिदानंद ही उसे प्राप्त करने का सबसे सुगम मार्ग है।
संस्कृत में ‘विनोद’ शब्द का धात्वर्थ है- ‘भगा देने वाला’ अथवा ‘निकाल देने वाला’। शायद शब्द रचने वाले ने चिंता या दुःख को भगाने वाला और आनंद देने वाले वचन को ‘विनोद’ कहा है। इसी प्रकार अंग्रेजी में ‘ह्यूमर’ शब्द का अर्थ है-शरीर के अंतर्गत वह द्रव पदार्थ जिससे स्वभाव का निर्माण होता है। इससे स्पष्ट है कि संस्कृत के ‘विनोद’ और अंग्रेजी के ‘ह्यूमर’ दोनों का संबंध बुद्धि की अपेक्षा मनोभाव या स्वभाव से अधिक निकट का है। विनोदी मनुष्य की पहचान यह है कि उसका व्यक्तित्व आनंदी, शांत, हंसमुख तथा सहिष्णुता, विचारशीलता, सात्विकता, उदारता, ममता आदि गुणों से परिपूर्ण होता है। हमारे मत से हास्य मानव जाति का परम उपकारक है। समाज की सेवा ही उसका परम धर्म है। इसलिए ‘सेवाहि परमो धर्मः’ के स्थान पर मैं दोनों हाथ उठाकर कहना चाहता हूं -‘हास्याहि परमो धर्म’ (हास्य ही जीवन का परम धर्म है)। परोपकार की पराकाष्ठा और अपने दुःख-दर्द को भूलकर तथा लोक-व्यवहारजनित मन में आई उदासी को त्यागकर जो दूसरों को आनंद से अभिभूत करता है वही सच्चा मानव है और वही सच्चा हास्यकार है।
इस संबंध में कार्लेनी नामक हास्यकार की कथा ध्यान देने योग्य है। एक बार कार्लेनी एक चिकित्सक के पास गया। उसने चिकित्सक से कहा -“श्रीमान, मेरा मन बार-बार उदास हो जाता है।
मुझे कुछ नहीं सुहाता। कोई बात मेरे मन को अच्छी नहीं लगती। कृपा करके कोई ऐसी दवा दीजिए जिससे मेरी उदासी दूर हो। मेरे मन में प्रफुल्लता उत्पन्न हो।” चिकित्सक ने उससे कहा- ”भाई, तुम्हारे इस रोग की केवल एक ही दवा है कि तुम अकेले मत रहा करो। चार खुशमिजाज दोस्तों की मंडली में बैठकर अपना समय बिताया करो। और हां, आजकल कार्लेनी नाम का एक प्रसिद्ध मजाकिया शहर में आया हुआ है। तुम उसकी नकलें और मजाक देखो-सुनो तो तुम्हारी उदासी दूर होगी और मन प्रसन्न होगा।” कार्लेनी ने चिकित्सक से कहा- ”महोदय, मैं वही कार्लेनी हूं, जिसकी आप तारीफ कर रहे हैं। मैं सारी दुनिया को ठहाके लगवा सकता हूं, लेकिन मुझ जैसा दुःखी और उदास आदमी शायद ही कोई हो।”
मनुष्य इस जगत में जीवन से लेकर मरण तक दुःख-दर्दों से जूझने और अखंड उदासी को सहेजने के लिए बाध्य है। धन्य हैं वे लोग जो अपनी उदासी को दबाकर दूसरों को खिलखिलाने और आनंदविभोर करने को अपना परम कर्तव्य मानते हैं। यह स्वानुभव है। हमने एक स्थान पर लिखा है-
“रोगों को सहेजा है हमने
भोगों को नहीं परहेजा है।
ग़म बांटे नहीं, खुशियां बोईं
मुस्कान को सब तक भेजा है।”
कहने को तो बहुत-सी बातें हैं। स्पेंसर से लेकर पं. रामचंद्र शुक्ल तक ने उनका भांति-भांति से वर्णन किया है। परंतु जैसे “हरि अनंत हरि-कथा अनंता” वैसे ही हास्य के संबंध में, उसके परम सहचर व्यंग्य के संबंध में दुनिया की भाषाओं को छोड़िए, हिन्दी में कितनी कहानियां, कितने उपन्यास, कितने निबंध और कितनी कविताएं लिखी गई हैं, उनकी संख्या आकाश के तारों की तरह अनगिनत है। व्यंग्य-विनोद के स्वर हिन्दी कविता में भले ही मंद पड़ गए हों, परंतु साहित्य की अन्य विधाओं में यह खूब फल-फूल रहा है। पद्य के व्यंग्य-विनोद के बादल आज गद्य में बरसकर साहित्य को ”सुजलां सुफलां मलयज शीतलाम्” बना रहे हैं और राज-समाज, व्यवस्था, विसंगति, विषमता पर केवल यही विधा निर्भीक होकर प्रहार कर रही है। बाकी तो ”भज गोविंदम, दे पुरस्कारम्, ला अलंकारम् ।”
क्षमा कीजिए, मैं व्यंग्य को विनोद से अलग करके नहीं देखता। बिना व्यंग्य के विनोद ऐसा ही है जैसे बिना चीनी के दूध। विनोद में सरसता और सुस्वाद व्यंग्य की खंडसारी से ही आता है। फीका दूध कोई नहीं पीता। जन-रंजन-विहीन व्यंग्य को जनता नहीं पचा पाती। हास्य यदि दूध है तो व्यंग्य दही का जामन, जो दूध को जमा देता है। लेकिन दही यदि खट्टा या कषाय हो तो वह दूध को फाड़ देता है। इसीलिए लोग उल्लसित, उबलित दूध से खट्टे दही को दूर ही रखते हैं।
व्यंग्य-विनोद दोनों सगे भाई हैं। तब रूठकर व्यंग्य अलग घर बसा ले, यह सामाजिकता नहीं है, भारतीयता नहीं है। इसलिए व्यंग्य को अलग विधा के रूप में स्वीकार करना मेरे लिए अग्राह्य है। बिना व्यंग्य के समूचा साहित्य ही नहीं, हास्य-कविता भी श्रीहीन है। मेरी मान्यता है कि जिस तरह उत्तम गद्य लिखना पद्य से कहीं कठिन है, उसी प्रकार व्यंग्य लिखना भी……….। व्यंग्य वह सामाजिक और साहित्यिक सिद्धि है, जो हरेक को प्राप्त नहीं होती। इसे अभ्यास से भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसके लेखक को पहले स्वयं आलंबन बनना पड़ता है। विसंगतियों और विषमताओं के दौर से जो स्वयं नहीं गुजरा, वह राजनीति के मंच पर भाषण तो दे सकता है, व्यंग्य में कशाघात नहीं कर सकता। अगर फिर भी वह ऐसा करने की चेष्टा करता है तो वह केवल आक्रोशी बन जाएगा, गाली-गलौज करने लगेगा, ऐसा बोलेगा और लिखेगा जैसे किसी राजनीतिक दल विशेष का एजेंट हो। उसकी कटूक्तियां स्वयं उसे खा जाएंगी। या, उसके पेशेवर व्यंग्य लिखने के प्रयत्न मात्र शब्दजाल, गपोड़े और बीच-बीच में पाठकों की खीस निकालने वाले सस्ते प्रकरण बन जाएंगे।
अच्छे व्यंग्य-लेखक के लिए सामाजिक नैतिकता पहली शर्त है। जिंदादिल विद्वज्जनों की अंतरंगता प्राप्त किए बिना कोई अच्छा व्यंग्य-लेखक नहीं बन सकता। कहूं कि आम आदमी की मानसिकता के साथ उनका निरंतर जुड़े रहना बहुत जरूरी है। व्यंग्य लिखने के लिए साहित्य की विधाओं का ज्ञान प्राप्त करना ही पर्याप्त नहीं, उसमें राजनीति के नए-से-नए आंदोलनों, समाज के अनुदिन के उतार-चढ़ावों, वैज्ञानिक विकृतियों, इतिहास के बदलते हुए पृष्ठों तथा दुनिया कहां जा रही है, सबकी प्रामाणिक जानकारी के प्रति ललक बनी रहनी चाहिए। जो आंख से नहीं देखता, कान से नहीं सुनता, समाज में घुसकर उसकी भलाई-बुराई को स्वयं अनुभव नहीं करता और जो संवेदनशील नहीं है, वह कभी व्यंग्यकार नहीं बन सकता।
यदि व्यंग्य-विनोद के साक्षात् दर्शन करने हों तो लोक में रमिए। यहां पग-पग पर व्यंग्य-विनोद के कुसुम खिले हुए हैं। विवाह में ज्यौनार के समय पकवानों के साथ कन्या-पक्ष की नारियों की ‘गालियों’ का स्वाद भी चखिए। बारात के गांव से निकलने के बाद नारियों का ‘खोइया’ देखिए- इसमें नाटक का भी आनंद है और व्यंग्य-विनोद के साक्षात दर्शन भी। होली के अवसर पर यदि आपने पुरुषों को नाचते-गाते नहीं देखा तो क्या देखा। मिल जाएं तो ईसुरी की फाग, लखमीचंद की रागनियां, ख्यालबाजी, पढंत, ब्रज की तानें और धमार में जो व्यंग्य-विनोद समाहित है वह साहित्य में कहां ? पश्चात्ताप इस बात का है कि इस ओर हमारे सुधीजनों, समालोचकों और शोधकर्ताओं का ध्यान नहीं गया। ऐसी रचनाओं को एकत्र करके प्रकाशित नहीं किया गया। मैंने ब्रज, बुंदेलखंड, राजस्थान, मैथिल, पंजाब, हरियाणा और बंगाल की लोक-रचनाएं सुनी हैं और मन-ही-मन अनुभव किया है कि साहित्य का दृश्य और श्रव्य इस लोकानंद के पासंग में भी नहीं ठहरता। अघाने तापिए, चौपालों पर बैठिए, कुंड-सरोवरों पर व्यंग्य-विनोदी उपाख्यान सुनिए तो निश्चयपूर्वक कह सकता हूं कि आप मेरे इस कथन से सहमत हो जाएंगे। अंत में बरसाने की फाग का एक टुकड़ा निवेदित करता हूं-
“जो रस बरसाने में बरसै,
सो रस तीन लोक में नॉंय।”
तीन लोक की बात तो नहीं जानता, परंतु इस धरातल पर भले ही साहित्य में व्यंग्य-विनाद की कमी हो, लोकरस का निराला आनंद सर्वत्र गुलाब की कलियों की तरह चटख रहा है, मटक रहा है। व्यंग्य-विनोद के प्रेमियों के हृदय में रसानुभूति की तरह अटक रहा है। इसकी लटक को, इसकी लोच और लचक को जरा देखिए तो सही ! कहने का तात्पर्य यह है कि व्यंग्य-विनोद शास्त्र से लेकर लोक तक सर्वत्र प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप में विद्यमान है। देखने वाली आंख चाहिए। फिर कहता हूं–
दिल दे तो इस मिज़ाज़ का परवरदिगार दे,
जो रंज की घड़ियां भी खुशी से गुज़ार दे।
(‘हास्य सागर’ से, सन् 1996)