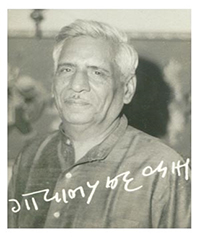 मैं समय हूं। समय से ही धरती पर आया और समय चुकने के साथ ही चला भी जाऊंगा। मैंने समय को परखा है। समय पर चूका भी नहीं हूं। समय को कभी व्यर्थ नहीं गुजरने दिया। उस ज़माने में समय ऐसा ही था, जब एक से एक बढ़कर समाजसेवी, सामयिक तपस्वी और कंकड़-पत्थरों की तरह मणि-माणिक्य बटोरने वाले ही नहीं, महात्मा गांधी जैसे अवतारी महापुरुष, पंडित नेहरू जैसे जननायक, शास्त्रीजी जैसे देश पर निछावर होने वाले, इंदिराजी जैसी दुर्धर्ष और साहसी नेता, एक से एक बढ़कर क्रांतिकारी और इनसब में अग्रगण्य नेताजी सुभाषचंद्र बोस जैसे बलिदानी व्यक्तित्व समय की सामयिकता को सार्थक कर रहे थे।
मैं समय हूं। समय से ही धरती पर आया और समय चुकने के साथ ही चला भी जाऊंगा। मैंने समय को परखा है। समय पर चूका भी नहीं हूं। समय को कभी व्यर्थ नहीं गुजरने दिया। उस ज़माने में समय ऐसा ही था, जब एक से एक बढ़कर समाजसेवी, सामयिक तपस्वी और कंकड़-पत्थरों की तरह मणि-माणिक्य बटोरने वाले ही नहीं, महात्मा गांधी जैसे अवतारी महापुरुष, पंडित नेहरू जैसे जननायक, शास्त्रीजी जैसे देश पर निछावर होने वाले, इंदिराजी जैसी दुर्धर्ष और साहसी नेता, एक से एक बढ़कर क्रांतिकारी और इनसब में अग्रगण्य नेताजी सुभाषचंद्र बोस जैसे बलिदानी व्यक्तित्व समय की सामयिकता को सार्थक कर रहे थे।
समय ने मुझे चेताया कि स्वदेश, स्वभाषा, स्वसंस्कृति और इन सबका मार्गदर्शन करने वाला साहित्य प्रतीक्षारत है। यदि खड्ग नहीं उठा सकते तो तलवार से भी ज्यादा धारदार कलम को उठाओ।
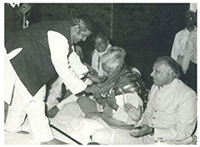 मैंने कलम उठाई तो समय ने चेतावनी दी कि हे पृथ्वी-पुत्र, देश की धरती से जुड़ो। धरती पर असंख्य दीन-हीन, अभावग्रस्त, रूढ़ियों में फंसे, पाखंडों में घिरे लोग विसंगति और विषमता का असहनीय त्रास भोग रहे हैं। उनकी ओर देखो। मत देखो आकाश की ओर। चार दिन की चांदनी दिखाकर निरंतर घटने वाले चंद्रमा या चंद्रमुखियों के चक्कर में मत पड़ो। तुम आकाश के तारे गिनने के लिए पैदा नहीं हुए हो। विधाता ने तुम्हारी कलम को साहित्य का सौभाग्य सुलभ किया है। वह साहित्य जो राज और समाज का मार्गदर्शन करता है। वह साहित्य जो क्रांति के लिए मार्ग प्रशस्त करता है। अपनी कलम को, अपनी कला को इधर मोड़ो।
मैंने कलम उठाई तो समय ने चेतावनी दी कि हे पृथ्वी-पुत्र, देश की धरती से जुड़ो। धरती पर असंख्य दीन-हीन, अभावग्रस्त, रूढ़ियों में फंसे, पाखंडों में घिरे लोग विसंगति और विषमता का असहनीय त्रास भोग रहे हैं। उनकी ओर देखो। मत देखो आकाश की ओर। चार दिन की चांदनी दिखाकर निरंतर घटने वाले चंद्रमा या चंद्रमुखियों के चक्कर में मत पड़ो। तुम आकाश के तारे गिनने के लिए पैदा नहीं हुए हो। विधाता ने तुम्हारी कलम को साहित्य का सौभाग्य सुलभ किया है। वह साहित्य जो राज और समाज का मार्गदर्शन करता है। वह साहित्य जो क्रांति के लिए मार्ग प्रशस्त करता है। अपनी कलम को, अपनी कला को इधर मोड़ो।
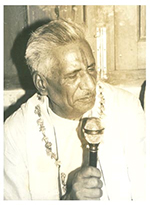 मुझे सूत्र याद आया-स्वान्तः सुखाय। तो पाया कि मूर्तिकार यद्यपि अपनी कलाकृति को अपने मन के सुख के लिए गढ़ता है, पर उसकी स्थापना अपने घर में नहीं करता। चित्रकार बड़ी लगन से, मानसिक उल्लास से, विविध रंगों के संयोजन से मनमोहक चित्र बनाता है, पर उसे अपनी बैठक में नहीं टांगता। गायक और वादक की स्वान्तः सुखाय भाव से अहर्निश स्वर-ताल-साधना की सार्थकता केवल उन तक सीमित नहीं रहती। इसी प्रकार कवि और लेखक स्वान्तः सुखाय भाव से एकाग्रचित्त होकर अपनी रचनाधर्मिता का निर्वाह करता है, परंतु घर की दीवारों को सुनाने के लिए नहीं।
मुझे सूत्र याद आया-स्वान्तः सुखाय। तो पाया कि मूर्तिकार यद्यपि अपनी कलाकृति को अपने मन के सुख के लिए गढ़ता है, पर उसकी स्थापना अपने घर में नहीं करता। चित्रकार बड़ी लगन से, मानसिक उल्लास से, विविध रंगों के संयोजन से मनमोहक चित्र बनाता है, पर उसे अपनी बैठक में नहीं टांगता। गायक और वादक की स्वान्तः सुखाय भाव से अहर्निश स्वर-ताल-साधना की सार्थकता केवल उन तक सीमित नहीं रहती। इसी प्रकार कवि और लेखक स्वान्तः सुखाय भाव से एकाग्रचित्त होकर अपनी रचनाधर्मिता का निर्वाह करता है, परंतु घर की दीवारों को सुनाने के लिए नहीं।
कला को जनरंजन के साथ-साथ जनमानस को बदलने वाला और क्रांतिवाहिनी होना चाहिए। कला कला के लिए नहीं होती। कला की सार्थकता मानवता या कहें कि समाज के लिए है। मैंने समय की मांग को यथासंभव पूरा करने का प्रयत्न किया है। उसमें कहां तक सफल हुआ हूं और किस प्रकार विफल हुआ हूं, इसे पीछे मुड़कर देखने या परखने का काम मेरा नहीं है। यह काम समय का है। वही यथासमय इसका निर्णय करेगा।
 राष्ट्र के जागरण के साथ-साथ उन दिनों राष्ट्रभाषा के अभ्युदय का भी समय था। हिन्दी के सभी पुराने कवियों की तरह मैंने भी ब्रजभाषा और ब्रज-साहित्य को अपनाया। मेरी कविता भी ब्रजभाषा से प्रारंभ हुई। ब्रजभाषा में कितनी कविताएं लिखीं, उनकी गिनती करके आपको बताने से क्या लाभ ? पर जैसे ही मुझे ज्ञात हुआ कि मेरी ब्रज-कविताएं पुरानी परिपाटी और परवर्ती कवियों का चर्वित चर्वण हैं तो जैसे ही सुयोग मिला, मैं खड़ीबोली हिन्दी की ओर प्रवृत्त होगया। देशभक्ति के गीत लिखे। छायावादी टाइप की कुछ रचनाएं भी लिखीं। परंतु सोचा कि साहित्य की इस ऐतिहासिक धरोहर को प्रसादजी, पंतजी और महादेवीजी वर्मा के पास ही रहने दूं। यह दुःसाध्य कार्य मेरे वश का नहीं है। क्योंकि अधिकतर ऐसी रचनाएं स्वान्तः सुखाय भाव से ही लिखी गई हैं। जन-साधारण से इनका कुछ लेना-देना नहीं है। तभी अचानक व्यंग्य-विनोद के धनुष-बाण मेरे हाथ लग गए और मन ने गुनगुनाया, “हास्य सोने की अंगूठी, व्यंग्य सांवरौ नगीना है। बस तब फिर क्या था ! मेरी कलम से हास्य के फूल बरसने लगे और मेरे तरकस से व्यंग्य के तीर छूटने लगे। साठ बरस से अधिक समय तक मैं निरंतर व्यंग्य-विनोद लिखता रहा हूं। गुणवत्ता की बात आप जानें, लेकिन परिमाण में मैंने इतना लिखा है कि अब उसे समेटना दूभर होगया है।
राष्ट्र के जागरण के साथ-साथ उन दिनों राष्ट्रभाषा के अभ्युदय का भी समय था। हिन्दी के सभी पुराने कवियों की तरह मैंने भी ब्रजभाषा और ब्रज-साहित्य को अपनाया। मेरी कविता भी ब्रजभाषा से प्रारंभ हुई। ब्रजभाषा में कितनी कविताएं लिखीं, उनकी गिनती करके आपको बताने से क्या लाभ ? पर जैसे ही मुझे ज्ञात हुआ कि मेरी ब्रज-कविताएं पुरानी परिपाटी और परवर्ती कवियों का चर्वित चर्वण हैं तो जैसे ही सुयोग मिला, मैं खड़ीबोली हिन्दी की ओर प्रवृत्त होगया। देशभक्ति के गीत लिखे। छायावादी टाइप की कुछ रचनाएं भी लिखीं। परंतु सोचा कि साहित्य की इस ऐतिहासिक धरोहर को प्रसादजी, पंतजी और महादेवीजी वर्मा के पास ही रहने दूं। यह दुःसाध्य कार्य मेरे वश का नहीं है। क्योंकि अधिकतर ऐसी रचनाएं स्वान्तः सुखाय भाव से ही लिखी गई हैं। जन-साधारण से इनका कुछ लेना-देना नहीं है। तभी अचानक व्यंग्य-विनोद के धनुष-बाण मेरे हाथ लग गए और मन ने गुनगुनाया, “हास्य सोने की अंगूठी, व्यंग्य सांवरौ नगीना है। बस तब फिर क्या था ! मेरी कलम से हास्य के फूल बरसने लगे और मेरे तरकस से व्यंग्य के तीर छूटने लगे। साठ बरस से अधिक समय तक मैं निरंतर व्यंग्य-विनोद लिखता रहा हूं। गुणवत्ता की बात आप जानें, लेकिन परिमाण में मैंने इतना लिखा है कि अब उसे समेटना दूभर होगया है।
कविता साहित्य की ऐसी विधा है जो सहज में ही लोकप्रियता प्राप्त कर लेती है। रसिकों का कंठहार बन जाती है। कवि को सिद्धि और प्रसिद्धि प्रदान करती है। मैंने कविता के द्वारा देश के कोने-कोने में ही नहीं, विदेशों में जहां-जहां भारतीय बसते हैं या देश-विदेश के अहिन्दीभाषी लोगों से वह सब प्राप्त किया जो कवि-जीवन की सार्थकता के लिए शायद बहुत दिनों तक स्मरण किया जाता रहेगा। परंतु कविता सूत्र है। वह बिम्बों और प्रतीकों द्वारा तादात्म्य स्थापित करती है। लेकिन मेरी समझ से यह ऐसी विधा है, जिसमें बहुत कुछ अनकहा रह जाता है।
मन छटपटाता रहता है कि कैसे अपने को संपूर्णता से व्यक्त करूं ? तभी मुझे संस्कृत की एक सूक्ति स्मरण हो आई, ”गद्यं कवीनां निकषं वदन्ति।” बाणभट्ट ने इस उक्ति को सार्थकता प्रदान की थी। उनकी ‘कादंबरी’ काल की कसौटी पर खरी उतरी थी।
परंतु मैं कोई जड़, पीली धातु नहीं हूं जो किसी भोंडे पत्थर से टक्कर लेता रहूं। मेरे पास कोई सुंदर कसौटी भी नहीं है। जो आपको देकर कहूं कि जिसे आप सोना समझते हों, जरा कसकर देखो, ताकि कलियुग की इस विभीषिका की पहचान हो सके। ध्यान से देखो कि कसौटी पर कोई रंग उभरता है या खरोंचें पड़ती हैं। परंतु यह काम मेरा या तुम्हारा नहीं है। यह काम तो आने वाले समय का है। वही समय आने पर अपनी कसौटी का इस्तेमाल करेगा। यह काम आज के साहित्याचार्यों का, विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमी तिकड़मी डॉक्टरों का, पदों और पुरस्कारों के लिए राशन जैसी लाइन लगाने वालों का नहीं है।
समय ने मेरी भर्त्सना की, मैंने तुम्हें धनुष-बाण इसलिए नहीं दिए थे कि अपने तीर हवा में छोड़ते रहो। मेरी अपेक्षा थी कि तुम लक्ष्य-वेध करो। समझे लक्ष्य-वेध का मतलब ? देखा तुमने कभी दीन-हीन दुःखी लोगों की ओर ? पूछा अपने से कभी कि आज गरीब गरीब क्यों है ? अमीर कैसी कमाई से अपार संपत्ति का स्वामी बन बैठा है ? क्या ध्यान गया तुम्हारा कभी इस बात पर कि आज जिसके पास है, वह भी दुःखी है और जिसके पास नहीं है, वह भी दुःखी है, भला क्यों ? राजा भी दुःखी और रंक भी दुःखी ! भूमिहीन किसान भी दुःखी। शोषण से त्रस्त मजदूर भी दुःखी। नेता राज-पद पाकर भी दुःखी और जनता उसे अपना प्रतिनिधि बनाकर, नेतृत्व सौंपकर भी दुःखी। असमानता से नारी दुःखी। कुपोषण और अशिक्षा से बालक दुःखी। वृद्ध बीते हुए समय को याद कर-करके दुःखी। सब दुःखी। सब सामाजिक अन्याय से पीड़ित। सब भ्रष्टाचार के मकड़जाल में फंसे हुए। समाजसेवी समाज-परिष्कार न करके अपने परिष्कार में लगे हुए हैं। इस विडंबना की ओर भी तो ध्यान देना व्यंग्य-विनोदी लेखक का काम है कि आज मनुष्य और मनुष्य के बीच खाई क्यों पड़ गई है। धर्म नहीं, संप्रदाय कहो, अपने-अपने स्वार्थों के लिए अपने मताग्रहों को विधर्मियों पर थोपने के लिए क्या-कुछ नहीं कर रहे ?
लेखक वर्ग का लेखन जो पहले राज्याश्रय के लिए होता था, राजाओं और सामंतों की स्तुति ही जिसका धर्म था, जागीर और पुरस्कार पाना जिसका उद्देश्य था। राज्य की प्रतिष्ठा पाकर जन-जन में प्रतिष्ठित कहलवाना ही जिसकी कला का लक्ष्य था। क्या वह आज भी नहीं दुहराया जा रहा ? विश्वबंधुत्व और मानवता के गीत पहले भी गाए जाते थे और आज भी उनका स्तवन हो रहा है। लेकिन मानवता आज के मानव में रही कहां ? वह चंद बुद्धिजीवियों के प्रवचनों एवं लेखों में रह गई है अथवा नेताओं के नारों में। इस विषमता पर, इस अन्याय पर, इस शोषण पर तुमने क्या लिखा और कितना लिखा ? ज़रा बताओ तो सही। मैंने तुम्हें सोने की अंगूठी इसलिए नहीं पहनाई थी कि तुम हाथ उठा-उठाकर उसे चमकाते रहो। उसमें श्याम नगीना इसलिए जड़कर दिया था कि समाज में आज जो कलुष, कटुता और सांवरे अंधकार की कालरात्रि व्याप्त है, उसमें उजाले की किरण का प्रकाश फैला सको। दीन-दुखियों के म्लान मुखमंडल पर मुस्कान की आभा बिखेर सको। मैंने तो तुम्हें व्यंग्य-विनोद के यही उद्देश्य बताए थे। लेकिन लगे रहे तुम अपने को प्रतिष्ठित करने में और भूल गए गरीबी की रेखा के नीचे बैठै हुए उस व्यक्ति को जो दुःखों के मटमैले खारे सागर में डूबा जा रहा है। अब भी समय है। अपने कालमों में, अपने गद्य-पद्य के लेखन में इस अभाव को दूर कर सको तो करो। बहुत कह लिया तुमने स्वान्तः सुखाय के संबंध में। अब ‘सर्वे भवन्तु सुखिनः’ को अपना परम साध्य बनाओ। इसी में तुम्हारा और जनजीवन का कल्याण है।
हां तो मैं गद्य के क्षेत्र में उतरा। उतरा कहना गलत होगा, कहना होगा कि गिरनार पर्वत की सीढ़ियों पर चढ़ना शुरू किया। उछलता हुआ चला। ताजमहल में जैसे लोग अपना नाम खोद जाते हैं, ऐसे ही हर सीढ़ी पर अपनी छाप छोड़ता चला गया। चढ़ता गया, पर मंजिल का ओर-छोर तो दिखाई ही नहीं पड़ता था। पीछे मुड़कर देखना या उतरना तो मैंने सीखा ही नहीं। इसलिए आवाज दे रहा हूं नई पीढ़ी को कि आओ, मुझे सहारा दो। मेरे डगमगाते कदमों को संभालो। हे भविष्य के होनहार लेखकों, मैं नहीं पा सका तो तुम मंजिल को अवश्य प्राप्त करना। उत्साही और लगनशीलों से मिलने के लिए मंजिल खुद उन तक दौड़ी चली आती है।
प्रस्तुत पुस्तक मेरे प्रकाशित और अप्रकाशित व्यंग्य-विनोदी निबंधों का समग्र संकलन है। इस प्रकार के लेख लिखे काफी, छांटे कम। ज़रा सोचिए सन् 36 से सन् 96 तक कितने वर्ष हुए। तभी से निरंतर लिख रहा हूं। अनुमान लगा सकते हो कितना लिखा होगा ? जब-जब उन्हें पढ़ा तो “निज कवित्त केहि लागि न नीका”। लेकिन मुझे कोई भी तो फीका नहीं लगा। परंतु समय की सीमा है। छापने वाले के पास वक्त नहीं है और पाठकों के पास बड़े-बड़े पोथों को पढ़ने की फुरसत नहीं है। वे तो आवरण पृष्ठ देखकर पुस्तक की ओर आकर्षित होते हैं और भूमिका पढ़कर तथा पन्ने पलटकर सोचते कि ”पोथी पढ़-पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय।”
(व्यास के हास-परिहास से, सन् 1998)