गोपालप्रसाद व्यास से साक्षात्कार
(श्री विश्वनाथ त्रिपाठी )
हिन्दी की संस्कृति के प्रतीक व्यासजी
 परम श्रद्धेय, हिन्दी के अनन्य सेवक और हमारे सम्माननीय पं. गोपालप्रसाद व्यासजी के व्यक्तित्व के प्रति मेरे मन में जो सम्मान है, वह अनेक कारणों से है। सबसे पहले तो मैं, यह निवेदन करूं कि मेरे गुरु आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदीजी व्यासजी से बहुत स्नेह रखते थे और व्यासजी से उनका बहुत अंतरंग संबंध था। व्यासजी जब 50 वर्ष के हुए तो उनके सम्मान में एक अभिनंदन ग्रंथ निकला था। कोई समारोह हुआ था दिल्ली में। मैं व्यासजी को जानता तो था, लेकिन उनकी गरिमा से उस समय बहुत अधिक परिचित नहीं था। मैंने द्विवेदीजी से पूछा कि “आप यहां व्यासजी के सम्मान में इतनी दूर से क्यों आए हैं ?” तो उन्होंने मुझे बहुत देर तक समझाया और कहा कि “तुम व्यासजी कि विद्वता से, उनके व्यक्तित्व से, उनकी हिन्दीसेवा से भली-भांति परिचित नहीं हो। वह बहुत कर्मठ आदमी हैं, बहुत उद्योगी आदमी हैं। वह सिर्फ हास्यरस के कोई सामान्य कवि ही नहीं हैं, बल्कि उनका व्यक्तित्व बहुमुखी है।” दूसरे जिस साहित्यकार का मैं बहुत सम्मान करता हूं उनका नाम है डॉ. रामविलास शर्मा। उनको जब साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था तो उसमें व्यासजी भी गए थे और उनके जाने का उल्लेख डॉ. रामविलास ने मुझसे बाद में किया था। फिर अनेक ऐसे प्रसंग आए जब मुझे इस बात का प्रमाण मिला कि व्यासजी कोई साधारण हिन्दीसेवी नहीं हैं और कुछ मेरा सौभाग्य रहा है कि उनकी मेरे ऊपर कृपा भी लगातार बनी रही। सामान्यतः लोग उनको हास्यरस के कवि के रूप में जानते हैं। शायद इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि व्यासजी ने अपने चारों ओर प्रभामंडल बनाने का कोई प्रयास नहीं किया। वह बहुत समर्थ गद्यकार हैं। लगभग पचास वर्षों से अधिक उनका एक बहुत मशहूर स्तंभ ‘नारदजी खबर लाए हैं’ दैनिक ‘हिन्दुस्तान’ में छपता है। मैं समझता हूं कि लगभग पचास वर्षों से लगातार कोई कालम शायद ही किसी भाषा के साहित्य में कहीं चला हो। फिर उन्होंने ‘यत्र-तत्र-सर्वत्र’ का स्तंभ भी प्रतिदिन लिखा था। राजनैतिक और सामाजिक दृष्टि से वर्षों तक ऐसा स्तंभ लिखना कोई साधारण बात नहीं है। जो हिन्दी की संस्कृति है, उसके प्रतिनिधि, उसके प्रतीक हैं वे। उन्होंने ‘ब्रज विभव’ नाम से एक दुर्लभ ग्रंथ का संपादन किया है। वह ऐसा अनुकरणीय व आदर्श ग्रंथ है कि हिन्दी की जितनी बोलियां हैं, उन सभी बोलियों के जो प्रेमी हैं, उनको ऐसे ही ग्रंथ निकालने चाहिए। उनके लिए एक आदर्श का काम करेंगे। जैसे ‘ब्रज विभव’ निकला है, वैसे ही ‘अवध विभव’, ‘छत्तीसगढ़ी विभव’ तथा ‘भोजपुरी विभव’ निकलने चाहिए। यह बड़ा ही महत्वपूर्ण काम किया है व्यासजी ने। ऐसे व्यक्ति का अनुभव बड़ा लम्बा है। बड़ा दीर्घ अनुभव है। वह वयोवृद्ध हैं। लोग वयोवृद्ध होते हैं, व्यासजी भी वयोवृद्ध हैं तो हमने यह उचित समझा कि ऐसे अवसर पर उनसे मिलकर जो हो सके, उनसे जानकारी हासिल करके हम भी लाभान्वित हों। मेरे प्रणाम करते ही व्यासजी प्रमुदित होकर बैठ गए। मैनें व्यासजी से उनके साहित्य-संस्कार के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा-
परम श्रद्धेय, हिन्दी के अनन्य सेवक और हमारे सम्माननीय पं. गोपालप्रसाद व्यासजी के व्यक्तित्व के प्रति मेरे मन में जो सम्मान है, वह अनेक कारणों से है। सबसे पहले तो मैं, यह निवेदन करूं कि मेरे गुरु आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदीजी व्यासजी से बहुत स्नेह रखते थे और व्यासजी से उनका बहुत अंतरंग संबंध था। व्यासजी जब 50 वर्ष के हुए तो उनके सम्मान में एक अभिनंदन ग्रंथ निकला था। कोई समारोह हुआ था दिल्ली में। मैं व्यासजी को जानता तो था, लेकिन उनकी गरिमा से उस समय बहुत अधिक परिचित नहीं था। मैंने द्विवेदीजी से पूछा कि “आप यहां व्यासजी के सम्मान में इतनी दूर से क्यों आए हैं ?” तो उन्होंने मुझे बहुत देर तक समझाया और कहा कि “तुम व्यासजी कि विद्वता से, उनके व्यक्तित्व से, उनकी हिन्दीसेवा से भली-भांति परिचित नहीं हो। वह बहुत कर्मठ आदमी हैं, बहुत उद्योगी आदमी हैं। वह सिर्फ हास्यरस के कोई सामान्य कवि ही नहीं हैं, बल्कि उनका व्यक्तित्व बहुमुखी है।” दूसरे जिस साहित्यकार का मैं बहुत सम्मान करता हूं उनका नाम है डॉ. रामविलास शर्मा। उनको जब साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था तो उसमें व्यासजी भी गए थे और उनके जाने का उल्लेख डॉ. रामविलास ने मुझसे बाद में किया था। फिर अनेक ऐसे प्रसंग आए जब मुझे इस बात का प्रमाण मिला कि व्यासजी कोई साधारण हिन्दीसेवी नहीं हैं और कुछ मेरा सौभाग्य रहा है कि उनकी मेरे ऊपर कृपा भी लगातार बनी रही। सामान्यतः लोग उनको हास्यरस के कवि के रूप में जानते हैं। शायद इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि व्यासजी ने अपने चारों ओर प्रभामंडल बनाने का कोई प्रयास नहीं किया। वह बहुत समर्थ गद्यकार हैं। लगभग पचास वर्षों से अधिक उनका एक बहुत मशहूर स्तंभ ‘नारदजी खबर लाए हैं’ दैनिक ‘हिन्दुस्तान’ में छपता है। मैं समझता हूं कि लगभग पचास वर्षों से लगातार कोई कालम शायद ही किसी भाषा के साहित्य में कहीं चला हो। फिर उन्होंने ‘यत्र-तत्र-सर्वत्र’ का स्तंभ भी प्रतिदिन लिखा था। राजनैतिक और सामाजिक दृष्टि से वर्षों तक ऐसा स्तंभ लिखना कोई साधारण बात नहीं है। जो हिन्दी की संस्कृति है, उसके प्रतिनिधि, उसके प्रतीक हैं वे। उन्होंने ‘ब्रज विभव’ नाम से एक दुर्लभ ग्रंथ का संपादन किया है। वह ऐसा अनुकरणीय व आदर्श ग्रंथ है कि हिन्दी की जितनी बोलियां हैं, उन सभी बोलियों के जो प्रेमी हैं, उनको ऐसे ही ग्रंथ निकालने चाहिए। उनके लिए एक आदर्श का काम करेंगे। जैसे ‘ब्रज विभव’ निकला है, वैसे ही ‘अवध विभव’, ‘छत्तीसगढ़ी विभव’ तथा ‘भोजपुरी विभव’ निकलने चाहिए। यह बड़ा ही महत्वपूर्ण काम किया है व्यासजी ने। ऐसे व्यक्ति का अनुभव बड़ा लम्बा है। बड़ा दीर्घ अनुभव है। वह वयोवृद्ध हैं। लोग वयोवृद्ध होते हैं, व्यासजी भी वयोवृद्ध हैं तो हमने यह उचित समझा कि ऐसे अवसर पर उनसे मिलकर जो हो सके, उनसे जानकारी हासिल करके हम भी लाभान्वित हों। मेरे प्रणाम करते ही व्यासजी प्रमुदित होकर बैठ गए। मैनें व्यासजी से उनके साहित्य-संस्कार के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा-
 बंधुवर त्रिपाठीजी, पहले तो आप कृपा करके स्वयं हमारी कुटिया में पधारे, आपका हृदय से सपरिवार स्वागत करता हूं। ये मेरा अहोभाग्य है कि आप जैसा साहित्य मनीषी हमारे घर आए और हमारे बारे में कुछ जाने, कुछ कहे, कुछ बताए यह हमारा परम सौभाग्य है। जहां तक मेरे साहित्य-संस्कार की बात है, जैसे मैंने बताया कि मेरा जन्म हुआ ब्रज चौरासी कोस के देवता गिरिराज महाराज की तलहटी में, वल्लभाचार्य ने जिसको ‘आदिवृंदावन’ कहा है, जहां परम रासस्थली बनी है, जहां पर महारास हुआ, जहां इन्द्र ने नगाड़े बजाए, वे पत्थर की शिलाएं भी वहां रखी हैं, जो बजाने से नगाड़ों की तरह बजने लगती हैं।
बंधुवर त्रिपाठीजी, पहले तो आप कृपा करके स्वयं हमारी कुटिया में पधारे, आपका हृदय से सपरिवार स्वागत करता हूं। ये मेरा अहोभाग्य है कि आप जैसा साहित्य मनीषी हमारे घर आए और हमारे बारे में कुछ जाने, कुछ कहे, कुछ बताए यह हमारा परम सौभाग्य है। जहां तक मेरे साहित्य-संस्कार की बात है, जैसे मैंने बताया कि मेरा जन्म हुआ ब्रज चौरासी कोस के देवता गिरिराज महाराज की तलहटी में, वल्लभाचार्य ने जिसको ‘आदिवृंदावन’ कहा है, जहां परम रासस्थली बनी है, जहां पर महारास हुआ, जहां इन्द्र ने नगाड़े बजाए, वे पत्थर की शिलाएं भी वहां रखी हैं, जो बजाने से नगाड़ों की तरह बजने लगती हैं।
जिसका नाम चंद्र सरोवर है, इसके संबंध में एक पौराणिक व्याख्या यह है कि भगवान के रास के समय में चन्द्रमा ने अपना अमृत उस सरोवर में निचोड़ा था, इसलिए इसका नाम ‘चंद्र सरोवर’ होगया। उस सरोवर के उस पार तो सूरदासजी ने ललित लीला के पद गाए थे और इस पार मेरा जन्म हुआ था। हमारा सूरदासजी से गांव का नाता है। हमारे गांव के लोगों का कृष्णभक्ति, रासलीला के पदों से गहरा नाता था। सूरदासजी के अलभ्य पदों को सभी लोग सुनाया करते थे। हमारे पिताजी तो सूरदासजी के भजनों का कीर्तन करते हुए उठते थे और सेवा करते समय वे मंगला के, श्रृंगार के, भोग के, आरती के पदों को तानपूरे पर गाया करते थे। उस सूरकुटी का प्रभु ने ऐसा सहयोग दिया कि मैंने उसका जीर्णोद्धार कराया और जिस चबूतरे पर सूरदासजी बैठा करते थे और उनके पीछे उनका एक भक्त टीप्पणी (डायरी) लेकर बैठ जाता था। सूरदासजी गाते थे और वह लिखता जाता था। उससे ही ‘सूर सागर’ बाद में प्रकाश में आया तो मैंने भी देखा-देखी बाद में ‘हास्य सागर’ नाम से एक ग्रंथ लिखा। सूरदासजी का ‘सूर सागर’ और मेरा ‘हास्य सागर’।
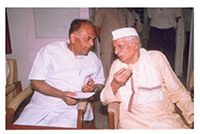 जिसका नाम चंद्र सरोवर है, इसके संबंध में एक पौराणिक व्याख्या यह है कि भगवान के रास के समय में चन्द्रमा ने अपना अमृत उस सरोवर में निचोड़ा था, इसलिए इसका नाम ‘चंद्र सरोवर’ होगया। उस सरोवर के उस पार तो सूरदासजी ने ललित लीला के पद गाए थे और इस पार मेरा जन्म हुआ था। हमारा सूरदासजी से गांव का नाता है। हमारे गांव के लोगों का कृष्णभक्ति, रासलीला के पदों से गहरा नाता था। सूरदासजी के अलभ्य पदों को सभी लोग सुनाया करते थे। हमारे पिताजी तो सूरदासजी के भजनों का कीर्तन करते हुए उठते थे और सेवा करते समय वे मंगला के, श्रृंगार के, भोग के, आरती के पदों को तानपूरे पर गाया करते थे। उस सूरकुटी का प्रभु ने ऐसा सहयोग दिया कि मैंने उसका जीर्णोद्धार कराया और जिस चबूतरे पर सूरदासजी बैठा करते थे और उनके पीछे उनका एक भक्त टीप्पणी (डायरी) लेकर बैठ जाता था। सूरदासजी गाते थे और वह लिखता जाता था। उससे ही ‘सूर सागर’ बाद में प्रकाश में आया तो मैंने भी देखा-देखी बाद में ‘हास्य सागर’ नाम से एक ग्रंथ लिखा। सूरदासजी का ‘सूर सागर’ और मेरा ‘हास्य सागर’।
जिसका नाम चंद्र सरोवर है, इसके संबंध में एक पौराणिक व्याख्या यह है कि भगवान के रास के समय में चन्द्रमा ने अपना अमृत उस सरोवर में निचोड़ा था, इसलिए इसका नाम ‘चंद्र सरोवर’ होगया। उस सरोवर के उस पार तो सूरदासजी ने ललित लीला के पद गाए थे और इस पार मेरा जन्म हुआ था। हमारा सूरदासजी से गांव का नाता है। हमारे गांव के लोगों का कृष्णभक्ति, रासलीला के पदों से गहरा नाता था। सूरदासजी के अलभ्य पदों को सभी लोग सुनाया करते थे। हमारे पिताजी तो सूरदासजी के भजनों का कीर्तन करते हुए उठते थे और सेवा करते समय वे मंगला के, श्रृंगार के, भोग के, आरती के पदों को तानपूरे पर गाया करते थे। उस सूरकुटी का प्रभु ने ऐसा सहयोग दिया कि मैंने उसका जीर्णोद्धार कराया और जिस चबूतरे पर सूरदासजी बैठा करते थे और उनके पीछे उनका एक भक्त टीप्पणी (डायरी) लेकर बैठ जाता था। सूरदासजी गाते थे और वह लिखता जाता था। उससे ही ‘सूर सागर’ बाद में प्रकाश में आया तो मैंने भी देखा-देखी बाद में ‘हास्य सागर’ नाम से एक ग्रंथ लिखा। सूरदासजी का ‘सूर सागर’ और मेरा ‘हास्य सागर’।
प्रश्न : व्यासजी आपकी पढ़ाई कहां तक हुई ?
उत्तर : पढ़ाई का ये हाल है कि मैं पढ़ा ज़रूर दर्जा सात तक, लेकिन हर बार प्रमोशन से पास हुआ। क्योंकि मेरा ध्यान गणित में, अंग्रेजी में, भूगोल में, फालतू चीजों में नहीं लगा। मैं तो कविता करता था और यमुनाजी के तट पर बैठकर लहरों को गिना करता था। पानी में चादर पड़ती है, भंवर पड़ते हैं, उनको देखा करता था। मछलियां कैसे जल के बहाव के ऊपर बहती हैं, देखा करता था। नावें कैसे चलती हैं और नाविक कैसे चलाते समय गाते हैं, उनके गीतों को सुना करता था। ये सब मेरे संस्कार बने यमुना से, मथुरा से। उसके बाद आगरा आया तो आगरा में नागरी प्रचारिणी सभा, साहित्य संदेश, बाबू गुलाबराय, रामविलासजी, हरिशंकर शर्मा, अमृतलाल चतुर्वेदी सबसे मेरा संपर्क हुआ। और साहित्य रत्न भंडार में जो उस समय साहित्य की पुस्तकों का एक मात्र केन्द्र था, मैंने उसमें जो नई-नई पुस्तकें आतीं उनका अध्ययन करता। मैं किराये के मकान में नहीं रहा। ‘साहित्य संदेश’ का संपादन करता था, वहीं रद्दी का तकिया बनाकर उसकी टांड पर सो जाता था। जो नई से नई साहित्य की पुस्तकें आतीं उन्हें पढ़ता। तभी मेरे सामने ‘पंतजी’ का ‘पल्लव’ आया। निरालाजी का ‘कुल्लीभाट’ ओर श्यामनारायण पाण्डे का ‘हल्दीघाटी’ आया।
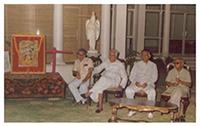 ‘प्रिय-प्रवास’ आया, मैं सभी पढ़ता गया। साहित्य की पुस्तकें और साहित्यकारों से संपर्क यही मेरी कमाई है, यही मेरे संस्कार हैं, यही मेरी शिक्षा है। कइयों की शिक्षा पूरी नहीं हुई। न रवीन्द्रनाथजी की हुई न देवदास गांधी की, न मेरे संपादक मुकुटबिहारी की हुई। लेकिन ये सब अपने समय के बहुत बड़े साहित्यकार व पत्रकार हुए। इसका मुझे बड़ा अफसोस रहा कि मैं मैट्रिक नहीं कर सका। मैं अंग्रेजी नहीं जानता था, तो बनारसीदास चतुर्वेदीजी ने मुझसे कहा कि व्यासजी, आप किसी एंग्लो इंडियन लड़की से प्रेम करो तो आपको अंग्रेजी आ जाएगी। मैंने कहा- मैं क्या प्रेम करूंगा। लेकिन आगरे में एक वैश्य हाउस (छात्रावास) है, उसमें मेरे मित्र पढ़ते थे बचपन के- भारतभूषण अग्रवाल, विद्याभूषण अग्रवाल आदि। रांगेय राघव से भी मेरी परम मित्रता थी। ये सब अंग्रेजी में बोलते थे। इनसे अंग्रेजी सुन-सुनके मैं भी अंग्रेजी जान गया और इतनी जान गया कि जब ‘हिन्दुस्तान’ में आया तो अंग्रेजी समाचारों का अनुवाद भी करने लगा। इसलिए मेरी मान्यता ये है कि जिसे अपनी भाषा अच्छी तरह से आती है, वह दूसरी भाषा भी आसानी से जान जाता है, सीख सकता है।
‘प्रिय-प्रवास’ आया, मैं सभी पढ़ता गया। साहित्य की पुस्तकें और साहित्यकारों से संपर्क यही मेरी कमाई है, यही मेरे संस्कार हैं, यही मेरी शिक्षा है। कइयों की शिक्षा पूरी नहीं हुई। न रवीन्द्रनाथजी की हुई न देवदास गांधी की, न मेरे संपादक मुकुटबिहारी की हुई। लेकिन ये सब अपने समय के बहुत बड़े साहित्यकार व पत्रकार हुए। इसका मुझे बड़ा अफसोस रहा कि मैं मैट्रिक नहीं कर सका। मैं अंग्रेजी नहीं जानता था, तो बनारसीदास चतुर्वेदीजी ने मुझसे कहा कि व्यासजी, आप किसी एंग्लो इंडियन लड़की से प्रेम करो तो आपको अंग्रेजी आ जाएगी। मैंने कहा- मैं क्या प्रेम करूंगा। लेकिन आगरे में एक वैश्य हाउस (छात्रावास) है, उसमें मेरे मित्र पढ़ते थे बचपन के- भारतभूषण अग्रवाल, विद्याभूषण अग्रवाल आदि। रांगेय राघव से भी मेरी परम मित्रता थी। ये सब अंग्रेजी में बोलते थे। इनसे अंग्रेजी सुन-सुनके मैं भी अंग्रेजी जान गया और इतनी जान गया कि जब ‘हिन्दुस्तान’ में आया तो अंग्रेजी समाचारों का अनुवाद भी करने लगा। इसलिए मेरी मान्यता ये है कि जिसे अपनी भाषा अच्छी तरह से आती है, वह दूसरी भाषा भी आसानी से जान जाता है, सीख सकता है।
प्रश्न : व्यासजी कोई अपनी ब्रजभाषा की कविता सुनाने की कृपा कीजिए।
उत्तर : तो सुनिए, ब्रजभाषा का एक स्वरचित छंदः
सूर कही, तुलसी नै लही,
प्रभु पांयन सों परसी ब्रजभाषा।
‘देव’, ‘बिहारी’ करी उर धारन,
मोतिन की लर सी ब्रजभाषा।
‘भूषण’ पाय ‘भवानीं’ भई,
कवि ‘व्यास’ हियै हरसी ब्रजभाषा।
‘मतिराम’ के मानस में सरसी,
धन आनंद ह्वै बरसी ब्रजभाषा।
प्रश्न : व्यासजी आप दिल्ली कब और कैसे आए ?
 उत्तर : दिल्ली, ऐसा है हरिद्वार में हिन्दी साहित्य सम्मेलन का अधिवेशन हुआ। इसमें माखनलालजी चतुर्वेदी को चांदी के रुपयों से तोला गया। मैं उन दिनों सन् 1942 के आंदोलन में तोड़-फोड़ करता हुआ भटकता-भटकता इटावा पहुंच गया था। इटावा में श्रीनारायण चतुर्वेदी के पिता श्री द्वारिकानाथ चतुर्वेदी रहते थे। वह ब्रजभाषा का शब्दकोश बना रहे थे। उन्होंने मुझे आया जानकर अपने पास रख लिया और मैंने ‘ब्रजभाषा शब्दकोश’ तैयार करने में उनकी काफी सहायता की। वह ‘शब्दकोश’ छप भी गया। मैंने श्रीनारायणजी चतुर्वेदी से कहा कि वह कोश मुझे भिजवा दो, मगर वह नहीं भिजवा सके। जहां भी गया, ब्रज में गया तो ‘ब्रज साहित्य मंडल’ बनाया और ब्रजभाषा की सेवा की। दिल्ली में आया तो ‘दिल्ली हिन्दी साहित्य सम्मेलन’ बनाया और इलाहाबाद में गया, आपने सुना है नाम ‘परिमल’। मेरा वहां भी आना-जाना होता था। इलाहाबाद में मैं रात में हमेशा महादेवीजी के पास घंटे-आधा घंटे अवश्य बैठता था और निरालाजी से तो मेरी लखनऊ से ही जानकारी थी। पंतजी तो मुझसे ऐसे प्रभावित थे उन्होंने मेरे बारे में ये कहा है कि, “दूध में पानी मिल सकता है मगर व्यासजी में जो शुद्ध हास्य है, वह किसी और के पास नहीं। वह मिलावट रहित है।”
उत्तर : दिल्ली, ऐसा है हरिद्वार में हिन्दी साहित्य सम्मेलन का अधिवेशन हुआ। इसमें माखनलालजी चतुर्वेदी को चांदी के रुपयों से तोला गया। मैं उन दिनों सन् 1942 के आंदोलन में तोड़-फोड़ करता हुआ भटकता-भटकता इटावा पहुंच गया था। इटावा में श्रीनारायण चतुर्वेदी के पिता श्री द्वारिकानाथ चतुर्वेदी रहते थे। वह ब्रजभाषा का शब्दकोश बना रहे थे। उन्होंने मुझे आया जानकर अपने पास रख लिया और मैंने ‘ब्रजभाषा शब्दकोश’ तैयार करने में उनकी काफी सहायता की। वह ‘शब्दकोश’ छप भी गया। मैंने श्रीनारायणजी चतुर्वेदी से कहा कि वह कोश मुझे भिजवा दो, मगर वह नहीं भिजवा सके। जहां भी गया, ब्रज में गया तो ‘ब्रज साहित्य मंडल’ बनाया और ब्रजभाषा की सेवा की। दिल्ली में आया तो ‘दिल्ली हिन्दी साहित्य सम्मेलन’ बनाया और इलाहाबाद में गया, आपने सुना है नाम ‘परिमल’। मेरा वहां भी आना-जाना होता था। इलाहाबाद में मैं रात में हमेशा महादेवीजी के पास घंटे-आधा घंटे अवश्य बैठता था और निरालाजी से तो मेरी लखनऊ से ही जानकारी थी। पंतजी तो मुझसे ऐसे प्रभावित थे उन्होंने मेरे बारे में ये कहा है कि, “दूध में पानी मिल सकता है मगर व्यासजी में जो शुद्ध हास्य है, वह किसी और के पास नहीं। वह मिलावट रहित है।”
प्रश्न : व्यासजी आपका जो जीवन संघर्ष है, जो आपका व्यक्तित्व रहा है, वह अपने समय के अनेक आयामों को छूता रहा है। कितने साहित्यकारों से मित्रता रही है, परिचय रहा है। वह तो बड़ा ओजस्वी युग था। स्वतंत्रता आंदोलन का युग था, उस समय में भी आपने हास्य रस को अपना विशेष विषय बनाया। इसका क्या कारण रहा ?
उत्तर : हम बाबू गुलाबराय आदि के साथ एक गोष्ठी चलाते थे। उस गोष्ठी का चंदा कुछ नहीं था, ये था कि रचना पढ़नी है। सब अपनी-अपनी रचना पढ़ते, यानी रचनाकार ही उसके सदस्य थे। तो मेरा नम्बर आया तो सोचने लगा मैं क्या सुनाऊं ? बाबू गुलाबराय की लड़के को शादी में एक भैंस मिली थी। वह भैंस दूध ही नहीं देती थी, बाबूजी को छाछ, मक्खन ही नहीं देती थी, बल्कि बाबूजी के बगीचे के फल-फूलों को खा जाती थी, बिगाड़ देती थी। और एक दिन तो वह गुसलखाने में घुस गई। गुसलखाने में उनकी पत्नी नहा रही थी। तो बाबूजी भागे-भागे आए ‘साहित्य संदेश’ में और कहने लगे भैंस गुसलखाने में घुस गई है और उसमें पत्नी बैठी हुई है, व्यासजी उसे निकलवाओ। तो मैं और दो-तीन आदमी रस्सा लेकर गए। रस्सा बांधकर उस भैंस को निकाला तो उनकी पत्नी मुक्त होगईं। मैंने उस भैंस पर एक कविता पहले लिखी थीः
 ओ, बाबूजी की डबल भैंस!
ओ, बाबूजी की डबल भैंस!
मेरी कुटिया में घुस आई
तू बाबूजी की डबल भैंस!
ओ, बाबूजी की डबल भैंस!
ओ काली-सी, मतवाली-सी,
क्यों बिना सूचना घुस आई ?
समझा होगा शायद तूने
इसको कालिज का खुला ‘मैस’
ओ, बाबूजी की ……………….।
ऐ भैंस! अभी तक मैं तुझको
अक्कल से बड़ी समझता था।
ऐ महिषी! अब तक मैं तुझको,
अपरूप सुंदरी कहता था।
तेरी जलक्रीड़ा मुझे बहुत ही
सुंदर लगती थी, रानी!
तेरे स्वर का अनुकरण नहीं
कर सकता था कोई प्राणी
पर आज मुझे मालूम हुआ
तू निरी भैंस है, मोटी है,
काली है, फूहड़ है, थुल-थुल,
मरखनी, रैंकनी, खोटी है।
मेरे ही घर में आज चली
तू पाकिस्तान बनाने को ?
मेरी ही हिन्दी में बैठी
तू जनपद नया बसाने को ?
मैं कहता हूं, हट जा, हट जा,
वरना मुझको आ रहा तैश
ओ बाबूजी की …….
ऐसी पहली कविता मैंने लिखी। फिर ‘नागरी प्रचारिणी सभा’ में साहित्यकार संसद होती थी। उसमें कविता-पाठ होते थे। उसमें एक हरिशंकर शर्मा भी थे। उन्होंने मेरी कविताएं सुनीं। शर्माजी आदि ने बहुत पसंद कीं। मेरा उत्साह बढ़ा। मैंने दो-तीन कविताएं और लिखीं। ‘वीणा’ के संपादक कालकाप्रसादजी ‘कुसुमाकर’ आगरा आए। उन्होंने मेरी कविताएं सुनीं। मैंने चार कविताएं ही तब तक लिखी थीं। ‘कुसुमाकर’ जी मेरी चारों कविताओं को ले गए और उनको लगातार ‘वीणा’ में छापा। उन्होंने मेरे विषय में लिखा “यह तो नया हास्य-व्यंग्य का आदमी पैदा हुआ है, नई ज़मीन तोड़ी है, बेढब से, बेधड़क से बिलकुल अलग है।”
प्रश्न : आपका विवाह कब हुआ ? क्या पिताजी ने किया ?
उत्तर : ब्याह तो मेरा सोलह साल की उम्र में पिताजी ने कर दिया। माँ तो मर गई थी, वह मेरी सगाई ही देख पाई। अपनी बहू देखने के लिए वह तड़पती चली गई। अपनी माँ की मैं कोई सेवा नहीं कर सका। ये दुख मुझे हमेशा सालता रहता है। मैंने यश भी खूब कमाया, धन भी खूब कमाया, लेकिन अपनी जननी माँ को जो जन्मभर दुखिया रही, उसकी मैं कोई सेवा नहीं कर सका।
प्रश्न : व्यासजी, मैंने विवाह का प्रश्न आपसे जानबूझकर पूछा। आपने हास्य-रस में विशेष तौर पर पत्नीवाद का प्रयोग किया है। इसके संबंध में कुछ बताइए ?
उत्तर : यह वह समय था जब अंग्रेजों का राज पूरी तरह से जमा हुआ था। कोई कुछ नहीं कह सकता था, दमन चक्र चल रहा था। जो कोई कुछ बोलता उसे पकड़कर जेल भेज दिया जाता था। ऐसी विषम परिस्थितियों में मैंने अपनी पत्नी को माध्यम बनाकर अंग्रेजों के खिलाफ़ कविता लिखना शुरू किया। मेरी हर कविता में समय की छाप हैः
उनको अपनी हिटलर समझो,
चर्चिल सा डिक्टेटर जानो,
पत्नी को परमेश्वर मानो।
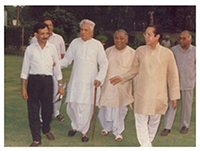 डिफेंस एक्ट के ज़माने में मैंने पत्नी को माध्यम बनाकर कविताएं लिखी। इटावा में ये कविताएं मैंने शिवनारायण अग्रवाल के चाचा को सुनाईं जो वहां रहते थे। उन्होंने मुझे पहचान लिया, ‘हिन्दुस्तान’ के मैग्ज़ीन सेक्शन का एक संपादक वहां रहता था। उन्होंने उसका उल्लेख पत्रकार महोदय से किया। वह मेरी कविताएं ले गया और वह कविताएं ‘हिन्दुस्तान’ में छपने लगीं। फिर देवदास गांधी का पत्र आया कि आप प्रति सप्ताह कविता भेजते रहिए। पाठकों को और हमें यह कविताएं बहुत पसंद आईं। तब मैं और अधिक लिखने लगा। मैं जब हरिद्वार आया था तो उस हिन्दी सम्मेलन में जैनेन्द्रजी भी आए थे। जैनेन्द्रजी ने मुझसे कहा कि “तुम दिल्ली आ जाओ” तो मैंने कहा, “कौन जाए यार अब, मथुरा की गलियां छोड़कर।” कुछ दिन बाद एक सादे लिफाफे में पचास रुपये और एक चिट जिस पर लिखा था, “व्यास, दिल्ली आ जाओ।” जैनेन्द्रजी का पत्र था। फिर लोगों ने मुझे परामर्श दिया कि चूको मत, चले जाओ। और मैं दिल्ली आ गया। जैनेन्द्रजी के पास बहुत दिन रहा। जैनेन्द्रजी से बिगड़ गई। ‘हिन्दुस्तान’ में कविताएं छपती रहीं। हिन्दुस्तान से दीवाली पर दो सौ रुपये का बोनस मिला। मैं फूला नहीं समाया। कविताओं पर पहली बार किसी अख़बार से बोनस मिला। कुछ दिन उपरांत देवदास गांधी (महात्मा गांधीजी के पुत्र) का पत्र आया कि आप मुझसे मिल लीजिए। मैं मिलने गया तो देवदासजी ने कहा कि आप ‘हिन्दुस्तान’ में आ जाइए। देवदास गांधीजी उस समय ‘हिन्दुस्तान टाइम्स’ में निदेशक थे। मैं ‘हिन्दुस्तान’ में काम करने लगा।
डिफेंस एक्ट के ज़माने में मैंने पत्नी को माध्यम बनाकर कविताएं लिखी। इटावा में ये कविताएं मैंने शिवनारायण अग्रवाल के चाचा को सुनाईं जो वहां रहते थे। उन्होंने मुझे पहचान लिया, ‘हिन्दुस्तान’ के मैग्ज़ीन सेक्शन का एक संपादक वहां रहता था। उन्होंने उसका उल्लेख पत्रकार महोदय से किया। वह मेरी कविताएं ले गया और वह कविताएं ‘हिन्दुस्तान’ में छपने लगीं। फिर देवदास गांधी का पत्र आया कि आप प्रति सप्ताह कविता भेजते रहिए। पाठकों को और हमें यह कविताएं बहुत पसंद आईं। तब मैं और अधिक लिखने लगा। मैं जब हरिद्वार आया था तो उस हिन्दी सम्मेलन में जैनेन्द्रजी भी आए थे। जैनेन्द्रजी ने मुझसे कहा कि “तुम दिल्ली आ जाओ” तो मैंने कहा, “कौन जाए यार अब, मथुरा की गलियां छोड़कर।” कुछ दिन बाद एक सादे लिफाफे में पचास रुपये और एक चिट जिस पर लिखा था, “व्यास, दिल्ली आ जाओ।” जैनेन्द्रजी का पत्र था। फिर लोगों ने मुझे परामर्श दिया कि चूको मत, चले जाओ। और मैं दिल्ली आ गया। जैनेन्द्रजी के पास बहुत दिन रहा। जैनेन्द्रजी से बिगड़ गई। ‘हिन्दुस्तान’ में कविताएं छपती रहीं। हिन्दुस्तान से दीवाली पर दो सौ रुपये का बोनस मिला। मैं फूला नहीं समाया। कविताओं पर पहली बार किसी अख़बार से बोनस मिला। कुछ दिन उपरांत देवदास गांधी (महात्मा गांधीजी के पुत्र) का पत्र आया कि आप मुझसे मिल लीजिए। मैं मिलने गया तो देवदासजी ने कहा कि आप ‘हिन्दुस्तान’ में आ जाइए। देवदास गांधीजी उस समय ‘हिन्दुस्तान टाइम्स’ में निदेशक थे। मैं ‘हिन्दुस्तान’ में काम करने लगा।
प्रश्न : व्यासजी, ये बताइए, आपने अपनी ‘पत्नी’ पर इतनी कविताएं लिखीं और वे बहुत प्रसिद्ध हुईं। भाभीजी उन कविताओं को सुनती थीं, तो उनकी क्या प्रतिक्रिया हुई।
उत्तर : ऐसा है कि विजयलक्ष्मी पंडित और पं. जवाहरलाल नेहरू मेरी कविताओं के बड़े प्रेमी थे। तो एक दिन विजयलक्ष्मी पूछतीं-पूछतीं मेरे घर आ गईं और मेरी पत्नी से कहने लगीं कि, “तुम्हारे बारे में व्यासजी कविता लिखते हैं, क्या तुम पढ़ती हो ? क्या अंट-शंट लिखते रहते हैं।” मेरी पत्नी पढ़ी-लिखी तो हैं नहीं, उन्होंने कहा कि, “कोई कुछ धंधा करता है, तो कोई कुछ। ये कविता करके मेरे नाम से कमा रहे हैं, तो कमा लेने दो। मैं तो इन्हें इसी रूप में जानती हूं, आगे कुछ नहीं।”
प्रश्न : हास्य रस की कविताओं की बात हुई। आपकी कुछ कविताएं एक बार मैंने सुनी थीं तो आपने पशुओं पर भी कुछ कविताएं लिखी हैं। ‘पशु-काव्य’ लिखा है। नाम तो उनका पशुओं पर था, पर यह कविताएं पशुओं के माध्यम से मनुष्यों पर हैं। वह कविताएं बड़ी पसंद की गईं। हास्य में सामाजिक चेतना कैसे समाहित की है, आपकी इन कविताओं से पता चलता है।
उत्तर : मैंने साहित्य में आप जैसे साहित्यकारों की प्रेरणा से बहुत प्रयोग किए हैं, कविता के क्षेत्र में भी और लेखन के क्षेत्र में भी। पत्नी पर ही नहीं, पूरा ‘परिवार रस’ लिखा है। ब्रजभाषा में ‘गोपिन के अधरान की भाषा’ और ‘रास-रसामृत’ में भगवान का रास कैसा हुआ, उस रास का रहस्य क्या है ? यह रासलीला नहीं, बल्कि गोपियों का प्रेमभाव है। संयोग नहीं, वियोग है। जब नेताजी ने ‘दिल्ली चलो’ का अभियान शुरू किया और सेना बनाकर हिन्दुस्तान की ओर चल दिए तो शायद आपको याद हो मैं हिन्दुस्तान में प्रतिदिन ‘नेताजी’ पर एक कविता लिखता था। उन कविताओं को दिनकरजी ने ‘वीर रस का खंडकाव्य’ कहा है। उसमें मैंने मातृभूमि के प्रति नेताजी का प्रेम व्यक्त किया है।
‘पशु-काव्य’ लिखने की बात कुछ यों शुरू हुईं। जब हजारीप्रसाद द्विवेदी ने लिखा और कहा कि हास्य ठीक-ठाक लिख रहे हो। हास्य को साहित्य में, संस्कृत साहित्य में, रीति साहित्य में मान्यता मिली है। लेकिन व्यंग्य को मान्यता नहीं मिली। इसलिए व्यासजी, तुम व्यंग्य लिखो। मेरे विचार से तुम अच्छा व्यंग्य लिख सकते हो और व्यंग्य में नए-नए प्रयोग करो। मनुष्य पर, नेताओं पर, समाज के लोगों पर सीधी बात न कहकर व्यंग्य के माध्यम से बात करो। जैसे पत्नी को माध्यम बनाकर मैंने अंग्रेजों पर कविताएं लिखीं। इसी प्रकार पशुओं को माध्यम बनाकर कविताएं लिखीं। एक कविता सुनाता हूं:-
आदमी की शेव बनती है,
रीछ की नहीं।
आदमी अंडरवियर पहनता है,
बन्दर नहीं।
हाथी पर अंकुश लगता है,
आदमी पर नहीं।
आदमी नेता हो सकता है,
लेकिन नेता आदमी नहीं।
ऐसी ही एक कविता और सुनिए ………..
इन्सानियत ले गए पशु
एक दिन ईश्वर के घर लूट हुई-
चूहा दांत ले भागा
बिल्ली मूंछें
खुदा स्टोर तलाश करने लगा
किससे पूछें ?
ऊंट ने उठाकर
उसे अपने पेट में फिट कर लिया था,
हाथी ने बुद्धि का बंडल
अपने कब्जे में कर लिया था,
घोड़े ने शक्ति
कुत्ते ने भक्ति
सियार ने संगीत
हिरनी ने अनुरक्ति
सूअर ने सृजन
बंदर ने तोड़-फोड़
शुतुरमुर्ग ने पलायन
लोमड़ी ने जोड़-तोड़
गाय ने श्रद्धा
भालू ने ताड़ी का अद्धा
गधे ने सहनशीलता
कुतिया ने अश्लीलता
शेर ने सम्मान
देसी पिल्ले ने अपमान
जब खजाना खाली होगया
पहुंचा इन्सान।
खुदा बोला —
इन्सानियत तो रही नहीं
उसे तो जानवर ले गए ,
अब तो हमारे पास
हैवानियत, खुदगर्जी़
और बे-मौसम के काम-क्रोध ही रह गए हैं
चाहो तो ले जाओ !
मनुष्य बोला-लाओ, जल्दी लाओ!
प्रश्न : आपने जो कविता के अतिरिक्त बड़ा काम किया है। जिसको मैं बहुत सम्मान की दृष्टि से देखता हूं। आपका जो मैं बड़ा अनुकरणीय काम मानता हूं। देशप्रेम, साहित्यप्रेम और संस्कृतिप्रेम सबका प्रतिमान है वह ग्रंथ ‘ब्रज विभव’। मैंने बहुत से लोगों से कहा कि ऐसा काम करना चाहिए। मैं भी ‘अवध विभव’ निकालना चाहता था। मेरी आकांक्षा थी जो पूरी नहीं हुई। आपने जो काम किया है, वैसा आज तक कोई और नहीं कर पाया। उसकी क्या पृष्ठभूमि थी। इसकी योजना आपने किस प्रकार से बनाई ?
उत्तर : आपने मेरा ‘स्वतंत्रता के पच्चीस वर्ष’, ‘गांधी हिन्दी दर्शन’ देखे हैं ? ‘ब्रज विभव’ का ऐसा है कि मैं जहां रहा, जिस प्रदेश में रहा, उसके प्रति मैंने अपने दायित्व को पूरा किया है। ब्रज में मैंने ‘ब्रज साहित्य मंडल’ बनाया। ब्रज की कहानियों का, ब्रज के लोकगीतों का, ब्रज की लोकोक्तियों का संग्रह किया। उस संग्रह से लोगों ने पी.एच.डी. तक की। उसकी रिपोर्ट आज भी नागरी प्रचारणी सभा में जमा है। दिल्ली आया तो दिल्ली को उठाया। चालीस हजार लोग तैयार किए। मेरे मन में ब्रज का साहित्य, ब्रज की संस्कृति, ब्रज की धरोहर जमी हुई थी, उसको बाहर निकालने के लिए मैं तड़प रहा था। उसके लिए बनारसीदासजी की प्रेरणा मिली और जगदीशप्रसाद चतुर्वेदी, भवानीप्रसाद मिश्र आदि ने कहा कि ब्रज पर लिखो। मैंने ब्रज पर लिखना शुरू किया और मथुरा के एक जोशी बाबा ने मुझे बड़ा प्रोत्साहन दिया और कहा कि ये सामग्री यहां से मिल सकती है। इनसे पत्र-व्यवहार करो। तो वहां से नंदगांव, बरसाने के बारे में, वृंदावन के बारे में पूछ-पूछकर और जो जानकारियां मेरे मन में थीं सब निकालकर यह ग्रंथ ‘ब्रज विभव’ तैयार कर दिया। बाद में हमारे पं. कमलापति त्रिपाठीजी की कृपा से इसके छपने का भी प्रबंध होगया। त्रिपाठीजी ने दस धनीमानी लोगों से दस-दस हजार रुपये इकट्ठे करके इस ग्रंथ को छपवा दिया।
प्रश्न : व्यासजी, ‘ब्रज विभव’ के अतिरिक्त आपके यश का एक और जो स्तंभ है दिल्ली में। आपके बहुत दिनों बाद तक यह यश का स्मारक बना रहेगा। वह है ‘हिन्दी भवन’। मेरी समझ से ‘हिन्दी भवन’ जैसा दूसरा भवन शायद भारतवर्ष में कहीं हो। मेरी समझ से शायद शान्ति निकेतन में ऐसा ‘हिन्दी भवन’ स्थापित किया था आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी ने भी। लेकिन आप जानते हैं कि हमारे संविधान में राष्ट्रभाषा हिन्दी होते हुए भी हिन्दी के नाम पर दिल्ली में, राजनीतिज्ञों में कोई उत्साह नहीं दिखाई पड़ता। आपने ऐसी स्थिति में दिल्ली में शानदार ‘हिन्दी भवन’ बनाया, जो इस समय बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है। इसके बारे में जानना चाहता हूं।
उत्तर : इसका भी संस्मरण सुन लो, कहानी सुन लो। मैं तो ‘ब्रज साहित्य मंडल’ में काम करता था। लेकिन टंडनजी की निगाह मुझ पर शुरू से ही थी। तो एक बार मैं बालकृष्ण शर्मा ‘नवीन’ जी के सभापतित्व में, सहारनपुर में, एक कवि-सम्मेलन में भाग ले रहा था। तब मुझे टंडनजी का तार मिला कि, ‘तुम दिल्ली आओ, आवश्यक काम है।’ तो मैं दिल्ली आ गया। तो मौलिचंद शर्मा ने कहा कि तुम ‘दिल्ली हिन्दी साहित्य सम्मेलन’ का मंत्रीपद संभाल लो। तो मैंने इस विषय में टंडनजी से परामर्श किया तथा उनकी आज्ञा से ‘दिल्ली हिन्दी साहित्य सम्मेलन’ संभाल लिया। टंडनजी के संपर्क से बढ़ता ही चला गया। ऐसा बढ़ा कि वे मुझे ‘अखिल भारतीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन’ का मंत्री बनाना चाहते थे, परंतु मैं नहीं बना। मैंने कहा कि मैं इलाहाबाद के चक्कर में नहीं पड़ता। इसके बाद मैंने और शास्त्रीजी ने (श्री लालबहादुर शास्त्री) ‘टंडन अभिनंदन ग्रंथ’ तैयार किया और उन्हें भेंट किया। तब से टंडनजी से संबंध और प्रगाढ़ होगए। मृत्यु-शैय्या पर जाने से पहले उन्होंने मुझे बुलाया। तो मैं गया तो मुझसे कहा, “मेरा हाथ छूकर के एक बात कहो।” मैंने कहा, “बाबूजी, आज्ञा करो, हाथ क्या चरण छूता हूं।” तो कहा, “मैं चरण किसी को नहीं छूने देता। मैं यह चाहता हूं कि जब तक तुम हो, तब तक दिल्ली में हिन्दी का काम करते रहो और दूसरी बात ये है कि दिल्ली में हिन्दी चलेगी तो देश में हिन्दी चलेगी, और दिल्ली में हिन्दी का एक घर होना चाहिए।” तो मैंने टंडनजी की प्रेरणा से ‘श्री पुरुषोत्तम हिन्दी भवन न्यास समिति’ बनाकर यह हिन्दी भवन खड़ा किया है।
प्रश्न : पं. हजारीप्रसाद द्विवेदी से आपका परिचय कैसे हुआ ?
उत्तर : मैंने बताया न कि मैंने एक लेख उनके पास भेजा था कि यह कैसा है, जानने के लिए। तब उन्होंने मुझसे बिना व्यक्तिगत परिचय के, उन्होंने उस लेख को पंसद किया, इससे परिचय बढ़ता चला गया। फिर शांति निकेतन से हिन्दी की पत्रिका निकालने का विचार आया तो उसके लिए उन्होंने मुझे बुलाया और कहा कि, “आ जाओ, ‘साहित्य संदेश’ का काम बहुत कर लिया। बंगाल में बैठकर हिन्दी का काम करोगे तो अखिल भारतीय हो जाएगा।” पर ‘साहित्य संदेश’ और बाबू गुलाबराय ने मुझको नहीं छोड़ा। तो यहां से शुरूआत हुई, फिर बढ़ता ही चला गया, बढ़ता ही चला गया। वह यहां आए, मैं काशी गया, वे मेरे घर आए, मैं उनके घर गया। भाईचारा स्थापित होगया, पारिवारिक संबंध स्थापित होगए। उन्होंने मुझे लेखन में, व्यक्तिगत जीवन में, बहुत ही सहारा दिया, बड़ी प्रेरणा दी। हाथ पकड़कर के उठाया है उठाने वालों ने। हजारीप्रसाद द्विवेदी, बाबू गुलाबराय और विष्णु प्रभाकर- ये तीन व्यक्ति मेरे जीवन में आए हैं। डॉ. सत्येन्द्र के साथ आए हैं, जिन्होंने मुझे साहित्य में बहुत सहारा दिया।
प्रश्न : अभी आप नवीनजी के संबंध में बता रहे थे। आपने उन पर कविता भी लिखी है।
उत्तर : नवीनजी से मेरा साहित्यिक विषयों पर संबंध नहीं रहा। उनके व्यक्तित्व से मैं प्रभावित था, मेरे लेखक, पत्रकार होने से वे प्रभावित थे। खाते-पीते, उठते-बैठते, रोज़ मिलते थे। बातें किया करते थे। इस प्रकार से संपर्क बढ़ता ही चला गया। साहित्य के बारे में कम बात होती थी, बस देश और समाज के बारे में बातें होती रहती थीं। लालकिले का कवि-सम्मेलन ‘नवीनजी’ की प्रेरणा से प्रारंभ हुआ। उन्होंने जवाहरलालजी से कहा कि, “आप पहले चुनाव का शुभारंभ कवि-सम्मेलन से कीजिए।” तो नेहरूजी ने कहा कि, “कवि-सम्मेलन में कितने आदमी आएंगे ? सौ कि पचास ?” तो मैं भी वहां बैठा था। मैंने कहा कि, “आपको कितने आदमी चाहिए ?” तो उन्होंने कहा कि, “कम से कम दो-चार हजार।” मैंने कहा, “इससे ज्य़ादा आ जाएं तो।” उन्होंने कहा, “तो फिर क्या कहना।” उन्होंने मान लिया। मैंने शंकर कार्टूनिस्ट से दो बैलों की जोड़ी का निशान बनवाया। नवीनजी की अध्यक्षता में कवि-सम्मेलन कराया। देश के मूर्धन्य कवि आए, पांच लाख से ऊपर रामलीला मैदान में लोग इकट्ठे होगए। मिन्टो रोड की छतों पर, पेड़ों पर आदमी चढ़ गए। जवाहरलालजी खुश होगए और उन्होंने मुझे हिन्दी समिति का कार्यकर्त्ता बनने का सुझाव दिया, जिसके दिनकरजी बाद में कार्यकर्त्ता प्रमुख बने, परंतु मुझे गांधीजी ने कहा कि “तुम राजनीति के चक्कर में मत पड़ो। पत्रकारिता और साहित्य-सेवा करते रहो। साहित्य-सेवा भी देश-सेवा है। बाद में मुझे संसद के लिए टिकट मिला, मैं नहीं गया। इन्दिराजी भी मुझे राज्यसभा का सदस्य बनाकर रखना चाहती थीं, मैं नहीं गया। श्री लालबहादुर शास्त्रीजी मुझको ‘पद्मभूषण’ दिलाना चाहते थे, लेकिन मैंने ‘पद्मभूषण’ स्वयं न लेकर श्री माखनलाल चतुर्वेदीजी को दिलवा दिया। मैंने कहा कि मेरी उम्र तो अभी बहुत है, चतुर्वेदीजी को अभी तक नहीं मिला, आप उन्हें दे दीजिए। बाद में मुझे ‘पद्मश्री’ मिली जो मैंने हिन्दी की उपेक्षा पर वापिस लौटा दी।
प्रश्न : आपका कवि-सम्मेलनों से बड़ा गहरा संबंध रहा है। आप तो कवि-सम्मेलनों के राजा रहे हैं। आप जहां जाते थे बहुत जमते थे। लोग बड़े ध्यान से आपकी कविताएं सुनते थे। तो कवि-सम्मेलनों के कुछ संस्मरण अथवा अनुभव सुनाइए।
उत्तर : मैंने रंगून से लेकर काहिरा तक कविता-पाठ किया है। देश का कोई शहर या विकसित कस्बा ऐसा नहीं है जिसमें मैंने कवि-सम्मेलन में भाग न लिया हो। सैकड़ों कवियों को मैंने मंचीय कवि बना दिया। क्या नीरज, क्या बैरागी, आदित्य, संतोषानंद, काका हाथरसी, अल्हड़, हुल्लड़ सब आगे बढ़ गए हैं। मेरा प्रथम लक्ष्य कवि-सम्मेलनों के माध्यम से हिन्दी का प्रचार करना था। कवि-सम्मेलन से ख्याति मिलती थी, पैसा भी मिलता था। दक्षिण भारत में भी मैंने यात्रा की। हिन्दी कविता और हिन्दी में भाषण दिए। खूब सुने और सराहे गए। बंगाल में, महाराष्ट्र में, आंध्र में अहिन्दी क्षेत्रों में भी दौड़-दौड़कर जाता था। अलीगढ़ में मुसलमानों के गढ़ में भी मैंने हिन्दी कविता-पाठ, हिन्दी का प्रचार किया है।
प्रश्न : व्यासजी, हजारीप्रसाद द्विवेदीजी की प्रेरणा से जो व्यंग्यात्मक कविताएं आपने लिखी हैं, उन्हें सुनने की ललक मेरे मन में है। कृपया उनमें से कोई एक कविता सुनाइए।
उत्तर : सुनिये ……….
बोए गुलाब
आंसू नीम चढ़े
खून पड़ा काला !
कानों में लाख जड़ी
जीभ पर छाला !
और तुम कहते हो, हंसो !
सड़ी हुई सभ्यता पर फब्तियां कसो !
कागज की व्यवस्था चर गई,
स्याही
सफेद को काला करते-करते
गुज़र गई !
चश्मे ने
कर दिया देखना बंद,
और कलम !
अपनी मौत खुद मर गई
और तुम कहते हो लिखो ?
समाज में बुद्धिजीवी तो दिखो !
छिलके-पर-छिलके
पर्त-पर-पर्त
काई ओर कीचड़
गर्त-ही-गर्त
और तुम कहते हो उठो और चलो !
बहारों का मौसम है
मचलो, उछलो !
बोए गुलाब, उग आए कांटे !
सांपों और बिच्छुओं ने
दंश-डंक बांटे,
नागफनी हंसी,
तुलसी मुरझाई !
खंडित किनारों पर
लहरों की चोटें,
और तुम कहते हो नाचो
,
युग की रामायण का
सुंदरकांड बांचो !
कुंभकरणी दोपहरी, मंदोदरी सांझ,
रात शूर्पणखा-सी बेहया, बांझ,
मेघनाद छाया है
दसों दिशा क्रुद्ध !
चाह रहीं बीस भुजा
तापस से युद्ध
और तुम कहते हो
सृजन को संवारो !
कंटकित करीलों की
आरती उतारो !
प्रतिभा के पंखों पर
सुविधा के पत्थर !
कमलों पर जा बैठे नाली के मच्छर !
गमलों में खिलते हैं
कागज के फूल !
चप्पल पर पालिश है,
टोपी पर धूल !
और तुम कहते हो आंसू मत बोओ !
सुमनों को छेद-छेद माला पिरोओ !
दफ्तर में खटमल की वंश-बेल फैली
कुर्सी पर बैठ गई चुपके से थैली !
बोतल से बहती है गंगा की धारा,
मंझधार सूख गई, डूबता किनारा !
द्रौपदी ने जुए में धर्मराज हारा !
अर्जुन से गांडीव कर गया किनारा !
और तुम कहते हो
छोड़ दो निराशा ?
होने दो होता है
जो भी तमाशा ?
प्रश्न : व्यासजी, आपने अपने व्यस्त समय में से इतना समय दिया इससे हम लोग बहुत लाभान्वित हुए। मैं समझता हूं कि आपसे जो संक्षिप्त वार्त्तालाप हुआ, इसका एक महत्व होगा और लोग भी लाभान्वित होंगे। यह मेरा सौभाग्य है कि आप जैसे साहित्य मनीषी और हिन्दी के अनन्य और अन्यतम सेवक के साथ बैठने का अवसर मिला। मैं आपके प्रति अपनी ओर से और हिन्दी समाज की ओर से कृतज्ञता व्यक्त करता हूं और अपनी ओर से आभार प्रगट करता हूं।
उत्तर : त्रिपाठीजी, आपकी कृपा है जो आप ऐसा मानते हैं। मैं तो एक साधारण जीव हूं, बिना पढ़ा-लिखा और गुरुजनों के आशीर्वाद से आगे बढ़ा हुआ आदमी हूं। आप जैसे मित्रों की प्रेरणा से मेरे व्यक्तित्व और साहित्य का निर्माण हुआ है। ऐसी ही प्रेरणा और प्रोत्साहन मुझे देते रहेंगे तो जीवन के जो थोड़े वर्ष रह गए हैं, उसमें भी मैं सक्रियता से काम करता रहूंगा।
त्रिपाठीजी : आप आशीर्वाद दीजिए व्यासजी, मैं चरण स्पर्श करता हूं।
-*- इति शुभम् -*-